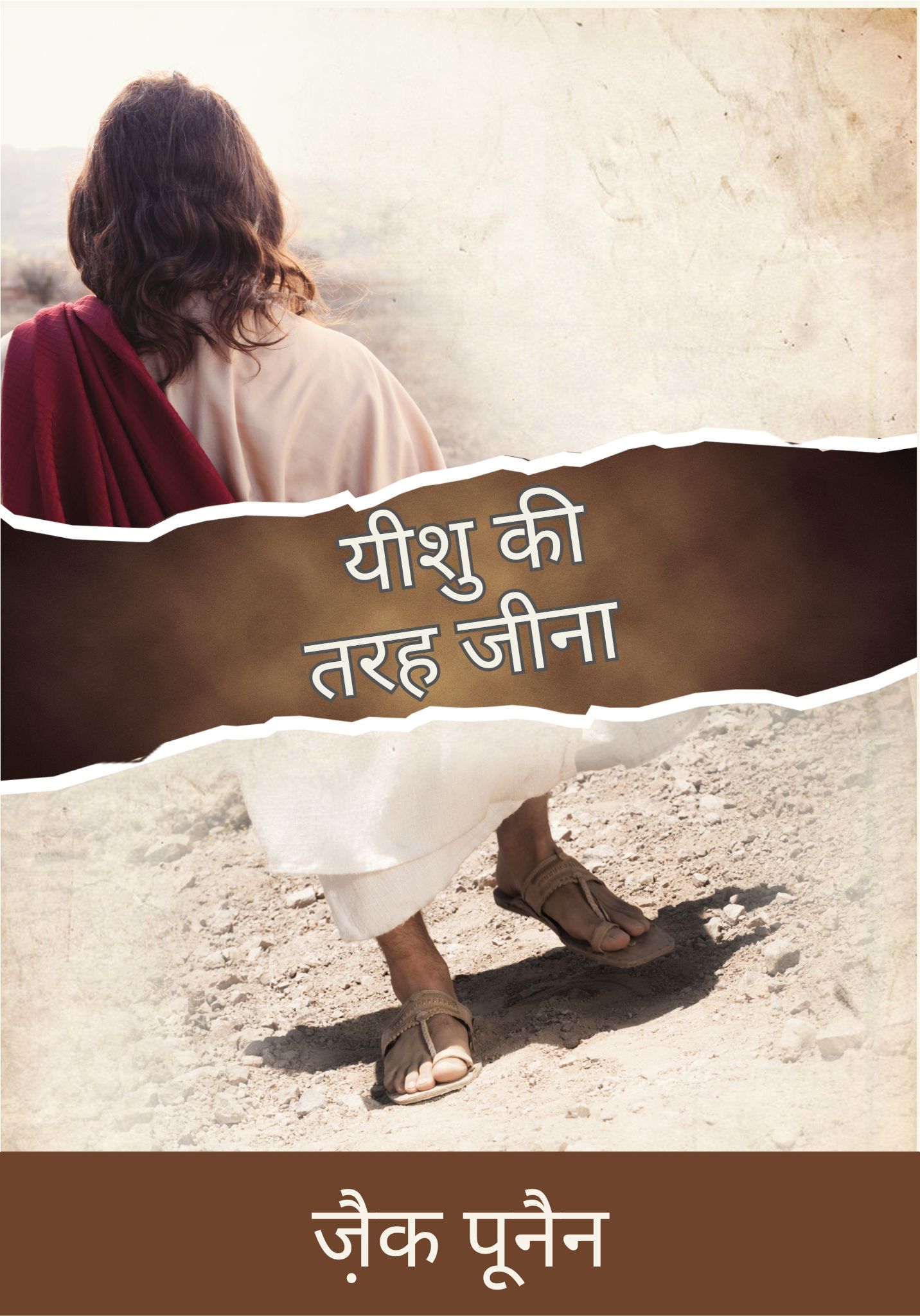
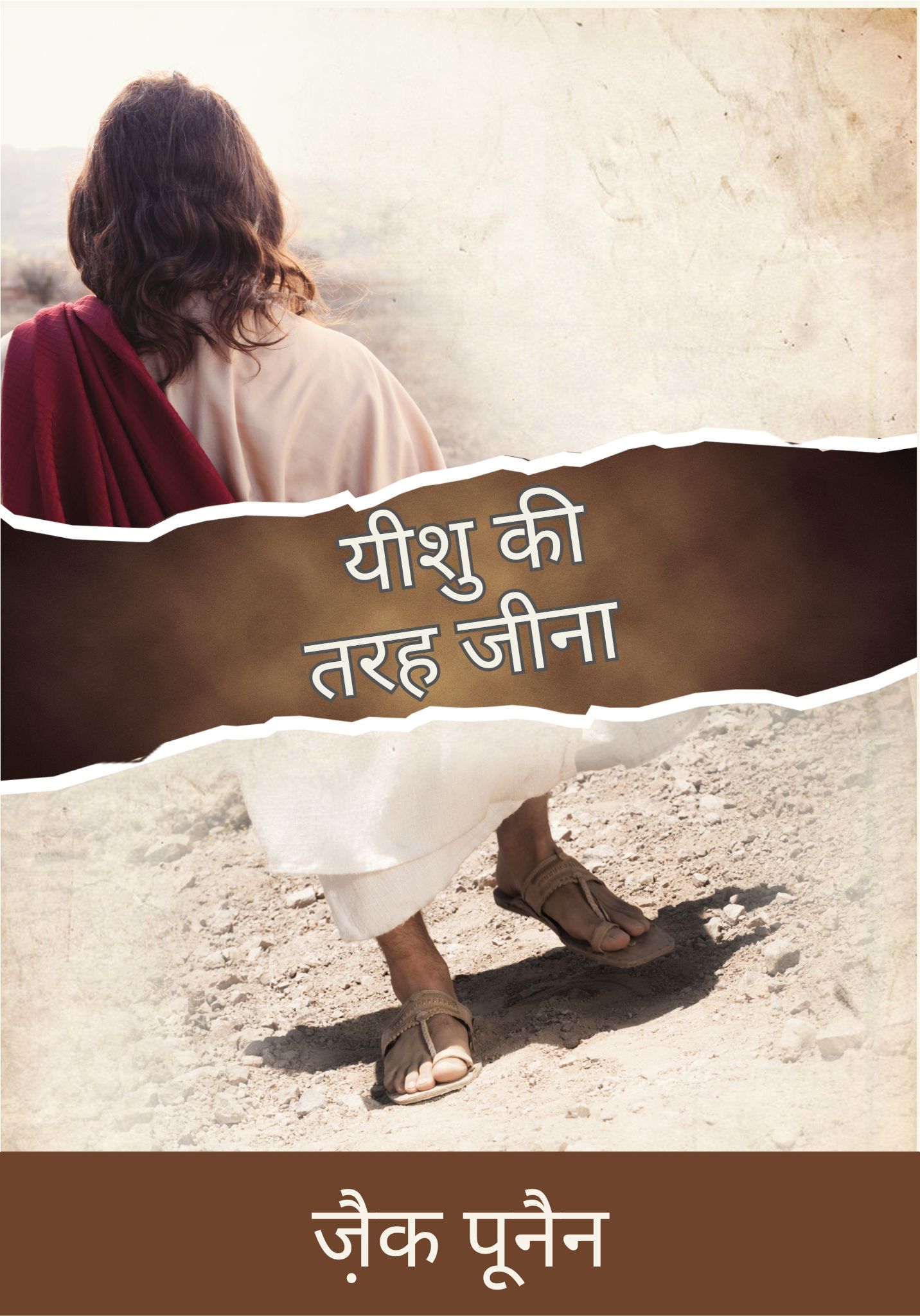
जो यह कहता है कि वह एक मसीही है ,
तो उसे मसीह की तरह जीना चाहिए।
(1यूहन्ना2:6 - लिविंग बाइबल)
परमेश्वर ने मनुष्य को इसलिए नहीं रचा था कि उसे एक सेवक की ज़रूरत थी। उसकी सेवा के लिए उसके पास पहले ही करोड़ों स्वर्गदूत थे। उसने मनुष्य की रचना इसलिए की क्योंकि वह कुछ ऐसा रचना चाहता था जो उसका चरित्र और उसका स्वभाव प्रकट करे।
अगर हम इस सत्य को भूल जाएंगे, तो हमारे लिए मार्ग से हट कर यह कल्पना करने वाले बन जाना बिलकुल आसान हो जाएगा कि मसीह में हमारे उद्धार का मुख्य उद्देश्य परमेश्वर की सेवा करना है। अनेक विश्वासी यह सोचने की ग़लती कर चुके हैं।
परमेश्वर ने जब आदम की रचना की तब उसके ये शब्द थे, "आओ, हम मनुष्य को अपने स्वरूप और अपनी समानता में बनाएं" (उत्पत्ति 1:26)।
आदम की रचना करने से पहले, अपने पूर्वज्ञान में, परमेश्वर ने अपने पहले ही मनुष्य को पाप के उस गड्ढे में से निकालने का इंतज़ाम कर दिया था जिसमें आदम जा गिरा था। आदम की रचना से पहले ही परमेश्वर के मन में मसीह का देहधारण और सूली पर उसकी मृत्यु थी।
हमारे लिए परमेश्वर ने मसीह में जो छुटकारा तैयार किया है, वह यही है कि हमें वापिस उसी जगह पर लाया जा सके जहाँ हमारी रचना का मूल उद्देश्य पूरा किया जा सके - कि मनुष्य परमेश्वर का स्वभाव अभिव्यक्त करे।
हमारा उद्धार मसीह में विश्वास द्वारा है, लेकिन विश्वास सिर्फ उस ईश्वरीय प्रकाशन पर ही आधारित हो सकता है जिसमें मसीह एक व्यक्ति के रूप में हम पर प्रकट हो जाता है। सिर्फ ऐसा विश्वास ही पवित्र आत्मा को यह अनुमति दे सकता है कि वह हमें मसीह की समानता में बदल सके।
ईश्वरीय प्रकाशन के अलावा, मसीह का बौद्धिक या आंशिक ज्ञान, हमें वैसा ही अंधा बना सकता है जैसे यीशु के समय में बाइबल के ज्ञानी अंधे थे। पवित्र-शास्त्रें के बारे में उनकी समझ उन्हें एक ऐसे मसीह को ढूंढने की दिशा में ले गई, जिसका चरित्र-चित्रण उससे अलग था जो नासरत के यीशु का था।
बाइबल के पृष्ठों में पाया जाने वाला यीशु वह है, जिसने परमेश्वर होते हुए, पिता के तुल्य होते हुए, "अपने आपको ख़ाली किया" और मनुष्य बन गया (फिलि. 2:6,7)।
यहाँ हमें सत्य को ध्यान-पूर्वक समझ लेने की ज़रूरत है। अपने व्यक्ति में, यीशु तब भी परमेश्वर था जब वह देहधारी होकर पृथ्वी पर आया था, क्योंकि परमेश्वर कभी भी परमेश्वर होना नहीं छोड़ सकता। यीशु के आराध्य-देव होने का सबसे बड़ा प्रमाण यह है कि उसने अपने देह में रहने के दिनों में मनुष्यों की आराधना स्वीकार की थी। सुसमाचारों में सात बार हमें बताया गया है कि जब मनुष्यों ने उसकी आराधना की, तो उसने वह स्वीकार की थी (मत्ती 8:2; 9:18; 14:33; 15:25; 20:20; मरकुस 5:6; यूहन्ना 9:38)। स्वर्गदूत ओर परमेश्वर का भय मानने वाले लोग आराधना ग्रहण नहीं करते (प्रेरितों-10:25,26; प्रका. 22:8,9)। लेकिन यीशु ने मनुष्यों की आराधना को ग्रहण किया, क्योंकि वह परमेश्वर का पुत्र था।
उसने अपने अन्दर से क्या ख़ाली किया था? परमेश्वर होने के अपने विशेषाधिकारों को।
दो उदाहरणों पर विचार करें। हम जानते हैं कि परमेश्वर को परीक्षा में नहीं डाला जा सकता (याकूब 1:13)। फिर भी पवित्र शास्त्र कहता है कि यीशु की परीक्षा हुई (मरकुस 4:1-11)।
हम यह भी जानते हैं कि परमेश्वर सर्वज्ञानी है (सब जानता है)। फिर भी पवित्र शास्त्र बताता है कि यीशु को यह जानने के लिए कि उसमें फल है या नहीं, एक अंजीर के पेड़ के पास आना पड़ा था (मरकुस 11:13)। यीशु ने एक बार यह भी कहा था कि वह अपने दूसरे आगमन का समय नहीं जानता है (मरकुस 13:32)।
इसलिए यह बिलकुल स्पष्ट है कि जब यीशु इस पृथ्वी पर हमारी देह में होकर चला-फिरा था, तब उसने आराध्य-देव होने के अपने विशेषाधिकारों से अपने आपको ख़ाली कर दिया था।
"वचन परमेश्वर था... और वचन देहधारी हुआ" (यूहन्ना 1:1,14)।
अगर हमें झूठे मसीही सिद्धान्तों में फँसने से बचे रहना है, तो हमें मसीह के व्यक्तिपन के इन दोनों सत्यों पर - उसके आराध्य-देव होने पर व उसके मनुष्य होने पर, एक समान विश्वास करना होगा।
हम पवित्र-शास्त्र के किसी भी सत्य को अनदेखा करके उससे होने वाले आत्मिक नुक़सान से नहीं बच सकते। इसलिए अगर हमारी समझ और हमारी सेवकाई में, यीशु के आराध्य-देवत्व और उसके मनुष्यत्व, दोनों पर ही समान ज़ोर नहीं दिया जाएगा, तो अंत में हम एक ऐसे अधूरे मसीह में विश्वास करते हुए पाए जाएंगे, जो पवित्र-शास्त्र में प्रकट हुआ यीशु नहीं बल्कि कोई फ्दूसरा यीशुय् होगा। इसे हमारे मसीही जीवन और सेवकाई में उतना ही नुक़सान होगा। हमें न सिर्फ परमेश्वर के रूप में मसीह की आराधना करने के लिए बुलाया गया है, बल्कि एक मनुष्य के रूप में उसके पीछे चलने के लिए भी बुलाया गया है।
यीशु ने हमें न सिर्फ उसकी मृत्यु द्वारा हमें छुड़ाया है, बल्कि पृथ्वी पर अपने जीवन द्वारा हमें यह भी दिखाया है कि परमेश्वर की इच्छानुसार मनुष्य को कैसा जीवन जीना चाहिए। वह न सिर्फ हमारा मुक्तिदाता है, बल्कि वह हमारा अग्रदूत भी है (इब्रा. 6:20)। हर समय और हर परिस्थितियों में हमें परमेश्वर के सिद्ध आज्ञापालन में कैसे जीना है, इसका उदाहरण उसने हमारे सामने रखा है।
पापों की क्षमा, पवित्र-आत्मा की भरपूरी, और परमेश्वर द्वारा दिए गए कृपा के वे सारे माध्यम जो उसने हमें दिए हैं, उनका सिर्फ एक ही लक्ष्य है - कि हम उसके पुत्र की समानता में बदल जाएं। असल में, परमेश्वर के वचन का हरेक सिद्धान्त उसके सही संदर्भ में सिर्फ तभी समझा जा सकता है जब उसे मनुष्य के लिए परमेश्वर के अनन्त उद्देश्य के संदर्भ की ज्योति में देखा जाता है - कि उसे यीशु के समान बना दे।
पवित्र-आत्मा की दोहरी सेवकाई है जिसका बयान इस तरह किया गया हैः "हम सब खुले चेहरे से मानो प्रभु के तेज को दर्पण में देखते हुए, आत्मा के द्वारा उसी तेजस्वी रूप में अंश-अंश करके बदलते जाते हैं" (2 कुरि. 3:18)।
पवित्र-आत्मा दर्पण (पवित्र-शास्त्र) में हमें लगातार प्रभु यीशु की महिमा दिखाना चाहता है, और फिर हमें उसकी समानता में बदल देना चाहता है।
परमेश्वर पिता भी उसके सर्वसत्ताधिकार में, हमारे सारे हालातों को इसी उद्देश्य को पूरा करने के लिए तैयार करता है। "जो परमेश्वर से प्रेम करते हैं, उनके लिए वह सब बातों को मिलाकर भलाई उत्पन्न करता है... जिन्हें उसने पहले से जाना है, उनके लिए उसने पहले से यह भी ठहराया है कि वे उसके पुत्र की समानता में बदल जाएं" (रोमि. 8:28,29)।
हमारे जीवन की हरेक घटना और हरेक हालात में परमेश्वर का हमारे लिए यही उद्देश्य होता है कि उनमें ढालते हुए वह हमें थोड़ा और मसीह की समानता में बदल दे।
इस तरह, हम देखते हैं कि स्वर्ग में हमारा पिता और हमारे हृदय में पवित्र आत्मा सिर्फ एक ही लक्ष्य प्राप्त करने के लिए काम कर रहे हैं - कि हम यीशु जैसे हो जाएं।
हम जितना अपने प्रभु के स्वभाव में सहभागी होते हैं, हम उतना ही पृथ्वी पर उसकी तरह जीवन व्यतीत कर सकेंगे। यह आत्मा से भरा जीवन है।
पृथ्वी पर यीशु एक स्वर्गदूत के रूप में नहीं बल्कि हमारे जैसा आया था। बाइबल कहती है, "वह सब बातों में अपने भाइयों के समान बना" (इब्रा. 2:17)। उसके भाई उसके शिष्य हैं - मत्ती 12:50)। अगर वह "सब बातों में" हमारे (उसके भाइयों) की तरह न बना होता, तो वह हमारा आदर्श उदाहरण भी न बन पाता। और न ही वह हमें यह आज्ञा दे पाता, "मेरे पीछे चलो," क्योंकि यह स्पष्ट है कि हम किसी व्यक्ति के पीछे नहीं चल सकते थे जो हमारी ही तरह एक सीमित दशा में न होता, वैसे ही जैसे एक स्वर्गदूत हमें तैरना नहीं सिखा सकता क्योंकि वह हमारी तरह नीचे की तरफ खींच लेने वाले गुरुत्वाकर्षण को महसूस नहीं करता है।
तब पहला कुरिन्थियों 11:1 में पौलुस का वह उपदेश अर्थहीन होता कि जैसे तुम मेरे पीछे चलो जैसे मैं मसीह के पीछे चलता हूँ, क्योंकि तब पौलुस के लिए यीशु की तरह जीवन व्यतीत कर पाना सम्भव न होता। तब मसीह का जीवन एक ऐसा जीवन होता जिसकी हम सराहना तो कर पाते लेकिन उसका अनुसरण कभी न कर पाते।
लेकिन परमेश्वर की स्तुति हो कि मसीह हमारी देह में आया, और हमारी देह की सीमित अवस्था को स्वीकार करने द्वारा, उसने हमें एक ऐसा उदाहरण दिया जिसका हम अनुसरण कर सकते हैं।
यीशु ने क्योंकि एक मनुष्य होते हुए, एक पवित्र और शुद्ध जीवन व्यतीत किया, इसलिए ऐसा कोई कारण नहीं कि हम भी यह न कर सकें कि "जैसे वह चलता था, वैसे ही हम भी चलें" (1 यूहन्ना 2:6)।
मनुष्य होते हुए क्योंकि हम कमज़ोर हैं, इसलिए परमेश्वर हमें पवित्र आत्मा की वही सामर्थ्य प्रदान करता है जो यीशु को उस समय दी गई थी जब वह पृथ्वी पर एक मनुष्य बन कर रहा था।
परमेश्वर ने जो यीशु के लिए किया, वही वह सहर्ष हमारे लिए भी करेगा, क्योंकि वह "हमें भी वैसा ही प्रेम करता है जैसा उसने यीशु से किया है" (यूहन्ना 17:23)। लेकिन उसकी सामर्थ्य सिर्फ उनके लिए है जो "विश्वास करते हैं" (इफि. 1:19)। परमेश्वर के वचन में विश्वास न होने की वजह से ही आज विश्वासी पाप और शैतान के खिलाफ़ पौरुषहीन और शक्तिहीन हैं। जबकि हमें यह आज्ञा दी गई है कि "हम उसके पद्चिन्हों पर चलें जिसने कभी कोई पाप नहीं किया," फिर भी शैतान हमें ऐसा बहाना बनाने वाला बना देता है कि क्योंकि हम मनुष्य हैं, इसलिए हम कभी-कभी तो पाप ज़रूर करेंगे। लेकिन जब हम यह देखते हैं कि यीशु मनुष्य की देह में आया और उसने कोई पाप नहीं किया, तब दो बातें होती हैंः
(1) हमारे पास फिर पाप करने के लिए कोई बहाना नहीं रह जाता।
(2) हममें यह विश्वास आ जाता है कि यीशु की तरह हम भी पाप पर जय पाने वाला जीवन जी सकते हैं।
इसलिए, इस पुस्तक में जब आप वचन के सत्यों को पढ़ेंगे, तो मैं भी पौलुस की प्रार्थना करता हूँः "हमारे प्रभु यीशु का परमेश्वर, जो महिमा का पिता है, तुम्हें अपनी पूर्ण पहचान (मसीह) में ज्ञान और प्रकाशन का आत्मा दे... और वह अपनी महिमा के धन के अनुसार तुम्हें यह दान दे कि तुम उसके आत्मा के द्वारा अपने भीतर मनुष्यत्व में सामर्थ्य पाकर बलवान होते जाओ" (इफि. 1:17; 3:16)।
मसीह के पूर्ण ज्ञान द्वारा ही हम पवित्र आत्मा की सामर्थ्य को जान सकते हैं। यीशु पवित्र-आत्मा से भरे मनुष्य का एक सिद्ध उदाहरण है।
अब हम जैसे-जैसे उसके जीवन को देखेंगे और यह कि उसने पृथ्वी पर कैसे जीवन बिताया था, तब हम एक स्पष्ट रूप में यह देख सकेंगे कि पवित्र-आत्मा से भरे एक जीवन की विशिष्टताएं क्या होती हैं।
संसार के लोगों को परमेश्वर की महानता उन्हें विस्मित कर देने वाली सृष्टि में नज़र आती है (भजन. 19:1)। पूरा ब्रह्माण्ड इतना विशाल है कि मानवीय बुद्धि उसे नहीं समझ सकती। पूरे अंतरिक्ष में तारों की आकाश-गंगाएं एक-दूसरे से अरबों प्रकाश-वर्षों की दूरी पर बिखेरी हुई हैं। इसके साथ ही, सृष्टि के सारे तत्व ऐसे सूक्ष्म अणुओं से रचे गए हैं जिन्हें आँख से देखा नही जा सकता, फिर भी उनके अन्दर सैंकड़ों विद्युदणु (इलैक्ट्रोन) परिक्रमा करते रहते हैं। हमारा परमेश्वर कितना महान् हैं!
लेकिन यीशु मसीह के शिष्य के लिए, परमेश्वर की महानता प्राथमिक रूप में सृष्टि की इन अद्भुत बातों में नहीं है, बल्कि उस नम्रता में है जिसने परमेश्वर के पुत्र को स्वयं उसमें से उसे ख़ाली कराया और तब वह हमारी देह में होकर हमारी गिरी हुई इंसानी नस्ल के साथ अपने आपको एक कर सका।
"वचन देहधारी हुआ, और हमारे बीच में निवास किया, और हमने उसकी महिमा को देखा," प्रेरित यूहन्ना ने कहा (यूहन्ना 1:14)। और हम इसमें यह जोड़ सकते हैं, "ऐसी महिमा जिसने उस महिमा को बिलकुल फीका कर दिया जो सृष्टि में नज़र आती है।"
स्वर्ग का महान् राजा हमारी देह में हमारे जैसा बनकर हमारे बीच में रहा। और उसका आना हमें नीचा दिखाने वाले या हमारा सरपरस्त होने वाले मनोभाव में नहीं था, बल्कि वास्तविक नम्रता में था, जिसमें उसने अपने आपको हर तरह से हमारे साथ एक कर लिया था।
हम प्रभु यीशु की महिमा उसके द्वारा किए गए अद्भुत चमत्कारों से भी कहीं बढ़कर उसकी नम्रता में देख सकते हैं।
पवित्र आत्मा सबसे पहले नम्रता का यही मार्ग हमें दिखाना चाहता है कि हम अपने सब दिनों में इसमें चलना सीख सकें। हमें प्राथमिक रूप में यहीं यीशु के पीछे चलना है।
इससे पहले कि यीशु ने एक मनुष्य के रूप में इस पृथ्वी पर एक शुद्ध और प्रेम-भरा जीवन बिताया, उसने अपने आपको नम्र व दीन किया। यह पहला क़दम था। और हमारे लिए भी यही पहला क़दम है।
यीशु के पृथ्वी पर आने से हज़ारों साल पहले, परमेश्वर ने लूसीफर नाम के एक स्वर्गदूत की रचना की थी जो बुद्धि में सिद्ध और सर्वांग सुन्दर था। स्वर्गदूतों की रचना के क्रम में परमेश्वर ने उसे शीर्ष स्थान पर रखा था। लेकिन घमण्डी और असंतुष्ट होकर उसने अपने निर्धारित स्थान से और ज़्यादा ऊँचा होना चाहा (यहेजकेल 28:11-17; यशा. 14:12-15)। इस तरह, परमेश्वर की सृष्टि में वह पाप का मूल स्रोत् बन गया। परमेश्वर ने उसे तुरन्त नीचे फेंक दिया और वह शैतान बन गया।
इसलिए इस सारे ब्रह्माण्ड में हरेक पाप और बुराई का मूल घमण्ड है।
जब आदम ने पाप किया, तब उसमें भी इस शैतानी घमण्ड का संक्रमण हो गया।
आदम की हरेक संतान इस संक्रामक रोग के साथ पैदा होती है।
मनुष्य के अन्दर से इस ज़हर को मिटाने के लिए, यीशु ने अपने आपको नम्र व दीन किया।
जैसे पाप का आरम्भ लूसीफर के घमण्ड में हुआ था, वैसे ही हमारे छुटकारे का आरम्भ यीशु की नम्रता में हुआ है। हममें मसीह का उतना ही मन होता है जितनी हममें उसकी नम्रता व दीनता होती है। आत्मिक उन्नति का यह एक अचूक मापदण्ड है।
यीशु का स्वर्ग की महिमा को छोड़ पृथ्वी पर आना ही अपने आपमें उसकी नम्रता का अद्भुत प्रदर्शन है। लेकिन हमें इससे भी आगे बढ़कर यह बताया गया है कि "उसने मनुष्य के रूप में उसने अपने आपको दीन किया" (फिलि. 2:8)। "सब बातों में अपने भाइयों के समान बनाए जाकर" (इब्रा. 2:17), परमेश्वर के सम्मुख वह सब मनुष्यों के समान होकर आ खड़ा हुआ। वह कुछ-नहीं बना कि परमेश्वर सब-कुछ बन सके। यह सच्ची नम्रता है।
सांसारिक महिमा और महानता का मूल्यांकन एक व्यक्ति की धन-सम्पत्ति, उसकी उपलब्धियों, और पारिवारिक मान-मर्यादा आदि, द्वारा होता है। लेकिन यीशु मसीह में नज़र आने वाली परमेश्वर की महिमा कितनी अलग है! पृथ्वी पर जन्म लेने वालों में सिर्फ यीशु ही एक ऐसा व्यक्ति हुआ है जिसके पास यह चुनाव करने का मौक़ा था कि वह किस परिवार में जन्म ले। हममें से किसी के पास यह चुनाव नहीं था।
यीशु ने कैसा परिवार चुना था? उसने एक ऐसे अज्ञात बढ़ई का परिवार चुना जो नासरत नाम की एक जगह में रहता था - एक ऐसी बस्ती जिसके बारे में लोगों का यह कहना था, "भला नासरत में से भी कोई भली वस्तु निकल सकती है?" (यूहन्ना 1:46)। युसुफ और मरियम इतने ग़रीब थे कि होमबलि के रूप में वे परमेश्वर को एक मेमना भी अर्पित नहीं कर सकते थे (तुलना करें लूका 2:22-24 के साथ लैव्य. 12:8)।
इसके अलावा, जन्म लेने वालों में सिर्फ यीशु ही एक ऐसा व्यक्ति जन्मा है जो अपने जन्म लेने के स्थान का अचूक चुनाव कर सकता था। अपने जन्म लेने की जगह तय करने का मौक़ा होते हुए, यीशु ने कौन सी जगह चुनी थी? एक तुच्छ गौशाला में पशुओं के चारे की चरनी!
आगे और ध्यान दें, कि अपने लिए यीशु ने जिस परिवार को चुना था उसकी पृष्ठभूमि कैसी थी। यीशु के पारिवारिक-वृक्ष में मत्ती 1:3-6 में चार स्त्रियों के नाम दिए गए हैं। पहली, तामार है जिसने अपने ससुर यहूदा के साथ व्यभिचार करने द्वारा एक पुत्र को जन्म दिया था। दूसरी, राहाब है जो यरीहो में एक कुख्यात वेश्या थी। तीसरी, रुत है जो मोआब की वंशज थी जो लूत द्वारा उसकी अपनी पुत्री के साथ व्यभिचार करने से पैदा हुआ था। चौथी, ऊरिय्याह की पत्नी बतशेबा है जिसके साथ दाऊद ने व्यभिचार किया था।
यीशु ने अपने आने के लिए ऐसी लज्जाजनक पारिवारिक पृष्ठभूमि क्यों चुनी थी? इसलिए कि वह आदम की पतित नस्ल के साथ अपनी पूरी पहचान बना सके। हम इसमें उसकी नम्रता को देखते हैं। उसने अपने परिवार या वंशावली में किसी प्रकार का घमण्ड करने की अभिलाषा नहीं की थी।
यीशु ने मनुष्य के साथ अपनी पूरी पहचान बनाई। नस्ल, परिवार, या पार्थिव पद-प्रतिष्ठा आदि असमानताओं को अनदेखा करते हुए, उसे यक़ीन था कि सब मनुष्य उनके मूल रूप में बराबर हैं, और इसलिए वह सामाजिक स्तर पर जो सबसे नीचे और सबसे छोटे थे, वह उनके साथ एक हो गया। वह सबसे नीचा हो गया कि वह सबका सेवक बन सके। जो दूसरों के नीचे झुकता है, वही उन्हें ऊँचा उठा सकता है। और यीशु इस तरह आया था।
पवित्र आत्मा हमारे मन के नए हो जाने से हमें बदलता है (रोमि. 12:2)। सच्ची मसीह-समान नम्रता दीनता के बीज हमारे मन में के विचारों में बोए जाते हैं। दूसरों के सामने किए जाने वाले हमारे काम या हमारा व्यवहार नहीं, बल्कि हमारे विचार (जब हम अपने साथ अकेले होते हैं) यह सुनिश्चित करते हैं कि हम इस क्षेत्र में मसीह-समान बन रहे हैं या नहीं - इसमें कि हमारे अपने बारे में हमारे क्या विचार हैं, और इसमें कि दूसरों की तुलना में हम कैसे हैं।
जब हम वास्तव में अपने विचारों में अपने आपको छोटा कर लेते हैं, सिर्फ तभी ऐसा हो सकता है कि हम वास्तव में "अपनी अपेक्षा दूसरों को उत्तम समझ सकते हैं" (फिलि. 2:3), और अपने आपको "सब संतों में छोटे से भी छोटा मान सकते हैं" (इफि. 3:8)।
एक मनुष्य के रूप में यीशु ने पिता के सम्मुख अपने आपको कुछ नहीं माना था। इस वजह से ही उसके द्वारा पिता की महिमा अपनी परिपूर्णता में प्रकट हो सकी थी।
यीशु ने क्योंकि पिता के सम्मुख कुछ-न-होने की इस दशा को स्वीकार किया था, इसलिए वह पिता द्वारा उसके जीवन के लिए ठहराई गई हरेक बात के सहर्ष अधीन हो सका और पूरे हृदय से पिता की आज्ञाओं का पालन कर सका।
"उसने स्वयं को दीन किया और यहाँ तक आज्ञाकारी रहा कि उसने मृत्यु भी सह ली" (फिलि. 2:8)।
परमेश्वर के प्रति पूरा आज्ञापालन असली नम्रता का स्पष्ट चिन्ह् होता है। इससे स्पष्ट और कोई परख नहीं होती।
तीस साल तक, यीशु अपने त्रुटिपूर्ण पालक माता-पिता के अधीन रहा था, क्योंकि यह उसके पिता की इच्छा थी। उसका ज्ञान युसुफ और मरियम से बहुत बढ़कर था, और वह उनकी तरह पापी नहीं था। फिर भी वह उनके अधीन हो गया था।
एक मनुष्य के लिए ऐसे लोगों के अधीन होना आसान नहीं होता जो बौद्धिक या आत्मिक रूप में उससे कम होते हैं। लेकिन असली नम्रता को ऐसा करने में कोई तकलीफ नहीं होती - क्योंकि जिसने यह देख लिया है कि वह परमेश्वर की दृष्टि में कुछ भी नहीं है, उसे ऐसे किसी भी मनुष्य के अधीन होने में कोई कष्ट नहीं होता जिसे परमेश्वर उसके ऊपर नियुक्त करता है।
यीशु ने जो व्यवसाय अपने लिए चुना, वह भी बहुत सामान्य था - एक बढ़ई का काम। और जब उसने अपनी सार्वजनिक सेवकाई शुरू की, तब उसके नाम के आगे या पीछे कोई शीर्षक या पदवी नहीं थी। वह "पास्टर यीशु" नहीं था। और वह "रेवरेन्ड डॉक्टर यीशु" तो हर्गिज़ नहीं था! उसने ऐसे किसी पार्थिव पद या शीर्षक की कभी इच्छा और अभिलाषा नहीं की थी जो उसे उन आम लोगों से ऊँचा उठा देते जिनकी वह सेवा करने के लिए आया था। जिसके सुनने के कान हों वह सुनें।
एक बार जब एक बड़ी भीड़ ने उसे घेर लिया और उसे अपना राजा बनाना चाहा, तो वह ख़ामोशी से उनके बीच में से निकल गया (यूहन्ना 6:15)। वह सिर्फ "मनुष्य का पुत्र" कहलाना चाहता था।
उसने मनुष्यों से न तो सम्मान पाना चाहा और न ही उसने उनके सम्मान की परवाह की। वह सिर्फ अपने पिता के सम्मुख रहता था, और वह इस बात में भी पूरी तरह संतुष्ट था कि उसके पूरे जीवन-भर मनुष्य उसकी उपेक्षा करते रहें और उसे तुच्छ समझते रहें। उसके लिए सिर्फ पिता का अनुमोदन ही सब कुछ था।
यीशु ने जब भी किसी को चंगा किया या कोई चमत्कार किया, तो वह चाहता था कि कोई उस चंगाई के बारे में न जाने, क्योंकि उसके चमत्कार संवेदना के ऐसे काम होते थे जो ज़रूरतमंद व्यक्तियों के लिए किए जाते थे; वे कोई सार्वजनिक तमाशा नहीं होते थे। यीशु ने जब याईर की बेटी को मृतकों में से जीवित किया, तब भी उसने यह निर्देश दिया था कि इसकें बारे में किसी को न बताना। (मरकुस 5:43)। यीशु के पृथ्वी से जाने के बाद ही उसके शिष्यों ने उसके जीवन के लेखे को सार्वजनिक रूप में प्रकट किया था।
सूली पर चढ़ाए जाने की पिछली रात, जब उसने एक बर्तन मे पानी लेकर अपने शिष्यों के पैर धोए, तो यह उसी बात का एक प्रतीकात्मक स्वरूप था जो उसके पूरे जीवन-भर एक यथार्थ रूप में थी। वह सब मनुष्यों का सेवक बन कर रहा था। उसने शीघ्र ही यह देख लिया था कि उसके शिष्यों के पैर गंदे थे, और यह इंतज़ार करने की बजाय कि कोई दूसरा यह करे, उसने उतनी ही शीघ्रता से बर्तन में पानी लेकर वह किया जो करना ज़रूरी था। उसका वह काम उसके जीवन-भर की सेवा का प्रतीक था। यीशु इस बात का इंतज़ार नहीं करता था कि कोई उसे कुछ करने के लिए कहे। वह ज़रूरत को देख लेता था, और फिर वह करता था जो ज़रूरी होता था।
यीशु समाज के निचले वर्ग के लोगों के साथ नज़दीकी के साथ जुड़ा रहता था और उनके बीच में ऐसे रहता था मानो वे उसके बराबर हों। स्वयं निष्पाप और सिद्ध होते हुए भी, उसने दूसरों को उनकी कमियों की वजह से कभी नीचा नहीं दिखाया था। अपने शिष्यों के साथ घूमते समय भी वह उन्हें ऐसा महसूस नहीं होने देता था मानो वह उनका सरपरस्त हो। असल में, वह उनके साथ इतनी आज़ादी से रहता था कि वे उसे डाँटने और सलाह देने में भी स्वयं को आज़ाद महसूस करते थे (मत्ती 16:22; मरकुस 4:38; 9:5)।
प्रार्थना में अपने शिष्यों की संगति की अभिलाषा करने में हम यीशु की नम्रता देखते हैं। गतसमनी के बाग़ में, उसने पतरस, याकूब, और यूहन्ना से उसके लिए प्रार्थना करने के लिए कहा क्योंकि उसका जीव "बहुत उदास था और वह मरने पर था" (मत्ती 26:38)। जो शरीर यीशु ने धारण किया था, वह उसकी निर्बलताओं से भली-भांति परिचित था। इस वजह से ही वह प्रार्थना में उनकी सहभागिता का इच्छुक था।
हम क्योंकि अपने कुछ-न-होने की बात को स्वीकार करने में ईमानदार नहीं होते, इसलिए हममें से परमेश्वर की सामर्थ्य एक सीमित रूप में ही काम कर पाती है। यीशु ने हमें नम्रता का रास्ता दिखाया है। यह हमारे शरीर का निर्बल होना, और मनुष्यों के रूप में हमारे कुछ-न-होना है।
यीशु ने क्योंकि अपने आपको नम्र व दीन किया था, इसलिए परमेश्वर ने उसे सारे ब्रह्माण्ड में उसे सबसे ऊँचा पद दिया है (फिलि- 2:9)। जो नम्रता के मार्ग में सबसे आगे निकल जाते हैं, वे यीशु के साथ महिमा में उसके दाएं और बाएं बैठेंगे।
उसके पूरे जीवन-भर यीशु नीचा ही होता रहा था। वह स्वर्ग से नीचे आया था, और फिर वह नीचा, नीचा और नीचा होता हुआ सूली तक पहुँच गया था। उसने एक बार भी उस रास्ते से अलग होकर ऊपर जाना नहीं चाहा था।
पृथ्वी के ऊपर आज सिर्फ दो ही आत्माएं काम कर रही हैं। एक, शैतान (लूसीफर) की आत्मा है जो लोगों को ऊपर जाने का आग्रह करती है - चाहे वह संसार में हो या मसीही जगत में। दूसरी, मसीह की आत्मा है जो उनके स्वामी की तरह लोगों को नीचे की तरफ ले जाती है। गेहूँ के दाने की तरह, यीशु नीचे गया था, और उसके सभी सच्चे शिष्यों को उनके इस गुण द्वारा आसानी से पहचाना जा सकता है।
यीशु की नम्रता के पूरे वैभव को उसकी मृत्यु में देखा जा सकता है। जैसे अन्याय से भरे मुक़द्दमे में से यीशु को गुज़रना पड़ा, था, वैसे अन्याय से भरा मुक़द्दमा इस पृथ्वी पर दूसरा नहीं हुआ है। फिर भी उसने ख़ामोशी से सारे घाव, अपमान, अन्याय, तिरस्कार और निन्दा को सह लिया था। उसने अपने शत्रुओं को कोई श्राप नहीं दिया। उसने उनसे बदला लेने की धमकी भी नहीं दी और स्वर्गदूतों को भी उसकी मदद के लिए नहीं बुलाया। उसने परमेश्वर का पुत्र होने के अपने सारे विशेषाधिकारों को त्याग दिया था।
"बंधी हुई मुट्ठी" मानव-जाति के लिए एक उपयुक्त चिन्ह् है - यह अपने अधिकारों, शक्तियों और वस्तुओं को पकड़े रहने का, और हमला होने पर वापिस हमला करने के मज़बूत इरादे का भी प्रतीक है।
दूसरी तरफ, यीशु ने सूली पर कीलें ठुकवाने के लिए अपनी मुट्ठी को खोल दिया था। उसका हाथ हमेशा खुला रहा था, हमेशा देता, देता और देता ही रहा था। अंत में उसने अपना जीवन भी दे दिया था। यह सच्ची नम्रता है। और यही वह सच्चा "पौरुष" है जो परमेश्वर चाहता है।
यीशु का जो शिष्य ईश्वरीय स्वभाव अभिव्यक्त करना चाहता है, उसे कोई शिकायत किए बिना अन्याय सहने के लिए तैयार रहना चाहिए।
बाइबल कहती हैः "अगर तुम सही काम करने पर भी सताए जाते हो और धीरज से वह सहते हो जिसके योग्य तुमने कुछ नहीं किया है, तो वह परमेश्वर प्रसन्न होकर स्वीकार करता है - क्योंकि तुम यही करने के लिए बुलाए गए हो - यह तुम्हारे काम का एक ऐसा हिस्सा है जिसे तुम अलग नहीं कर सकते। क्योंकि मसीह ने भी पीड़ा सही... और वह तुम्हारे लिए अपना व्यक्तिगत उदाहरण छोड़ गया है कि अब तुम उसके पद्चिन्हों पर चल सको। ...उसने गाली सुनते हुए गाली नहीं दी, दुःख सहते हुए धमकियाँ नहीं दीं, बल्कि अपने आपको और सब बातों को उसके भरोसे पर छोड़ दिया जो सच्चा न्याय करता है" (1 पत. 2:20-23-ऐम्प्लिफाइड)।
यीशु की नम्रता ने उसे कभी किसी का न्याय करने की अनुमति नहीं दी। सिर्फ परमेश्वर ही सब मनुष्यों का न्याय करने वाला है; और जो भी मनुष्य दूसरे का न्याय करता है, वह स्वयं को उस जगह पर ला खड़ा करता है जो सिर्फ परमेश्वर की जगह है। पृथ्वी पर एक मनुष्य होते हुए, यीशु ने कहा, "मैं किसी मनुष्य का न्याय नही करता" (यूहन्ना 8:15)। उसने सारा न्याय अपने पिता के हाथ में सौंप दिया था। वहाँ भी हम उसकी नम्रता की ख़ूबसूरती देखते हैं।
यीशु ने स्वेच्छा से अपने आपको उस अपमानजनक मृत्यु के अधीन कर दिया जिसकी योजना उसके पिता ने उसके लिए बनाई थी। उसे सूली पर चढ़ाने की योजना बनाने और उस योजना को कार्यान्वित करने वाले उन मानवीय पात्रों के आगे, यीशु उसके पिता के हाथ को देख रहा था, और उसने स्वेच्छा से उस प्याले को पी लिया जो उसे "पिता ने दिया था" (यूहन्ना 18:11)।
"वह मृत्यु सहने तक, हाँ, सूली की मृत्यु सहने तक आज्ञाकारी रहा था" (फिलि. 2:8)।
यह पवित्र शास्त्रों का वास्तविक यीशु है। आधुनिक सुसमाचार-प्रचारकों की तरह, उसका एक महानुभाव या फिल्मी सितारे की तरह सम्मान नहीं किया गया था। इसके विपरीत, वह मनुष्यों द्वारा तुच्छ जाना गया था और उसे अस्वीकार कर दिया गया था; और उसके समय के संसार ने उसे सूली पर चढ़ाने द्वारा उससे अपना पीछा छुड़ा लिया था। आज का संसार भी वैसा ही है, और शिष्य अपने गुरू से बड़ा नहीं होता। ऐसी मसीहियत जो लोकप्रिय है और जो संसार में आदर-सम्मान पाती है, वह असली विश्वास की नकल है। यीशु का पूरा जीवन - उसके जन्म से लेकर उसकी मृत्यु तक - इस हक़ीक़त को दर्शाता रहा था कि "वह जो मनुष्यों में अति सम्मानित है, परमेश्वर की दृष्टि में घृणित है" (लूका 16:15)।
"मुझसे सीखो", यीशु ने कहा, "क्योंकि मैं मन में नम्र व दीन हूँ" (मत्ती 11:29)। अपने शिष्यों से यीशु ने कहा कि उन्हें जो मुख्य बात उससे सीखनी है, वह नम्रता है। और यही बात हमें भी उससे सीखनी है।
"परमेश्वर ज्योति और प्रेम है" (1 यूहन्ना 1:5; 4:8)। "वह अगम्य ज्योतियों में वास करता है" (1 तीमु. 6:16)। वह क्योंकि पवित्र है, इसलिए वह हमें भी पवित्र होने के लिए बुलाता है।
लेकिन मनुष्य के लिए पवित्रता सिर्फ परीक्षा में से ही आ सकती है। आदम उसकी रचना के समय दोषरहित था; वह तो भला और बुरा भी नहीं जानता था। परमेश्वर चाहता था कि वह पवित्र हो, और इसलिए परमेश्वर ने उसे परीक्षा में से गुज़रने दिया।
भले और बुरे के ज्ञान का वृक्ष स्वयं परमेश्वर द्वारा रचा गया था और अपने आप में उसमें कोई बुराई नहीं थी। वह एक ऐसे संसार में खड़ा था जिसे परमेश्वर ने फ्बहुत अच्छाय् घोषित किया था (उत्पत्ति 1:31)। वह बहुत अच्छा था, क्योंकि प्रलोभन का विरोध करने द्वारा वह आदम को पवित्र होने का मौक़ा देता था।
बाइबल कहती है, "जब तुम विभिन्न परीक्षाओं का सामना करो, तो इसे आनन्द की बात समझो" (याकूब 1:2) क्योंकि परीक्षाएं हमें परमेश्वर की पवित्रता में सहभगी होने का मौक़ा देती हैं (इब्रा. 12:10) और हमें "पूर्ण और सिद्ध" बनाती हैं (याकूब 1:4)।
जब हम यीशु की पवित्रता की तरफ देखते हैं, तो हम परमेश्वर होने के उसके उत्तराधिकार में अंतर्निहित पवित्रता की तरफ नहीं देखते, क्योंकि वह हमारे लिए एक नमूना नहीं हो सकता। हम उसकी ओर ऐसे देखते हैं "जो सब बातों में अपने भाइयों के समान बना" और "सब बातों में हमारी ही तरह परखा गया, फिर भी निष्पाप रहा" (इब्रा. 2:17; 4:15)।
यीशु हमारा अग्रदूत है (इब्रा. 6:20), जो उसी दौड़ में दौड़ा है जिसमें हमें दौड़ना है, और वह हमारे लिए रास्ता बना गया है। और इसलिए वह हमसे कहता है, "मेरे पीछे चलो" (यूहन्ना 12:26)। और उस पर दृष्टि लगाए रखते हुए जो हमसे पहले दौड़ा है, हम भी थके या हारे बिना धीरज से सहते हुए दौड़ सकते हैं (इब्रा. 12:1-4)।
जिसका सामना किसी भी मनुष्य को करना पड़ सकता है, यीशु ने ऐसी हरेक परीक्षा/प्रलोभन का सामना किया था। इब्रानियों 4:15 में यह स्पष्ट सिखाया गया है कि वह "सब बातों में हमारे ही समान परखा गया।" और यही बात हमें उत्साहित करती है। जो शक्ति आज परमेश्वर ने हमें दी है, यीशु ने उससे बढ़कर किसी शक्ति का इस्तेमाल नहीं किया था। एक मनुष्य के रूप में, उसने परीक्षा/प्रलोभन का सामना किया, और उस शक्ति से उस प्रबल हुआ जो उसे पवित्र आत्मा द्वारा पिता ने दी थी।
शैतान ने मनुष्य को हमेशा यही बताया है कि परमेश्वर के नियमों का बोझ बहुत भारी है और उनका पालन करना असम्भव है। यीशु एक मनुष्य के रूप में आया और उसने अपने सिद्ध आज्ञापालन द्वारा शैतान के इस झूठ का पर्दाफाश कर दिया। अगर हमें किसी ऐसी परीक्षा में प्रबल होना हो, या परमेश्वर की किसी ऐसी आज्ञा का पालन करना हो जिसका सामना यीशु ने न किया हो, तब उस मामले में हमारे पास पाप करने का बहाना हो सकता है। और अगर यीशु ने वह सिद्ध जीवन हमारी शारीरिक निर्बलता के बिना या उस शक्ति द्वारा बिताया होता जो हमें उपलब्ध नहीं है, तब उसका जीवन हमारे लिए एक अनुकरणीय उदाहरण नहीं हो सकता था, और न ही हमारी परीक्षा के क्षणों में वह हमें उत्साहित कर सकता था। लेकिन पृथ्वी पर एक मनुष्य के रूप में यीशु ने यह प्रदर्शित किया कि जो सामर्थ्य परमेश्वर ने हमें उपलब्ध कराई है, वह उस व्यवस्था को पूरा करने के लिए काफी है जो हम उसके वचन में पाते हैं।
"हमारा ऐसा महायाजक नहीं है जो हमारी निर्बलताओं में हमसे सहानुभूति न रख सके, क्योंकि वह सब बातों में हमारे ही समान परखा गया था" (इब्रा. 4:15)। यीशु के निष्पाप जीवन द्वारा परमेश्वर ने जगत के सामने यह प्रदर्शित किया कि पवित्र आत्मा की सामर्थ्य द्वारा पाप पर जय पाना और आनन्दपूर्वक परमेश्वर का आज्ञापालन करना सम्भव है। अगर हम उसमें बने रहें, तो हम भी "वैसे ही चल सकते हैं जैसे वह चला था" (1 यूहन्ना 2:6)।
यीशु ने पाप के उन सारे प्रलोभनों का सामना किया था जिनसे आज हमारा सामना होता है, और वह उसके पिता द्वारा हरेक उस परीक्षा में से गुज़ारा गया जिसका सामना आज किसी भी मनुष्य को करना पड़ सकता है। वह हमारा अगुवा और महायाजक होने की योग्यता से सुसज्जित था (इब्रा. 2:10,17,18; 5:7,9)। इन सभी परिस्थितियों में, उसने अपनी ख़ुदी से इनकार किया था और उसे पाप करने के लिए प्रलोभित करने वाली लालसाओं को कुचला था। इस तरह, उसने लगातार "शरीर में पीड़ा भोगी थी।"
पवित्र शास्त्र हमारा उदाहरण होने के लिए यीशु की तरफ संकेत करता हैः "इसलिए, जबकि मसीह ने शरीर में दुःख उठाया, तो तुम भी इसी अभिप्राय से हथियार धारण करो, क्योंकि जिसने शरीर में दुःख उठाया है, वह पाप से छूट गया है, कि अब वह शरीर में अपना शेष जीवन मनुष्यों की अभिलाषाओं में नहीं वरन् परमेश्वर की इच्छानुसार व्यतीत कर सके" (1 पत. 4:1,2)। यीशु ने "मृत्यु तक विश्वासयोग्य" रहने वाले अपने जीवन के द्वारा यह प्रदर्शित किया कि कोई भी विपत्ति उस विपत्ति से बड़ी नहीं हो सकती जो एक बात में भी परमेश्वर की आज्ञा न मानने द्वारा हम पर आ सकती है।
सारे पाप का मूल अपने स्वयं की इच्छा पूरी करने में पाया जाता है। और पवित्रता का मूल इसमें है कि हम अपनी इच्छा पूरी करने से इनकार करते हुए परमेश्वर की इच्छा पूरी करें। यीशु ने इस तरह ही जीवन व्यतीत किया था।
उसने कहा, "मैं अपनी नहीं, वरन् अपने भेजने वाले की इच्छा चाहता हूँ... मैं अपनी इच्छा नहीं बल्कि अपने भेजने वाले की इच्छा पूरी करने के लिए स्वर्ग से उतरा हूँ... मेरी नहीं, पर तेरी इच्छा पूरी हो" (यूहन्ना 5:30; 6:38; मत्ती 26:39)।
यीशु अपनी स्वयं की मानवीय इच्छा को एक चिरस्थाई बलिदान के रूप में अपने पिता को अर्पित करता रहा था, चाहे इसका अर्थ घोर पीड़ा सहना भी क्यों न था। हमें बताया गया है, "अपनी देह में रहने के दिनों में, मसीह ने उससे जो उसे मृत्यु से बचा सकता था उच्च स्वर में पुकारकर आँसू बहा-बहाकर प्रार्थनाएं और विनतियाँ कीं" (इब्रा. 5:7)।
गतसमनी के बाग़ में यीशु ने अपने तीन शिष्यों को यह चेतावनी दी थी कि क्योंकि मनुष्य का शरीर कमज़ोर है, इसलिए सिर्फ जागते रहने और प्रार्थना करते रहने (मतलब, मदद के लिए परमेश्वर को पुकारते रहने) द्वारा ही परीक्षाओं पर जय पाई जा सकती थी (मत्ती 26:41)। वह स्वयं प्रार्थना करता रहता था, और इस तरह से ही वह प्रबल हो सका था।
गतसमनी में जाने से कुछ देर पहले ही उसने अपने शिष्यों से कहा था कि वह दिन जल्दी ही आ जाएगा जब वे भी वही काम कर सकेंगे जो वह करता था, क्योंकि पिता उन्हें भी उनका "सहायक" होने के लिए उन्हें पवित्र आत्मा देगा (यूहन्ना 14:12,16)। यीशु हमें चिन्ह्-चमत्कार करने वाले बनाने के लिए नहीं आया था; वह हमें पवित्र करने के लिए आया था। उसके काम पवित्रता के काम थे, पिता के आज्ञापालन के काम थे, और यही वे काम थे जिनके लिए उसने हमसे प्रतिज्ञा की कि हम भी वे काम कर सकेंगे। उसने वे सब काम एक ऐसा मनुष्य होते हुए किए थे जो पवित्र आत्मा से भरा हुआ था।
जब पैन्तेकुस्त के दिन शिष्य पवित्र आत्मा से भर गए, तब उन्हें भी, यीशु की तरह, आज्ञापालन के सभी काम करने की सामर्थ्य मिल गई थी। यीशु के पृथ्वी पर रहने के दिनों में, उनके पास बीमारों को चंगा करने, मृतकों को जीवित करने, कोढ़ियों को चंगा करने और दुष्टात्माओं को निकालने की सामर्थ्य थी (मत्ती 10:8), लेकिन उनके पास पाप पर जय पाने की सामर्थ्य नहीं थी। वह पाने के लिए, उन्हें पवित्र आत्मा से भरे जाने का इंतज़ार करना था जो पैन्तेकुस्त के दिन हुआ था।
पवित्र-आत्मा की भरपूरी का उद्देश्य हमें इस योग्य बनाना है कि हम "यीशु के काम करें," या दूसरे शब्दों में, "परमेश्वर की इच्छा पूरी करें" (देखें यूहन्ना 4:34)।
यही जीवन वह नया जीवन है जो देने का प्रस्ताव नई वाचा में परमेश्वर हमारे सामने रखता है।
"क्योंकि जो काम व्यवस्था शरीर के द्वारा दुर्बल होते हुए न कर सकी, उस काम को परमेश्वर ने किया, अर्थात् अपने ही पुत्र को पापमय शरीर की समानता में भेजकर, शरीर में पाप को दोषी ठहराया, जिससे कि व्यवस्था की माँग (परमेश्वर की इच्छा) हममें पूरी हो सके, जो शरीर के अनुसार नहीं, बल्कि आत्मा के अनुसार चलते हैं" (रोमि. 8:3,4)।
यीशु द्वारा प्रलोभनों का सामना करने और उन पर जय पाने में जो बात हमारे लिए महत्व की है, वह यह वास्तविकता है कि उसने हमारे लिए अब ऐसा रास्ता खोल दिया है जिसमें हम उसके पीछे चल सकते हैं।
जिस रास्ते को यीशु ने खोल दिया है, उसे इब्रानियों 10:19,20 में "नया और जीवित मार्ग" कहा गया हैः "अब हमें उस नए और जीवित मार्ग द्वारा उस महापवित्र स्थान में प्रवेश करने का साहस हुआ है जो उसने पर्दे, अर्थात् अपनी देह के द्वारा हमारे लिए खोल दिया है।"
परमेश्वर की महिमा मन्दिर के महापवित्र स्थान में रहती थी। यीशु ने हमारे लिए इस स्थान में प्रवेश करने का रास्ता खोल दिया है, कि हम उसे पीछे चलते हुए इसमें प्रवेश करें और उसकी पवित्रता में सहभागी हो सकें। वह हमारा ऐसा अग्रदूत है जिसने देह के पर्दे में से होकर सबसे पहले प्रवेश किया है (इब्रा. 6:20)। अब हमें यीशु के उदाहरण ओर अपनी दृष्टि लगाए हुए, इस दौड़ को दौड़ते हैं (इब्रा. 12:1,2)।
शरीर में मृत्यु के द्वारा यीशु के जीवन में परमेश्वर की पवित्रता की महिमा को देखा जा सका था। और हमारे लिए भी इसके अलावा दूसरा कोई रास्ता नहीं है। अगर हम फ्यीशु के मरनेय् को अपनी देह में प्रकट करते हैं, तभी, और सिर्फ तभी "यीशु का (वह शुद्ध और पवित्र) जीवन हमारी देह में प्रकट हो सकेगा" (2 कुरि. 4:10)।
हममें बसने वाला पवित्र आत्मा हमारी अगुवाई वैसे ही करेगा जैसी उसने यीशु की अगुवाई की थी, हमेशा सूली की दिशा में बढ़ते रहना। और यही वह रास्ता है जिसमें आगे बढ़ते हुए हम लगातार उसकी पवित्रता में सहभागी होते रहेंगे। ऐसा स्वयं यीशु के साथ हुआ था, और ऐसा ही उन सबके साथ होगा जो इस मार्ग में उसके पीछे चलेंगे।
यीशु इसलिए आया कि वह हमें ईश्वरीय स्वभाव में सहभागी बना सके, कि वही जीवन जो उसमें था, हममें भी हो।
"उसकी ईश्वरीय सामर्थ्य ने उसी के पूर्ण ज्ञान के द्वारा... हमें बहुमूल्य और उत्तम प्रतिज्ञाएं दी हैं कि उनके द्वारा हम उसके ईश्वरीय स्वभाव में सहभागी हो सकें" (2 पत. 1:3,4)।
परमेश्वर ने हमें इस पृथ्वी पर निष्पाप रूप में सिद्ध बनाने की प्रतिज्ञा नहीं की है। लेकिन हम सचेत पाप पर जयवंत होकर जी सकते हैं।
हमने देखा है कि यीशु हरेक बात में हमारे ही समान परखा गया था। हमारे सबसे शक्तिशाली प्रलोभन वे होते हैं जो हमारे वैचारिक-जीवन पर हमला करते हैं। यीशु के साथ भी ऐसा ही हुआ होगा। फिर भी, उसने पाप नहीं किया था। हम भी अपने वैचारिक-जीवन में जय पा सकते हैं।
यीशु की बोली शुद्ध थी। उसके मुख से न तो कोई गंदा शब्द, और न ही कोई निकम्मी बात निकली थी। उसने हमेशा सच बोला था। उसके मुख में कोई धोखा नहीं था। कोई भी व्यक्ति यीशु को ऐसी बातचीत में नहीं फँसा सका था कि ज़्यादा से ज़्यादा धन (अपनी ज़रूरतें पूरी करने से ज़्यादा) कैसे कमाया जाए। उसे ऐसे मामलों में कोई दिलचस्पी नहीं थी। उसका मन पृथ्वी की नहीं स्वर्गीय बातों में लगा हुआ था। निस्संदेह, उसने भौतिक वस्तुओं को इस्तेमाल किया था, लेकिन वह उनसे प्रेम नहीं करता था, और न ही उसका उनमें से किसी के साथ लगाव था।
यीशु की पवित्रता भीतरी थी। वह कोई ऐसी बाहरी पुण्यता नहीं थी जिसका प्रदर्शन खाने, पहनने, या मिलने-जुलने में था। वह कोई साधु या तपस्वी नहीं था। वह रोज़मर्रा की कामकाजी जि़न्दगी के बीच में रहता था, उसके सामाजिक स्तर के लोगों की तरह कपड़े पहनता था, और सामान्य रूप में खाता-पीता था (लूका 7:34), और उन सारी भली वस्तुओं का आनन्द के साथ उपयोग करता था जो परमेश्वर ने मनुष्य को इस जगत में आनन्द मनाने के लिए दी हैं (1 तीमु. 6:17)। फिर भी, वह खाने के मामले में कभी अपनी ख़ुदी-को-पोषित करने वाला नहीं बना था, क्योंकि इसमें उसने अपने आपको इतना अनुशासित करके रखा कि 40 दिन के उपवास के बाद भी उसने पत्थर को रोटी बनाने के लिए अपनी चमत्कारी शक्ति का उपयोग नहीं किया था। वह न सिर्फ धार्मिक लोगों से बल्कि सबसे बुरे पापियों के साथ भी मिलता-जुलता था और फिर भी निष्पाप बना रहता था। उसकी पवित्रता मूल रूप में भीतरी थी।
यीशु ने सिर्फ पाप का ही त्याग नहीं किया था, बल्कि उसने ऐसे अनेक वैध (न्यायोचित) सुख भी त्याग दिए थे जिनसे कोई लाभ न था, या जिनका आनन्द तब तक नहीं लिया जा सकता था जब तक कि पिता के उस काम के कुछ भाग का नुक़सान न होता जिसे वह पूरा करने के लिए आया था। (1 कुरि. 6:12)।
यीशु की पवित्रता परमेश्वर के वचन पर चिंतन-मनन करने वाले जीवन में से आई थी। 12 साल की उम्र तक उसे पवित्र शास्त्रों का गहरा ज्ञान प्राप्त हो चुका था, क्योंकि उसने पवित्र शास्त्रों पर मनन करने में बहुत मानसिक परिश्रम किया था और वचन में पवित्र आत्मा की ज्योति को खोजा था। वह धर्मज्ञान के विद्वान स्नातकों से ज़्यादा जानता था क्योंकि वह पवित्र आत्मा के प्रकाशन की खोज में रहता था। यीशु किसी बाइबल स्कूल में नहीं गया था। उसने अपने पिता के हाथ के नीचे रहते हुए सब सीखा था, वैसी ही जैसे पुरानी वाचा के समयकाल के सच्चे नबियों - मूसा, एलिय्याह, एलीशा, यिर्मयाह, यूहन्ना बपतिस्मा आदि ने सीखा था। बाइबल का कोई भी सच्चा नबी किसी बाइबल स्कूल में से नहीं आया था। हम यह याद रखें!
यीशु ने वचन का अध्ययन किया और फिर उसका पालन किया। इस तरह, वचन उसके हाथ में एक शक्तिशाली अस्त्र बन गया था, न सिर्फ शैतान के खिलाफ़ युद्ध करने के लिए (मत्ती 4:1-11), बल्कि उसकी प्रचारक की सेवा के लिए भी। वह अधिकार के साथ बोलता था, और उसका प्रचार उन लोकप्रिय परम्पराओं के विपरीत होता था जिनका प्रचार उसके समय के विद्वान और व्यवस्था के शास्त्री किया करते थे।
उसने फरीसियों के पाखण्ड और सांसारिकता का पर्दाफाश किया था, और उन्हें बता दिया था कि मूल रूप में उनके सारे धर्म-सिद्धान्तों में सही होने पर भी वे नर्क में जाने वाले थे (मत्ती 23:33)। और उसने सदूकियों की ग़लत व्याख्याओं और धर्म-सैद्धान्तिक भूलों को भी उजागर किया (मत्ती 22:23-33)।
यीशु ने अपनी शिक्षा में कभी लोकप्रिय होना नहीं चाहा था। सत्य में मामूली सा भी समझौता करने की बजाय वह यातना और पीड़ा सहने के लिए सहर्ष तैयार रहता था। वह "किसी भी क़ीमत पर शांति व एकता बनाए रखने" में विश्वास नहीं करता था। उसके शत्रु भी यह स्वीकार करते थे कि "हम जानते हैं कि तू पूरी तरह ईमानदार है, और परिणामों की चिंता न करते हुए, बिना डरे और बिना पक्षपात किए सच्चाई से सिखाता है" (मत्ती 22:16 - लिविंग)।
यीशु की पवित्रता परमेश्वर के घर की शुद्धता को बनाए रखने की धुन में भी देखी जा सकता थी (यूहन्ना 2:14)। जब उसने मन्दिर में जाते समय यह देखा कि लोग धर्म के नाम में धंधा कर रहे थे, तो उसमें धार्मिकता की आग की जलजलाहट भर गई और उसने एक चाबुक बना कर उन्हें वहाँ से बाहर खदेड़ दिया था।
बाइबल हमें यह आज्ञा देती है कि हम पाप किए बिना क्रोधित हो सकते हैं (इफि. 4:26)। जब रोमी सैनिक यीशु को पिलातुस के आंगन में मार रहे थे और कोड़े लगा रहे थे, तो उसने धीरज से वह सब सह लिया था। जब बात व्यक्तिगत होती थी तो वह कभी क्रोधित नहीं होता था। ऐसा क्रोध पाप होता। लेकिन जब मामला परमेश्वर के घर की शुद्धता का होता था, तब वह अलग बात होती थी। वहाँ क्रोधित न होना पाप होता!
उस दिन उसने चाबुक का इस्तेमाल किया था, और उसे इस बात की कोई चिंता नहीं थी कि लोग उसे ग़लत समझ लेंगे और यह सोच लेंगे कि उसका दिमाग़़ ख़राब हो गया है और वह शरीर के वश में हो गया है। वैसे भी, वह मनुष्यों के सम्मुख अपना जीवन व्यतीत नहीं करता था। वह तलवार चलाने आया था (मत्ती 10:34) और उसे चलाते हुए उसने कोई पक्षपात नहीं किया था। वह काटने, घायल करने, और चोट पहुँचाने वाली थी। और इस तरह पिता की महिमा प्रकट हुई थी।
यीशु का जीवन सबसे सुन्दर, सबसे सुचारु, सबसे शांतिपूर्ण और सबसे ख़ुश जीवन था, ऐसा जीवन जैसा संसार ने आज तक नहीं देखा है। इसकी वजह यह थी कि वह परमेश्वर के वचन का पूरा आज्ञापालन करता था।
भौतिक जगत में व्याप्त सुव्यवस्था को देखें। आकाश में तारे और नक्षत्र ऐसे सिद्ध रूप में अपनी कक्षाओं में परिक्रमाएं करते हैं कि हम उनके क्रमानुसार अपने समय के एक सैकण्ड के दस लाख अंश तक की सिद्धता प्राप्त कर सकते हैं। वे ऐसे भरोसेमंद हैं कि खगोल-शास्त्री भविष्य के किसी भी दिन में किसी भी तारे और नक्षत्र की अवस्था के बारे में अचूक रूप से बता सकते हैं। ऐसी सिद्ध व्यवस्था का रहस्य क्या है? इसका सिर्फ एक कारण हैः वे पूरी तरह से परमेश्वर की आज्ञा का पालन करते हैं, अपनी उन कक्षाओं में उसी गति के अनुसार भ्रमण करते हैं जो उनके सृष्टिकर्ता ने उनके लिए ठहराई है।
जहाँ भी आज्ञापालन होता है, वहाँ सिद्धता और सौन्दर्य होता है। और जहाँ आज्ञापालन नहीं होता, वहाँ अस्त-व्यस्तता और कुरुपता होती है।
आकाश के तारे भी हमारे सामने इस वास्तविकता की मूक साक्षी देते हैं कि परमेश्वर की आज्ञाएं हमारे लिए सबसे अच्छी होती हैं, और यह कि वे बोझिल नहीं हैं।
यीशु का जीवन इस वास्तविकता की साक्षी देता है कि सिर्फ ईश्वरीय भक्ति ही इस जगत में और आने वाले जगत में एक लाभदायक बात है (1 तीमु. 4:8)। एक ईश्वरीय भक्त से ज़्यादा ख़ुशी, शांति और संतोष दूसरे किसी व्यक्ति के पास नहीं होते। "परमेश्वर का भय जीवन का स्रोत् है" (नीति. 14:27); और यीशु ने "सदा परमेश्वर के भय में बने रहने" की आज्ञा का पालन किया था (नीति. 23:17)। परमेश्वर ने उसकी प्रार्थनाएं उसके ईश्वरीय भय के कारण सुनी थीं (इब्रा. 5:7)। यीशु के ऊपर स्वर्ग हमेशा खुला रहता था, क्योंकि वह परमेश्वर के भय में बना रहता था। उसने एक बार यह कहा था, "मैं अपने पिता के भय में रहता हूँ" (यूहन्ना 8:49 - ऐम्प्लिफाइड)। और उसने अपने जीवन के द्वारा इस वचन के सत्य को प्रदर्शित किया था, "परमेश्वर का भय बुद्धि का आरम्भ है" (नीति. 9:10)।
यीशु की प्रार्थनाएं स्वतः इसलिए नहीं सुनी जाती थीं क्योंकि वह परमेश्वर का पुत्र था, बल्कि इसलिए क्योंकि उसमें ईश्वरीय भय था (इब्रा. 5:7)। वह पवित्र आत्मा के आनन्द और अधिकार, "हर्ष के तेल" से अभिषिक्त रहता था, परमेश्वर का पुत्र होने के अधिकार की वजह से स्वतः नहीं, बल्कि इसलिए क्योंकि उसने धार्मिकता से प्रेम और पाप से घृणा की थी (इब्रा. 1:9)। परमेश्वर स्वयं को सिर्फ ऐसे व्यक्ति के प्रति ही वचनबद्ध कर सकता है जो नैतिक रूप में शुद्ध होता है। आत्मिक अधिकार होने का यही रहस्य है।
लेकिन, यीशु के समय का धार्मिक संसार, यीशु की पवित्रता के बारे में परमेश्वर के दृष्टिकोण से सहमत नहीं था। यीशु की पवित्रता ने उनकी घृणा को उत्तेजित किया था क्योंकि उसने निर्भय होकर उनके पाप की तरफ संकेत किया था। (यूहन्ना 7:7)। और इसलिए यीशु ने यहूदी धार्मिक अगुवों द्वारा द्वेष, तिरस्कार, घृणा, आलोचना, बहिष्कार और अंततः मृत्यु की पीड़ा को सहा - और यह सब इसलिए क्योंकि उसने पवित्रता का प्रचार किया था। अगर उसने सिर्फ एक पवित्र जीवन व्यतीत किया होता, तो उसे सूली पर भी न चढ़ाया जाता। लेकिन उसने अपने प्रचार द्वारा उनके पाखण्ड को धिक्कारा था और उनके पाप का पर्दाफाश किया था। इसलिए उन्होंने उसे मार डालने का दृढ़ निश्चय किया था।
यीशु ने कहा था, "उन्हें इस कारण दण्डित किया जाएगाः स्वर्ग से उतरी ज्योति जगत में आ चुकी है, लेकिन उन्होंने ज्योति की अपेक्षा अंधकार से ज़्यादा प्रेम किया, क्योंकि उनके काम बुरे थे। उन्होंने स्वर्गीय ज्योति से इसलिए घृणा की क्योंकि वे अंधेरे में पाप करना चाहते थे। वे उस ज्योति से दूर रहना चाहते थे क्योंकि उन्हें डर था कि उनके पाप प्रकट हो जाएंगे" (यूहन्ना 3:19,20 -लिविंग)।
आज का 'मसीही' जगत भी ऐसा ही है; और शिष्य अपने स्वामी से बड़ा नहीं होता। जब हम पवित्रता में चलेंगे, तो गुनगुना मसीही जगत हमारी प्रशंसा नहीं करेगा। "जो मसीह यीशु में भक्तिपूर्ण जीवन बिताना चाहते हैं, वे सताए जाएंगे" - हरेक देश में, और हरेक युग में (2 तीमु. 3:12) और यह सताव प्राथमिक रूप में धार्मिक संसार की तरफ से आएगा, जैसा स्वयं यीशु के मामले में हुआ था।
अगर कोई व्यक्ति यीशु के पीछे चलेगा, तो वह पहले बैठकर हिसाब लगा ले, और फिर "उसकी निंदा को अपने ऊपर उठाए हुए छावनी से बाहर निकल जाए" (इब्रा. 13:13)।
हमने यह देखा है कि परमेश्वर ज्योति और प्रेम दोनों है। परमेश्वर की महिमा प्रभु यीशु में देखी गई थी, जो ज्योति और प्रेम दोनों से भरपूर थी। ज्योति और प्रेम को एक-दूसरे से अलग नहीं किया जा सकता। सच्ची पवित्रता प्रेम से भरपूर होती है और सच्चा प्रेम पूरी तरह शुद्ध होता है। यहाँ उन्हें सिर्फ हमारे समझने के लिए अलग करके देखा जा रहा है।
अगर कोई पवित्रता का दावा करता है लेकिन ईश्वरीय प्रेम का प्रदर्शन नहीं करता, तो वह असली पवित्रता नहीं बल्कि "फरीसी धार्मिकता" है। दूसरी तरफ, वे जो सभी के लिए बड़े प्रेम से भरे होने का दावा करते हैं लेकिन शुद्धता और धार्मिकता में नहीं जीते, तो वे भ्रम में पड़कर अपनी कोमल भावनाओं को ईश्वरीय प्रेम समझ लेते हैं।
फरीसियों की ऐसी "धार्मिकता" थी जो कर्कश और सूखी थी। वे हड्डियों के कंकाल की तरह थे - कठोर और विभत्स। उनमें कुछ सत्य था, लेकिन वह बिगड़ा और बिखरा हुआ था।
यीशु में सारा सत्य था। फरीसियों से बढ़कर, वह परमेश्वर की व्यवस्था की छोटी से छोटी बात का पक्षधर था। वह सिर्फ हड्डियाँ नहीं था। हड्डियों पर माँस चढ़ा हुआ था - जैसा मनुष्यों के लिए परमेश्वर ने चाहा था - ज्योति ने प्रेम का ओढ़ना ओढ़ रखा था। उसने सत्य बोला था, लेकिन उसने प्रेम से सत्य बोला था (इफि- 4:15)। उसके शब्दों में अधिकार होता था, लेकिन उनमें कृपा भी होती थी (लूका 4:22,36)।
यह वह स्वभाव है जो पवित्र आत्मा हमें देना और हमारे द्वारा प्रदर्शित करना चाहता है।
परमेश्वर प्रेम है। ऐसा नहीं है कि वह सिर्फ प्रेमपूर्वक व्यवहार करता है। वह, उसके मूल तत्व में, प्रेम है। यीशु में देखी गई परमेश्वर की महिमा, स्पष्ट रूप में यह प्रदर्शित करती है। यीशु ने सिर्फ प्रेम के काम ही नहीं किए। वह फ्भलाई करता हुआय् घूमता फिरा था (प्रेरितों. 10:38)। लेकिन यह इसलिए था क्योंकि परमेश्वर का प्रेम उसके पूरे अस्तित्व में होकर बहता रहता था।
प्रेम का मूल भी, हमारी पवित्रता और नम्रता की तरह, हमारे नए मनुष्य में है। आत्मा से भरे हुए एक मनुष्य के भीतर से जीवन की नदियाँ बहती हैं (यूहन्ना 7:38,39)।
हमारे विचार और मनोभाव (चाहे उन्हें व्यक्त भी न किया जाए), हमारे शब्दों, हमारे कामों, और हमारे व्यक्तित्व को भी एक गंध प्रदान करते हैं। और दूसरे लोग आसानी से इस गंध को पहचान सकते हैं। अगर दूसरों के प्रति हमारे विचार और मनोभाव स्वार्थ और आलोचना से भरे रहते हैं, तो हमारे शब्दों और हमारे प्रेम के कामों का कोई मूल्य नहीं होता। परमेश्वर हमारे "मन की गहराई में सच्चाई चाहता है" (भजन. 51:6)।
यीशु ने हरेक मनुष्य को बहुत मूल्यवान माना था, इसलिए वह सब मनुष्यों का आदर करता था। ईश्वरीय, सभ्य, और बुद्धिमान लोगों का आदर करना आसान है। जब हम मसीह में अपने साथी-विश्वासियों से प्रेम करते हैं, तब हम यह भी सोच सकते हैं कि हम बहुत ऊँचाइयों पर पहुँच गए हैं। लेकिन परमेश्वर की महिमा उस प्रेम में देखी गई जो यीशु में सब मनुष्यों के लिए था। यीशु ने किसी को कभी उसकी ग़रीबी, अज्ञानता, बदसूरती या असभ्यता की वजह से तुच्छ नहीं जाना। उसने ख़ास तौर पर यह कहा कि सारा जगत और जो कुछ इसमें है, उसका मूल्य उतना नहीं है जितना एक मानवीय जीव का है (मरकुस 8:36)। उसने इस तरह मनुष्य का मूल्य को आँका था। और इसलिए वह सब मनुष्यों में हर्षित होता था। वह मनुष्यों को शैतान द्वारा भरमाए और जकड़े हुए देखता था, और वह उन्हें मुक्त करने की बड़ी अभिलाषा करता था।
प्रेम में से जन्म लेने वाली यह अभिलाषा इतनी महान् थी कि मनुष्यों के जीवनों पर से पाप के शिकंजे को तोड़ने के लिए वह सबसे बड़ी क़ीमत चुकाने के लिए भी तैयार था। और क्योंकि मनुष्यों को उनके पापों से बचाने के लिए वह मरने के लिए तैयार था, इसलिए उसने यह अधिकार अर्जित किया था कि वह पाप के खिलाफ़ ज़ोरदार प्रचार कर सके। अगर हमने एक पाप का अपने शरीर में न्याय नहीं किया है और उस पर जय नहीं पाई है, या, जिस पाप के खिलाफ़ हम प्रचार करते हैं उससे लोगों को बचाने के लिए (ज़रूरत पड़ने पर) हम मरने को तैयार न हों, तो हमें उस पाप के खिलाफ़ प्रचार करने का कोई अधिकार नहीं है। "प्रेम में एक-दूसरे से सच बोलने" का यही अर्थ है (इफि. 4:15)।
हमारे द्वारा बोले गए शब्दों में प्रेम की ऊष्मा ही है जो दूसरों में परमेश्वर की महिमा के लिए फल पैदा करती है। हालांकि उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव में भरपूर प्रकाश होता है, फिर भी ऊष्मा (गर्माहट) न होने की वजह से वहाँ कुछ नहीं उगता।
यीशु ने लोगों और भौतिक वस्तुओं के परस्पर मूल्य को स्पष्ट रूप में देख लिया था। वह जानता था कि लोग प्रेम करने के लिए बने हैं और वस्तुएं इस्तेमाल करने के लिए बनी हैं। लेकिन जगत में पाप के विकृत प्रभाव की वजह से यह क्रम उलटा हो गया है, और अब वस्तुओं से प्रेम किया जा रहा है और लोगों को (स्वार्थी उद्देश्यों को पूरा करने के लिए) इस्तेमाल किया जा रहा है।
यीशु ने यह देखा था कि लोग वस्तुओं से ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं। उसने मनुष्यों से ऐसा प्रेम किया कि वह उनके साथ पूरी तरह एक हो गया और उसने उन्हें ऐसा महसूस कराया कि वे चाहने योग्य हैं। उसने उनके साथ उनका बोझ उठाया, और दबे-कुचलों के लिए उसके पास दया के शब्द थे, और जीवन के संघर्षों में हारे हुए लोगों के लिए उसके पास उत्साहित करने वाले शब्द थे। उसने कभी किसी मनुष्यों के बारे में ऐसा नहीं सोचा कि वह किसी काम का नहीं है। वे असभ्य या गंवार हो सकते थे, लेकिन फिर भी वे ऐसे लोग थे जिन्हें छुड़ाए जाने की ज़रूरत थी।
दूसरी तरफ वस्तुएं थीं जिनसे उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता था। भौतिक वस्तुओं का इसके अलावा कोई मूल्य नहीं होता कि उनका उपयोग दूसरों को लाभ पहुँचाने के लिए किया जाए। हम कल्पना कर सकते हैं कि अगर यीशु की कार्यशाला में किसी बच्चे ने आकर कोई महँगा औज़ार तोड़ दिया हो, तो उससे यीशु को कोई परेशानी नहीं होती क्योंकि उसके लिए बच्चा उस टूटी हुई वस्तु से बहुत ज़्यादा मूल्यवान और महत्वपूर्ण था। वह वस्तुओं से नहीं मनुष्यों से प्रेम करता था। वस्तुओं का उपयोग लोगों की मदद के लिए होता था।
पवित्र आत्मा हमारे मनों को इसलिए नया करता है कि हम "वस्तुओं को परमेश्वर के दृष्टिकोण से देखने वाले बन जाएं" (कुलु. 1:9 - फिलिप्स)। एक व्यक्ति से प्रेम करना उसे परमेश्वर के नज़रिए से देखना है - संवेदना के साथ।
परमेश्वर अपने लोगों में गीतों के साथ आनन्द मनाता है (सप. 3:17)। और यीशु क्योंकि परमेश्वर के आत्मा से परिपूर्ण था, इसलिए वह भी अपने पिता के साथ उसके बच्चों के आनन्द में आनन्दित रहता था। जिन लोगों के मन नए होकर लोगों को परमेश्वर के नज़रिए से देखने वाले बन जाएंगे, उनके साथ भी ऐसा ही होगा। दूसरे लोगों के बारे में यीशु के विचार हमेशा प्रेम के विचार होते थे - उनकी अशिष्टता या अभद्रता के बारे में उसके विचार कभी आलोचना-भरे नहीं होते थे। इस वजह से ही लोग उसकी आत्मा की मधुर सुगंध को महसूस कर लेते थे, और "सामान्य लोग आनन्द से उसकी बात सुनते थे" (मरकुस 12:37 - के.जे.वी.)। जब हम पवित्र आत्मा से भरे जाते हैं, तब परमेश्वर इसी प्रेम को हमारे हृदयों में उण्डेलता है (रोमि. 5:5)।
यीशु के अन्दर लगातार बीमार, ज़रूरतमंद, भूखे और एक चरवाहा न होने से भटक रहे लोगों के लिए संवेदना उमड़ती रहती थी। वह उनकी पीड़ा को अपनी पीड़ा बना लेता था, और इस वजह से ही वह उन्हें सान्त्वना दे सकता था। हम दूसरे की पीड़ा में उन्हें उसी अनुपात में सान्त्वना दे सकते हैं, जिस अनुपात में हम उसी पीड़ा में उनके साथ एक हुए हैं। यीशु लोगों की अनकही ज़रूरतों के प्रति संवेदनशील रहता था क्योंकि अपनी कल्पना का इस्तेमाल करते हुए वह अपने आपको उनकी परिस्थितियों में रख कर देखता था, और इस तरह वह उनकी समस्याओं को समझ लेता था। एक बार जब उसने यह देखा कि एक ज़रूरतमंद व्यक्ति के लिए लोगों में कोई संवेदना नहीं थी, तो वह लोगों के हृदय की कठोरता के कारण बहुत दुःखी हुआ था (मत्ती 3:5)।
मनुष्यों के साथ अपने सम्बंध में, यीशु अपनी ख़ुदी में लगातार मरता रहता था। उसे किसी ने जो भी कहा या उसके साथ जो भी किया, उसका वह कभी बुरा नहीं मानता था। और न ही उसे तब बुरा लगता था जब दूसरे उसके लिए कुछ करने में नाकाम हो जाते थे, क्योंकि वह दूसरों से कोई अपेक्षा नहीं रखता था। वह सेवा करवाने नहीं सेवा करने आया था।
यीशु क्योंकि अपनी सूली को प्रतिदिन उठाता था, इसलिए कोई चाहे कितना भी असभ्य या मूर्ख क्यों न हो, वह उससे झुंझलाता नहीं था। दूसरों का धीमापन उसे बेचैन नहीं करता था, और न ही दूसरों का मैला-कुचैलापन, अस्त-व्यवस्तता, या लापरवाही उसे कभी अधीर करती थी। सिद्ध व्यक्ति आसानी से लोगों की कमी-घटी सह सकता है। सिर्फ त्रुटिपूर्ण मनुष्य ही दूसरों की त्रुटियों को नहीं सह पाते! दूसरों के लिए अपने प्रेम को हम धीरज द्वारा स्पष्ट रूप में प्रकट कर सकते हैं।
यीशु के प्रेम की महिमा को उसकी बोली में देखें।
यीशु ने अपनी बोली द्वारा कभी किसी को नीचा नहीं दिखाया, न ही ऐसी टीका-टिप्पणियाँ या हँसी-मज़ाक किए जिससे उन्हें चोट लगती। उसने छुपे तौर पर चोट पहुँचाने वाली कोई बात कभी नहीं कही। उसने अपने शिष्यों की पीठ-पीछे कभी उनकी कमियों के बारे में बातचीत नहीं की। यह वास्तव में एक अद्भुत बात है कि तीन साल के समयकाल में भी, उसने अपने बाक़ी शिष्यों के सामने यहूदा का पर्दाफाश नहीं किया था - क्योंकि, अंतिम भोज के समय भी, उन ग्यारहों को यह नहीं मालूम था कि उनके स्वामी के साथ कौन विश्वासघात करने वाला था।
यीशु ने अपनी जीभ को दूसरों को उत्साहित करने और ताड़ना देने के लिए इस्तेमाल किया था, और इस तरह उसने अपनी जीभ को परमेश्वर के हाथ में जीवन के संसाधन के रूप में सौंप रखा था। उसने अपनी जीभ को थके-मांदों से संभालने के लिए इस्तेमाल किया था (यशा. 50:4), और घमण्डी और अहंकारी लोगों को काटने-छाँटने के लिए एक तलवार की तरह भी इस्तेमाल किया था (यशा. 49:2)।
जब रोमी सूबेदार और सुरूफिनीकी स्त्री ने उनके विश्वास के लिए यीशु को सबके सामने उनकी प्रशंसा करते सुना था, तब वे कितने उत्साहित हुए होंगे (मत्ती 8:10; 15:28)। वह पापी स्त्री जिसके प्रेम के लिए (लूका 7:47) और बैतनिय्याह की मरियम जिसकी बलिदानी भेंट के लिए उनकी प्रशंसा की गई (मरकुस 14:6), कभी यीशु के शब्दों को न भूली होंगी।
परतस को यीशु के इन शब्दों से कितना बल मिला होगा कि वह उसके लिए प्रार्थना करेगा (लूका 22:32)। सिर्फ कुछ शब्द ही थे, लेकिन उनसे लोगों को कितना बल और उत्साह मिला था।
ऐसे और भी बहुत से लोग होंगे जिन्होंने यीशु के मुख से उनकी थकी-मांदी आत्माओं को ऊँचा उठाने वाले शब्द सुने होंगे, क्योंकि यशायाह 50:4 में लिखा है कि यीशु प्रतिदिन अपने पिता की आवाज़ सुनता था कि प्रतिदिन उसके मार्ग में आने वाले थके-मांदे लोगों के लिए उसके पास एक उचित शब्द हो।
यीशु की धार्मिकता उसके मुख को उदास बना देने वाली नहीं थी। न ही उसका हर्ष के तेल से अभिषेक हुआ था (इब्रा. 1:9)। सूली पर चढ़ने की पिछली शाम उसमें ऐसा उमड़ने-छलकने वाला आनन्द था कि वह अपने शिष्यों से यह कह सका था, "मेरा आनन्द तुम में बना रहे" (यूहन्ना 15:11)। वह सब जगह नीरस और उदास लोगों में उस आनन्द को बाँटता हुआ घूमा था।
वह सब मनुष्यों के प्रति कोमल था, और कभी भी किसी झुके हुए सरकण्डे को नहीं तोड़ा और न ही किसी टिमटिमाते हुए दिये को बुझाया (मत्ती 12:20)। उसने कमज़ोर और पापी लोगों में अच्छी बातें देखनी चाहीं और सबके लिए सर्वश्रेष्ठ चाहा। वह एक ऐसा व्यक्ति था जिसके साथ लोग समय बिताना चाहते थे क्योंकि वह समझदार, दयालु और नम्र था। सिर्फ ऐसे लोग ही उससे दूर रहते थे जो घमण्डी थे और जिनमें छुपे हुए पाप थे।
यीशु का प्रेम भावुक नहीं था। वह सबके लिए सबसे अच्छा चाहता था। और इस वजह से ही, उसे जहाँ भी ऐसी ज़रूरत नज़र आती थी, वह ताड़ना के शब्दों का इस्तेमाल करने से भी नहीं झिझकता था। उसने पतरस को डाँटा था क्योंकि वह उसे सूली की तरफ जाने से रोक रहा था - और वह भी ऐसे कठोर शब्दों द्वारा किया था, "दूर हट, शैतान" (मत्ती 16:23)।
उसने याकूब और यूहन्ना को डाँटा था क्योंकि उन्होंने अपने लिए सम्मानित पद चाहे थे और वे सामरियों से बदला लेना चाहते थे (मत्ती 20:33; लूका 9:55)। और उसने सात बार अपने शिष्यों को उनके अविश्वास के लिए डाँटा था।
चाहे दूसरों को उससे चोट लगे, फिर भी यीशु सच बोलने से कभी नहीं डरा, क्योंकि उसका हृदय उनके लिए प्रेम से भरा था। उसे इस बात की परवाह नहीं थी कि ऐसे कठोर शब्द बोलने से उसकी एक सौम्य व्यक्ति होने की नेकनामी ख़त्म हो जाएगी। वह अपने से ज़्यादा दूसरों से प्रेम करता था, इसलिए उनकी मदद करने के लिए अपनी नेकनामी की भेंट चढ़ाने के लिए तैयार था। इस वजह से उसने दृढ़ता के साथ सच बोला, कि ऐसा न हो मनुष्य का अनन्त नाश हो जाए। उसके लिए मनुष्यों की अनन्त भलाई उसके स्वयं के बारे में दूसरों के मत से ज़्यादा महत्वपूर्ण थी।
पतरस ने यीशु की सेवकाई का बयान इन शब्दों में किया, "वह भलाई करता हुआ घूमता फिरता था" (प्रेरितों. 10:38)। वास्तव में, यही उसके जीवन का सार था। वह सिर्फ एक अच्छा प्रचारक ही नहीं था, और न ही उसकी दिलचस्पी सिर्फ आत्माओं को जीतने में थी। वह सम्पूर्ण मनुष्य से प्रेम करता था, और वह जहाँ भी गया, वहाँ उसने मनुष्यों की देह और आत्माओं दोनों का भला किया।
उसके शत्रु, ताने मारते हुए, उसे "चुंगी लेने वालों और पापियों का मित्र" कहते थे (लूका 7:34), और वास्तव में वह वही था, समाज में सबसे तुच्छ माने जाने वाले लोगों का मित्र।
मनुष्य के लिए यह एक सामान्य बात नहीं होती कि वह समाज के बहिष्कृत लोगों का भला करता घूमे और उनका मित्र बने। और जहाँ ऐसा किया जाता है, वह स्वार्थी उद्देश्यों से किया जाता है। लेकिन ऐसे लोगों के लिए, जो समाज से बहिष्कृत थे और जिनका कोई मित्र नहीं था, यीशु का प्रेम निःस्वार्थ और शुद्ध था।
हम सभ्य व सुसंस्कृत होने द्वारा मसीह का स्वभाव प्रदर्शित नहीं कर सकते, बल्कि जो स्वाभाविक है उसके प्रति मरने, और जो ईश्वरीय है उसे पवित्र आत्मा से ग्रहण करने द्वारा ही हम यह कर सकते हैं।
यीशु के प्रेम ने उसे इस योग्य बनाया कि वह उसके शिष्यों की सहर्ष सेवा कर सका, और उनके लिए गंदे काम भी कर सका - जैसे उनके पैर धोना। यह इसलिए नहीं किया गया था कि वे उसकी नम्रता से प्रभावित हो जाएं, बल्कि यह उनके लिए उसके प्रेम का स्वाभाविक बाहरी प्रवाह था।
मानवीय भलाई और प्रेम का ज़रूर कुछ-न-कुछ बुरा उद्देश्य होता है, जैसे अपने लिए सम्मान चाहना या कोई दूसरा स्वार्थ। वह उसके मूल-स्रोत् में ही भ्रष्ट होता है। सिर्फ ईश्वरीय प्रेम ही भ्रष्टता से मुक्त होता है। यीशु ने जो भलाई की, उसमें उसके व्यक्तिगत लाभ का कोई विचार नहीं था। उसकी अच्छाई उसके पिता के स्वभाव का प्रकटीकरण था जो "भले और बुरे दोनों को अपने सूर्य का प्रकाश देता है, और न्यायी और अन्यायी दोनों पर अपनी वर्षा भेजता है" (मत्ती 5:45 - लिविंग)।
परमेश्वर का स्वभाव भला करने और देने, और ज़्यादा देने, और देते ही रहने का है। यह उसके लिए ऐसा ही स्वाभाविक है जैसे सूर्य के लिए चमकते रहना स्वाभाविक है। यही वह महिमा है जो यीशु के जीवन में से प्रकट हुई थी। वह लगातार भलाई करता रहा, दूसरों की सेवा करता रहा, और जिसको जो दे सकता था उसे वह देता रहा।
यूहन्ना 13:29 के शब्द उस बात की तरफ इशारा करते हैं जो यीशु की पूरी सार्वजनिक सेवा में उसके शिष्यों ने उसके द्वारा धन का उपयोग करने के बारे में देखी थी। उन्होंने यह महसूस कर लिया था कि यीशु सिर्फ दो कामों के लिए धन का उपयोग करता थाः जो ज़रूरी होता था वह ख़रीदने के लिए, और ग़रीबों को देने के लिए।
यीशु ने अपने शिष्यों को यह सिखाया था कि "लेने से देना अच्छा होता है" (प्रेरितों. 20:35), और उसने अपने जीवन के द्वारा यह दर्शाया था कि इस पृथ्वी पर एक मनुष्य तब सबसे ज़्यादा प्रसन्न और आशिषित जीवन व्यतीत कर सकता है जब वह पूरी तरह परमेश्वर और दूसरों के लिए जीता है, जिसमें वह अपने आपको और अपनी वस्तुओं को दूसरों को आशिष देने के लिए इस्तेमाल करता है।
यीशु जिनके बीच में प्रचार करता था, वह उनके लिए रोता और प्रार्थना करता था। जब यरूशलेम ने परमेश्वर के वचन को ग्रहण नहीं किया, तब वह उसे देखकर रोया था। इससे पहले कि उसने एक चाबुक बना कर सब पाखण्डी लोगों को मन्दिर में से बाहर निकाला, वह उनके लिए रोया था (लूका 19:41,45)। जो रोता है, सिर्फ वही चाबुक मार सकता है।
ऐसा कोई मनुष्य नहीं है जिसके पास पृथ्वी पर पूरा करने के लिए यीशु से ज़्यादा महत्वपूर्ण काम है। किसी मनुष्य ने 3 साल की सार्वजनिक सेवा में ऐसा उपयोगी परिश्रम नहीं किया है। वास्तव में, वह दिन-रात व्यस्त रहा होगा। फिर भी, सबसे अद्भुत बात यह है कि उसने ऐसा कोई सचिव नियुक्त नहीं किया था जो उससे मिलने के लिए आने वाले लोगों को नियमबद्ध कर उन्हें नियंत्रित करे! जब उसके शिष्यों ने उसका सचिव बनने की कोशिश की, तो उसने उन्हें डाँटा (मरकुस 10:13-15)।
हालांकि उसकी चिन्ह्-चमत्कार की एक ऐसी सेवा थी जैसी किसी मनुष्य की कभी नहीं रही थी (और सिर्फ इसी सेवकाई की वजह से बहुत लोग उससे समय चाहते होंगे), फिर भी उसने हर समय अपने आपको सबके लिए उपलब्ध रखा था।
उसके सम्बंधी यह सोचने लगे थे कि उसका दिमाग़ ख़राब हो गया है, क्योंकि उनके विचारानुसार वह ज़रूरतमंद लोगों की सेवा करने में ऐसा व्यस्त हो गया था कि उसे अपने खाने-पीने का भी होश नहीं रहा था (मरकुस 3:20,21)।
लोग यह जानते थे कि उसके पास कोई भी कभी भी आ सकता है। हालांकि यीशु सारा दिन प्रचार करने में व्यस्त रहा था, फिर भी नीकुदेमुस को रात के समय में उसके पास आने में कोई झिझक महसूस नहीं हुई थी। नीकुदेमुस भली-भांति जानता था कि उसका स्वागत किया जाएगा। यीशु के लिए लोगों में यही मनोभाव रहता था - कि वे दिन में या रात में, आज़ादी के साथ कभी भी उसके पास मदद के लिए आ सकते थे।
एक बार सूर्यास्त के बाद उसके पास बीमार लोगों को लाया गया था - और उनकी संख्या बहुत थी - और यीशु ने उन सब पर हाथ रख कर उन्हें चंगा किया था (लूका 4:40)। इसमें उसे कई घण्टे का समय लगा होगा। लेकिन उसने एक सामूहिक प्रार्थना करने द्वारा उस प्रक्रिया में लगने वाले समय को कम करने की कोशिश नहीं की थी। उसे उनमें से हरेक व्यक्ति में दिलचस्पी थी, और वह उन पर व्यक्तिगत रूप से ध्यान देना चाहता था। और उसे इस बात की कोई परवाह नहीं थी कि इसमें उसके खाने और सोने के समय की हानि हो रही थी।
यीशु अपने समय को अपना नहीं समझता था। उसने अपने आपको पूरी तरह से लोगों को दे रखा था। ज़रूरतमंद लोग स्वयं उसे, उसके समय को, उसकी वस्तुओं को, और उसका जो कुछ था वह इस्तेमाल कर सकते थे (यशा. 58:10)। वह तकलीफ उठाने के लिए तैयार रहता था, और जब लोग उसे तकलीफ देते और उसके निजी जीवन में घुसपैठ करते थे, तो वह बुरा नहीं मानता था।
उसके द्वारा प्रकट होने वाले पवित्र आत्मा के शक्तिशाली अलौकिक दान-वरदानों से लोग आशिष पाते थे क्योंकि उसके अन्दर से काम करने वाली परमेश्वर की सामर्थ्य परमेश्वर के प्रेम और संवेदना में आवृत थी। प्रेम और संवेदना के बिना किए गए चमत्कार एक बिजली के नंगे तार की तरह, जिस पर कोई आवरण नहीं है, आत्मिक मृत्यु का कारण बन सकते हैं।
यीशु का प्रेम और उसकी दिलचस्पी देह की रीति के अनुसार उसके सम्बंधियों के लिए भी थी। "परमेश्वर के काम" के बारे में उसकी सोच फरीसियों जैसी विकृति नहीं थी, जो प्रभु की "पूर्ण-कालिक सेवा" में निकले लोगों को माता-पिता के ज़रूरतों को अनदेखा करना सिखाते थे, क्योंकि उन्हें "माता -पिता से ज़्यादा परमेश्वर को प्रेम करना था" (मरकुस 7:10-13)। सूली पर मरते समय भी, यीशु को यह ख़्याल था कि वह अपनी माता के भविष्य का इंतज़ाम करे (यूहन्ना 19:25-27)।
यीशु ऐसी परिपूर्णता के साथ परमेश्वर और लोगों के लिए जीता था, कि मरते समय भी, उसने एक डाकू की अगुवाई करते हुए उसे उद्धार के मार्ग में पहुँचाया। सूली पर लटके हुए, उसने न तो अपनी पीड़ा की और न दूसरों के ठट्ठों और घृणा की परवाह की, बल्कि उसकी दिलचस्पी उसे सूली पर चढ़ाने वालों में और उनके पाप क्षमा होने में थी (लूका 23:34)।
यीशु ने हमेशा बुराई को भलाई से जीता था। दूसरे लोगों की घृणा की बाढ़ उसके प्रेम की धधकती आग को नहीं बुझा सकी थी (श्रेष्ठ. 8:7)। यही वह प्रेम है जो वह उसके आत्मा द्वारा हमें देता है जिससे हम एक-दूसरे से वैसा प्रेम कर सकते हैं जैसा उसने हमसे किया है (यूहन्ना 13:34,35; रोमि. 5:5)। हम भी इसी तरह ईश्वरीय स्वभाव को अभिव्यक्त कर सकेंगे।
पिछले तीन अध्यायों में, हमने यह देखा कि यीशु पृथ्वी पर कैसे रहा - नम्रता, पवित्रता और प्रेम में।
अब ख़तरा यह है कि हम यह सोच सकते हैं कि इन तीनों क्षेत्रों में हम यीशु की नकल करते हुए उसके जैसे बन सकते हैं। हममें से परमेश्वर की महिमा यीशु की नकल करने द्वारा प्रकट नहीं होती, बल्कि ईश्वरीय स्वभाव में सहभागिता करने द्वारा होती है।
जगत के इतिहास में ऐसे बहुत से ग़ैर-मसीही हुए हैं जो यीशु के बड़े प्रशंसक थे, और उन्होंने उसकी नम्रता, शुद्धता और प्रेम की नकल करनी चाही, और यह उन्होंने काफी अच्छी तरह भी किया। लेकिन यह आग के ऐसे चित्र की तरह है जिसमें से कोई गर्माहट नहीं मिलती।
नकली हीरे इतने असली लग सकते हैं कि एक जौहरी ही उन्हें परखने के बाद उनके बीच फ़र्क कर सकता है। लेकिन वे सिर्फ काँच के टुकड़े होते हैं, और असली हीरे की तुलना में उनका कोई मूल्य नहीं होता। और मनुष्य नकल करने में बहुत दक्ष है - यीशु की नकल करने के परिमण्डल में भी।
तब हम धोखे से कैसे बच सकते हैं? हम यह कैसे जान सकते हैं कि हम सिर्फ यीशु की नक़ल कर रहे हैं या हम असल में उसके ईश्वरीय स्वभाव में सहभागी हो रहे हैं?
इसका सिर्फ एक ही तरीक़ा है, और वह यह है कि हम पवित्र आत्मा को यह अनुमति दें कि हमारे जीवनों में से वह आत्मिक को जैविक से अलग कर दे (इब्रा. 4:17)। अगर हम जैविक और आत्मिक के बीच के फ़र्क को नहीं जानेंगे, तो हम पूरी तरह से धोखा खा जाएंगे, और हमें पता भी नहीं चलेगा कि हम धोखे में पड़ गए हैं।
हमारे समय में विश्वासियों को जो बात सबसे ज़्यादा समझने की ज़रूरत है, वह यह है कि उनके मनों, भावनाओं और इच्छाओं की शक्ति कैसे पवित्र आत्मा के काम में बाधा बनती है। जब हम जैविक और आत्मिक कामों के बीच का फ़र्क नहीं जानते, तब इसमें सिर्फ यही सम्भावना नहीं होती कि हम अपने हृदयों द्वारा धोखा खाते हैं, बल्कि दुष्टात्माएं भी आकर हमें भरमाती हैं क्योंकि वे परमेश्वर के काम की नकल करती हैं।
ज़्यादातर विश्वासी जैविक और आत्मिक काम के बीच के फ़र्क के बारे में पूरी तरह अनजान होते हैं, क्योंकि उन्होंने अपने आत्मिक जीवनों को उस बिन्दु तक उन्नत नहीं किया है जहाँ से आगे बढ़ना फिर जैविक और आत्मिक के बीच का फ़र्क जानने पर निर्भर हो जाता है।
एक नौवीं कक्षा के छात्र को अवकलन गणित (डिफरैन्यश्ल कैलक्यूलस) और समाकलन गणित (इन्टिग्रल कैल्क्यूलस) के बीच का फर्क़ मालूम नहीं होता (और शायद वह उन दोनों को एक ही समझ समझेगा), क्योंकि अपने गणित शास्त्र के अध्ययन में वह उस बिन्दु तक नहीं पहुँचा है जहाँ से उसकी आगे की प्रगति, आंकलन के इन दोनों स्वरूपों के बीच का फ़र्क जानने पर निर्भर होगी।
अगर आप इस बात से संतुष्ट हो जाते हैं कि मनुष्य आपको एक खरा, दयालु, सौम्य और संवेदनशील व्यक्ति मानते हैं, तो आप एक "जैविक मसीही" होने से आगे नहीं बढ़ पाएंगे, यीशु की सिर्फ एक नकल होने से ज़्यादा कुछ न होंगे।
पौलुस ने मसीहियों को तीन श्रेणियों में बाँटा हैः
(1) आत्मिक मनुष्य (1 कुरि. 3:1)_
(2) जैविक मनुष्य (1 कुरि. 2:14 - शाब्दिक अनुवाद); और
(3) शारीरिक मनुष्य
यह मनुष्य के उस तीन स्तरीय विभाजन के अनुरूप है जिसका उल्लेख पहला थिस्सलुनीकियों 5:23 में किया गया है - आत्मा, जीव, देह।
जब शरीर की अभिलाषाएं हम पर राज करती हैं, तब हम शारीरिक होते हैं। और, यह हो सकता है कि हम शरीर की अभिलाषाओं पर जय पाने के बाद भी सिर्फ जैविक ही बने रहें - जिसमें मन और भावना की अभिलाषाएं हम पर राज कर रही हों। आत्मिक मनुष्य वह है जिस पर आत्मा का राज होता है, और जिसका जीव और देह पवित्र-आत्मा के नियंत्रण में रहते हैं।
हालांकि यह ज़रूरी नहीं है कि एक शारीरिक मनुष्य की तरह एक जैविक मनुष्य "परमेश्वर से शत्रुता" करने वाला होगा (रोमि. 8:7), फिर भी, उसमें आत्मिक बातों की समझ नहीं होगी (1 कुरि. 2:14), क्योंकि वे उसके लिए मूर्खतापूर्ण होंगी। अगर उसके सामने जैविक और आत्मिक के बीच का फ़र्क दर्शाया भी जाएगा, तब भी वह उसे मूर्खता से भरा और बाल की खाल उतारने जैसा ग़ैर-ज़रूरी काम लगेगा, क्योंकि वह जैविक है, और जैविक रहने से ही संतुष्ट है क्योंकि उसकी मनुष्यों के सामने एक अच्छी साक्षी है। वह जो मनुष्यों का आदर-सम्मान चाहता है, कभी भी जैविक दशा से आगे नहीं बढ़ पाएगा।
मसीही कलीसिया में व्यापक रूप से फैले धोखे के इन दिनों में, जिसमें ऐसी बहुत सी आवाज़ें और चिन्ह् प्रकट हो रहे हैं और जो सभी परमेश्वर की तरफ से होने का दावा कर रहे हैं, इसलिए आज यह पहले से ज़्यादा ज़रूरी हो गया है कि अगर हमें शत्रु की युक्तियों से बचे रहना है, तो हमें जैविक और आत्मिक के बीच के फ़र्क को जानना होगा।
"पहला मनुष्य आदम एक जीवित प्राणी बना, लेकिन दूसरा आदम एक जीवन-दायक आत्मा बना" (1 कुरि. 15:45)।
हमें, जो पहले आदम की शीर्षस्थता से छुड़ा लिए गए हैं और मसीह (दूसरे आदम) के शीर्षस्थ हो गए हैं, यह समझने की ज़रूरत है कि जीव में से जीना छोड़ कर आत्मा में जीना क्या होता है।
सिर्फ यही काफी नहीं है कि हमारी देह का शारीरिक तत्व निष्क्रिय कर दिया जाए। हमारा जैविक तत्व, जो देखने में इतना बुरा नहीं होता, हमारी आत्मिक उन्नति के लिए उतना ही ख़तरनाक है, और उसके साथ भी वैसा ही व्यवहार करना ज़रूरी है। हमें प्रतिदिन ज़्यादा से ज़्यादा न सिर्फ पाप की शक्ति से बल्कि हमारे जीव की निरन्तर होने वाली गतिविधि से भी बचने की ज़रूरत है।
जैविक लोग यह कभी नहीं समझ पाएंगे कि यीशु ने कुछ ख़ास मौक़ों पर वैसी बातें क्यों की थीं। एक बार जब वह अपने शिष्यों के बीच में था, और उसे यह बताया गया कि उसके सम्बंधी उससे मिलना चाह रहे हैं, तो उसने अपने शिष्यों की तरफ इशारा करते हुए कहा कि वे उसके सबसे नज़दीकी सम्बंधी थे (मत्ती 12:49,50)।
उसके सम्बंधियों और दूसरे लोगों ने उसके कथन को कठोर और असंवेदना से भरा कथन समझा होगा। लेकिन यीशु यह नहीं चाहता था कि उसके सम्बंधियों के साथ उसका कोई जैविक लगाव हो।
उसके शिष्य भी यह नहीं समझ पाए थे कि उसने पतरस को यह कहते हुए ऐेसे कठोर शब्दों में क्यों डाँटा था, "दूर हट, शैतान।"
जैविक लोग कभी ऐसी बात नहीं बोल सकते, क्योंकि वे हमेशा यही सोचते रहते हैं कि दूसरे लोग उनके बारे में क्या सोचेंगे।
यह हो सकता है कि हमने देह के पापों पर जय पा ली हो। लेकिन जो सवाल अब हमारे पास आता है वह यही है कि यीशु की तरह होने के लिए हम अपने मानवीय, जैविक जीवन के संसाधनों के अनुसार जीएंगे या ईश्वरीय जीवन की सामर्थ्य के द्वारा जीएंगे।
क्या हम पवित्र आत्मा द्वारा सिद्ध किए जाएंगे या अपनी योग्यताओं द्वारा (गलातियों 3:3)?
जैविकता आत्मिक उन्नति में एक बाधा है। जब पतरस ने यीशु को सूली के मार्ग से हटाना चाहा था, तब उसने यह मसीह के लिए अपने गहरे प्रेम की वजह से किया था। लेकिन यीशु ने उसमें शैतान की आवाज़ को सुन लिया था। उसने पतरस से कहा, "तू परमेश्वर के स्वभाव में (आत्मिक) सहभागी नहीं होता, बल्कि मनुष्य के स्वभाव (जैविक) में सहभागी होता है" (मत्ती 16:23 - ऐम्प्लिफाइड)।
एक जैविक मनुष्य वह है जिसका जीवन अब भी "आदम के जीवन" द्वारा संचालित होता है। इसमें गहरा मानवीय प्रेम और धर्मी होने की इच्छा भी हो सकती है, लेकिन यह ईश्वरीय नहीं होती।
जब परमेश्वर ने मनुष्य को रचा, तब उसने उसी रचना एक आत्मा, जीव और देह के रूप में की थी (1 थिस्स. 5:23)। मनुष्य परमेश्वर का मन्दिर होने के लिए रचा गया था। और जब परमेश्वर ने मूसा को तम्बू का नमूना दिखाया था, तब उसमें यही त्रिभागीय विभाजन देखा गया था - क्योंकि वह मनुष्य का प्रतीक था जो परमेश्वर के रहने का स्थान है।
तम्बू के तीन हिस्से थे। एक हिस्सा खुला हुआ था - बाहरी आँगन - और यह मनुष्य की देह का प्रतीक था, जिसे देखा जा सकता है। अन्य दो भाग - पवित्र स्थान और महापवित्र स्थान - ढाँपे हुए थे - और ये मनुष्य के अदृश्य हिस्से - क्रमशः जीव और आत्मा के प्रतीक थे।
परमेश्वर की उपस्थिति महापवित्र स्थान में थी। वहाँ से वह मनुष्य से बात करता था। जब हमारा नया जन्म होता है, तब पवित्र आत्मा हमारी आत्मा को जीवित करता है, और हमें प्रभु के साथ एक आत्मा कर देता है (1 कुरि. 6:17) - वैसे ही जैसे पति और पत्नी एक देह हो जाते हैं। परमेश्वर की यह इच्छा है कि वह हमारे छुटकारा पाए हुए जीव और आत्मा के द्वारा हम पर राज करे। अगर हम यह देख लें, और हमारे लिए परमेश्वर के इस उद्देश्य को पूरा होने देने के लिए अपने आपको उसके अधीन कर दें, तो हम आत्मिक मनुष्य बन सकते हैं।
मनुष्य के जीव में मन (सोचने वाला अंग), उसकी भावनाएं (महसूस करने वाला अंग), और उसकी इच्छा (फैसला करने वाला अंग) होते हैं। वह इनमें से किसी के भी द्वारा परमेश्वर के संपर्क में नहीं आ सकता, वैसे ही जैसे वह अपनी देह के द्वारा परमेश्वर को नहीं छू सकता क्योंकि परमेश्वर एक आत्मा है (यूहन्ना 4:24)।
जैसे भौतिक संसार को सिर्फ भौतिक/दैहिक तत्वों से बनी देह के द्वारा ही छुआ जा सकता है, वैसे ही आत्मिक संसार को सिर्फ आत्मा के द्वारा ही छुआ जा सकता है। अगर हम जीव और आत्मा के बीच के फ़र्क को नहीं जान पाएंगे, तो जैविक परिमण्डल में, हम शैतान की उन नकली बातों द्वारा धोखा खाएंगे जिनमें वह पवित्र आत्मा के काम की नकल करता है।
हम सिर्फ अपने जीव द्वारा परमेश्वर को नहीं जान सकते। जहाँ तक परमेश्वर को जानने की बात है, तो वहाँ एक चतुर मन किसी भी तरह से एक निबुद्धि मन से श्रेष्ठ नहीं होता, क्योंकि एक व्यक्ति की जैविक क्षमता उसे किसी भी तरह से एक ऐसी बात में श्रेष्ठ नहीं बना सकती जिसे सिर्फ आत्मा में ग्रहण किया जा सकता है। जीव और आत्मा पूरी तरह से अलग हैं। इसलिए, एक व्यक्ति का उसके जीव द्वारा परमेश्वर को जानने की कोशिश करना उतना ही मूर्खतापूर्ण है जितना अपने कान से देखने की कोशिश करना!
हम इस बारे में विचार करें कि हम पवित्र शास्त्र का अध्ययन कैसे करते हैं। परमेश्वर का वचन पढ़ते समय हम अपनी आँखें (देह) और मन (जीव) का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन अगर पवित्र-आत्मा हमें वचन का प्रकाशन नहीं देता, तो हमारी आत्मा फिर भी मध्यरात्रि की तरह अंधकारमय हो सकती है। बाइबल का ज्ञान सिर्फ यह साबित करता है कि आपका एक अच्छा मन - एक शक्तिशाली जीव है। आपकी आत्मा फिर भी अंधी हो सकती है। परमेश्वर अपने भेदों को चतुर और ज्ञानी लोगों से छुपाए रखता है लेकिन बच्चों पर प्रकट कर देता है (मत्ती 11:25)। यीशु मसीह के समय के ज्ञानियों का अंधापन इस बात का सबसे स्पष्ट प्रमाण है (1 कुरि- 2:7,8)।
हमारी भावनाएं भी हमारे जीव का हिस्सा हैं। परमेश्वर को भावना द्वारा भी नहीं जाना जा सकता। भावनात्मक उत्साह आत्मिकता नहीं सिर्फ जीव की उत्तेजना होती है। यह एक व्यक्ति की गहराई में मौजूद पाप के साथ वैसे ही अपना सह-अस्तित्व बनाए रख सकती है जैसे बौद्धिक चतुराई भी पाप के साथ रह सकती है।
कर्मेल पर्वत पर बाल के नबी बहुत भावुक होकर चिल्ला रहे थे, चीख़ रहे थे और नाच रहे थे (1 राजा 18:26-29), लेकिन वे आत्मिक नहीं थे। बहुत भावुकता से भरी अनेक मसीही सभाओं में भी ऐसी अभिव्यक्तियाँ पाई जा सकती हैं जिनका सच्ची आत्मिकता से कोई सम्बंध नहीं होता।
यहूदा इस्करियोती शिष्यों में शायद सबसे चतुर था, लेकिन उसकी जैविक शक्ति से वह परमेश्वर के सत्य को नहीं जान सका था। यरूशलेम के विद्वान भी वह न समझ सके थे जो पतरस ने, अनपढ़ होते हुए भी, ईश्वरीय प्रकाशन द्वारा समझ लिया था (मत्ती 16:17)।
हम अपने जीव की शक्ति से परमेश्वर को नहीं जान सकते। एक जैविक मसीही यही करने की कोशिश करता है।
एक जैविक मसीही नम्र व दीन नज़र आ सकता है, लेकिन वह हमेशा अपनी नम्रता के प्रति सतर्क रहता है। सच्ची नम्रता स्वयं के प्रति सचेत नहीं रहती। एक जैविक मसीही को नम्र व दीन नज़र आने के लिए कोशिश करनी पड़ती है, जबकि सच्ची नम्रता हमेशा सहसा और सहज ही होती है, क्योंकि वह भीतर से आती है।
एक जैविक विश्वासी में धार्मिकता के लिए बहुत उत्साह भी नज़र आ सकता है। वह चाबुक लेकर लोगों को कलीसिया से बाहर भी निकाल सकता है, और स्वयं को एक नबी मानते हुए पाप के खिलाफ़ ज़बरदस्त प्रचार भी कर सकता है। लेकिन अपने कामों के लिए वह मनुष्यों की प्रशंसा चाहता है। उसकी एक नज़र हमेशा मनुष्यों पर रहती है। एक जटिल प्रकार की जैविकता भी होती है जिसमें एक व्यक्ति यह कह सकता है, "मेरे बारे में कोई क्या सोचता है, मुझे इसकी कोई परवाह नहीं है।" लेकिन यही बात उसकी जैविकता को दर्शाती है कि वह लोगों को यह बताना चाहता है कि वह इस बात की परवाह नहीं करता कि वे उसके बारे में क्या सोचते हैं।
जैविक विश्वासी बहुत संवेदना से भरे हुए भी नज़र आ सकते हैं। लेकिन वह संवेदना मानवीय और नासमझी-भरी होगी। जैसे, एक जैविक मसीही, प्रेम करने वाला नज़र आने के लिए, किसी ऐसे ज़रूरतमंद व्यक्ति को नियमित भौतिक सहायता भेजने वाले हो सकता है जो एक ऐसा उड़ाऊ पुत्र हो जो परमेश्वर द्वारा अनुशासित किया जा रहा हो। तब ऐसी सहायता उस व्यक्ति के परमेश्वर की तरफ मन फिराने में एक रुकावट ही बनेगी। लेकिन एक जैविक विश्वासी को इससे मदद ही मिलेगी क्योंकि उसकी कल्पनानुसार वह परमेश्वर की सेवा कर रहा है, और वह यह नहीं जानता कि अपने ऐसे "प्रेम के कामों" के द्वारा असल में वह शैतान के उद्देश्यों को ही पूरा कर रहा है।
ऊपर अनेक सम्भावनाओं के थोड़े से उदाहरण दिए गए हैं। लेकिन इनके द्वारा हमें जैविक और आत्मिक कामों के बीच का फ़र्क साफ नज़र आ जाना चाहिए।
जैविक फल आत्मिक फल जैसा नज़र आ सकता है, और बहुत लोग इससे धोखा खा जाते हैं। हम भी इसमें धोखा खा सकते हैं।
एक खाने की मेज़ पर बैठे बहुत लोग वहाँ रखे प्लास्टिक के संतरों और केलों से धोखा चुके हैं। लेकिन वे सिर्फ दिखाने के लिए हैं और उनका कोई पोषक मूल्य नहीं होता। मसीही गुणों की जैविक नकल भी ऐसी ही होती है।
जो कुछ अभी तक कहा गया है, उसका अर्थ यह नहीं है कि हमारा जीव किसी काम का नहीं है। स्वयं परमेश्वर ने ही मनुष्य के जीव की रचना की है, और उसने उसका एक काम तय किया है। हमें अपने विचारों और भावनाओं का इस्तेमाल करना है, लेकिन सच्ची आत्मिकता का आरम्भ तब होता है जब हम अपने आपको परमेश्वर के हाथ के नीचे दीन करते हैं, और अपनी इच्छा (जो हमारी आत्मा का द्वार है) उसे अर्पित कर देते हैं। यीशु हमारे इसी द्वार से अन्दर आने के लिए उसके बाहर खड़ा रहता है (प्रका. 3:20)।
जब हम वह कहने के लिए तैयार हो जाते हैं जो यीशु ने अपनी देह में रहने के दिनों में किया था, "मेरी नहीं पर तेरी इच्छा पूरी हो," सिर्फ तभी हम यीशु की तरह जीवन जीने वाले हो सकेंगे। तब परमेश्वर हमारी आत्मा में राज कर सकेगा। और हमारा जीव परमेश्वर के आत्मा का सेवक बन जाएगा। और फिर हमारी देह भी पवित्र आत्मा के वश में हो जाएगी। सिर्फ ऐसे मनुष्य को ही "आत्मिक मनुष्य" या "आत्मा से भरा हुआ मनुष्य" कहा जा सकता है।
मन-फिराव, पवित्र-आत्मा में बपतिस्मा, और आत्मिक दान-वरदानों का इस्तेमाल एक व्यक्ति को आत्मिक नहीं बनाते, जैसा कि कुरिन्थियों की कलीसिया के विश्वासियों के उदाहरण से स्पष्ट हो जाता है। वे आत्मा के सारे दान-वरदानों से परिपूर्ण थे, फिर भी वे शारीरिक पापों के दास थे, और अपने बौद्धिक ज्ञान और भावनात्मक अनुभवों पर घमण्ड करते थे। वे आत्मिक नहीं थे।
हमने यह देखा है कि मिलाप वाले तम्बू में, परमेश्वर की उपस्थिति महापवित्र स्थान में थी। महापवित्र स्थान और पवित्र स्थान के बीच में एक मोटा पर्दा होता था। इस पर्दे की वजह से ही महापवित्र स्थान की महिमा पवित्र स्थान में प्रवेश नहीं कर सकती थी। यह पर्दा शरीर का प्रतीक था (इब्रा. 10:20)। जब शरीर को सूली पर चढ़ाया जाता है (पर्दा फट जाता है), सिर्फ तभी परमेश्वर की महिमा हमारे पूरे व्यक्तित्व (जीव) में से प्रकट होती है।
अगर हम विश्वासयोग्ता के साथ उस नए और जीवित मार्ग में चलते रहेंगे जिसे यीशु ने अपनी देह के द्वारा हमारे लिए खोला है, तब परमेश्वर का जीवन हमारे व्यक्तित्व में से प्रकट होगा और ज़्यादा से ज़्यादा नज़र आता रहेगा।
तब परमेश्वर का यह वचन हमारे लिए पूरा हो जाएगा जो यह कहता है, "पाप से समझौता न करने वाले धर्मीजनों का मार्ग भोर के प्रकाश के मार्ग की तरह होता है - वह ज़्यादा तेज़ और साफ ज्योति में बढ़ता रहता है - जब तक कि वह सिद्धता के उस दिन में (जब मसीह आएगा) प्रवेश करते हुए, अपनी पूरी शक्ति और महिमा को प्राप्त नहीं कर लेता" (नीति. 4:18, ऐम्प्लिफाइड)।
पवित्र आत्मा इसी तरह हमें महिमा के एक स्तर से दूसरे स्तर पर ले जाता है (2 कुरिन्थियों 3:18), जब तक कि हम यीशु के आने के दिन में पूरी तरह मसीह-समान नहीं बन जाते (1 यूहन्ना 3:2)।
हमने देखा है कि यीशु ने कभी अपनी इच्छा को पूरा नहीं किया था। उसने अपना जीवन कभी अपने मन और भावनाओं के अनुसार नहीं बिताया था। वह आत्मा में रहता था और उसका मानवीय जीव पवित्र आत्मा के वश में रहता था। यीशु ने अपने मन और भावनाओं को भरपूरी से इस्तेमाल किया था, लेकिन वे हमेशा पवित्र आत्मा के सेवक बन कर रहे, जो उसके जीवन में प्रभु था। इस तरह, परमेश्वर की महिमा उसके अन्दर से रुकावट बिना उसकी परिपूर्णता में प्रकट हो सकी थी।
बाइबल यह सिखाती है कि हमारा जीवन और काम यीशु के पृथ्वी पर लौटने के दिन आग द्वारा परखा जाएगा (1 कुरि. 3:10-14)। आग द्वारा परखे जाने पर यह तय होगा कि हमारा काम जैविक था या आत्मिक था। हमें उत्साहित करते हुए सोने, चाँदी और मूल्यवान पत्थरों से निर्माण करने के लिए कहा गया है जो आग में से गुज़र सकते हैं, लकड़ी, घास-फूस और भूसे पर से नहीं जो आग में राख हो जाते हैं।
सोने, चाँदी और मूल्यवान पत्थरों से बनाने का क्या अर्थ है?
रोमियों 11:36 हमें इसका जवाब देता है। वहाँ हमें यह बताया गया है कि "सब बातें परमेश्वर से हैं, उसके द्वारा हैं, और उसके लिए हैं।"
सारी सृष्टि का आरम्भ परमेश्वर में से हुआ है, वह उसके सामर्थ्य के द्वारा सम्भाली जाती है, और उसका उद्देश्य उसकी महिमा करना है। लेकिन शैतान और मनुष्यों ने उसकी इस व्यवस्था को भंग किया है।
लेकिन सिर्फ वही जिसका आरम्भ परमेश्वर में हुआ है, जो परमेश्वर की सामर्थ्य द्वारा किया जाता है, और परमेश्वर की महिमा में किया जाता है, सिर्फ वही अनन्त होता है। बाक़ी सब मिट जाएगा, मसीह के न्यायासन के सामने आग में भस्म हो जाएगा।
इसलिए, वह जिसका आरम्भ मनुष्य के जीव (मनुष्य में) होता है, मनुष्य की शक्ति द्वारा किया जाता है, और मनुष्य की महिमा के लिए किया जाता है, वह लकड़ी, घास-फूस और भूसा होता है, चाहे उसे मसीही काम भी क्यों न कहा जाए!
दूसरी तरफ, वह जिसका आरम्भ परमेश्वर में होता है, जो उसकी सामर्थ्य द्वारा किया जाता है, और उसकी महिमा के लिए किया जाता है, वह न्याय के दिन सोने, चाँदी और मूल्यवान पत्थरों के रूप में प्रकट होगा।
अंतिम दिन हमारे काम की मात्र नहीं बल्कि उसकी गुणवत्ता को परखेगा। हमारे द्वारा बनाई गई इमारत के आकार से ज़्यादा हमारे द्वारा इस्तेमाल की गई सामग्री का महत्व ज़्यादा होगा। हमारे काम का मूल, उसकी सामर्थ्य और उसका उद्देश्य इस बात से बहुत ज़्यादा मूल्यवान होंगे कि हमने कितना काम या बलिदान किया है।
हमारे जीव में नहीं बल्कि पवित्र-आत्मा में जीने के इस मामले में, यीशु हमारा उदाहरण है। उसने कभी अपनी ख़ुदी में से, या अपनी मानवीय योग्यता में, या अपनी महिमा के लिए, कोई काम नहीं किया था। उसने सिर्फ वही किया जिसका मूल परमेश्वर में था, और जो उसने परमेश्वर की सामर्थ्य में, और परमेश्वर की महिमा के लिए किया।
उसने अपने शिष्यों से बार-बार कहा था, फ्जो भी अपना जैविक-जीवन बचाना चाहेगा, वह उसे खो देगा, लेकिन जो भी मेरे लिए अपना जैविक-जीवन खोएगा, वह उसे पा लेगा।य् यीशु द्वारा जैविक-जीवन को खो देने की बात चारों सुससमाचारों में सात बार दोहराई गई है (मत्ती 10:39; 16:25; मरकुस 8:35; लूका 9:24; 14:26; 17:33; यूहन्ना 12:25)।
अगर पवित्र-आत्मा ने चारों सुसमाचारों में जैविक-जीवन से घृणा करने (या उसे खो देने) की बात को सात बार दोहराए जाने योग्य जाना, तो अवश्य ही यह बात यीशु द्वारा सिखाई गई बातों में बहुत महत्वपूर्ण बात रही होगी। ऐसे विश्वासी बहुत कम हैं जो यीशु की बात का अर्थ समझ पाए हैं।
हम अपने जीवन में जैविक और आत्मिक के बीच के फ़र्क को कैसे जान सकेंगे? इसका जवाब हैः यीशु की ओर देखने द्वारा जो जीवित वचन है, जिसे पवित्र-आत्मा ने हम पर पवित्र शास्त्रों द्वारा प्रकट किया है जो लिखित वचन है।
हमें अपना न्याय करते रहना है, अपने जीव की ज्योति द्वारा नहीं, बल्कि परमेश्वर की ज्योति द्वारा (भजन. 36:9)। और वह ज्योति यीशु में (यूहन्ना 8:12) और परमेश्वर के वचन (भजन. 119:105) में मिलती है।
यीशु ने, जो देहधारी वचन है, कहा, "मेरे उदाहरण से सीखो... और तुम अपने जैविक कामों से विश्राम पाओगे" (मत्ती 11:29, भावानुवाद)।
हम यह भी पढ़ते हैं कि "परमेश्वर का वचन जैविक को आत्मिक से अलग करता है और हमें दिखाता है" (इब्रा- 4:12, भावानुवाद)।
इसलिए इस क्षेत्र में ज्योति पाने के लिए, हमें अपने उदाहरण (अग्रदूत) यीशु की तरफ, और अपने मार्गदर्शक पवित्र-आत्मा की तरफ देखते रहना है। सिद्धता यीशु के पार्थिव जीवन में और परमेश्वर के वचन में पाई जाती है। इसलिए हमें ध्यान लगाकर इनकी तरफ देखते रहना है।
"क्योंकि सब कुछ उसी की ओर से है" (रोमियों. 11:36)।
यीशु ने कहा कि स्वर्ग का राज्य उन्हीं का है जो मन में दीन हैं (मत्ती 7:21)। स्वर्ग का राज्य अनन्त है, और वहाँ सिर्फ वही पाया जाएगा जो परमेश्वर की इच्छा में किया गया होगा। आत्मा में वही लोग दीन होते हैं जो यह जानते हैं कि वे अपनी मानवीय क्षमताओं में अधूरे हैं, और इसलिए वे पूरी तरह परमेश्वर की इच्छा के प्रति समर्पित हो सकते हैं।
इस भावार्थ से, यीशु आत्मा में हमेशा दीन-हीन दशा में ही रहा था। उसने वैसा ही जीवन बिताया, जैसा परमेश्वर ने मनुष्य के लिए चाहा था - परमेश्वर से अलग होकर अपने मन की शक्तियों का इस्तेमाल करने से इनकार करते हुए, और लगातार परमेश्वर पर निर्भर रहते हुए। उसके द्वारा कहे गए शब्दों पर विचार करेंः "पुत्र स्वयं (अपने अन्दर से) कुछ नहीं कर सकता... मैं स्वयं कुछ नहीं करता, बल्कि वही कहता हूँ जो मुझे पिता ने सिखाया है... मैं अपनी नहीं बल्कि अपने भेजने वाले की इच्छा पूरी करने के लिए आया हूँ... क्योंकि मैंने अपनी तरफ से बात नहीं की है, लेकिन पिता जिसने मुझे भेजा है उसी ने मुझे आज्ञा दी है कि मैं क्या बोलूँ और क्या कहूँ... जो बातें मैं तुमसे कहता हूँ अपनी तरफ से नहीं कहता, बल्कि पिता मुझमें रहकर अपना काम करता है" (यूहन्ना 5:19,30; 8:28,42; 12:49; 14:10)।
यीशु ने एक ज़रूरत को देखकर कभी कोई काम नहीं किया। वह एक ज़रूरत को देखता था, उसकी उसमें दिलचस्पी होती थी, लेकिन वह सिर्फ तभी कुछ करता था जब उसका पिता उसे कहता था।
जगत हालांकि निराशा की दशा में पड़ा एक मुक्तिदाता खोज रहा था, फिर भी उसने स्वर्ग में कम-से-कम चार हज़ार साल तक इंतज़ार किया, और वह तभी आया जब उसे पिता ने भेजा (यूहन्ना 8:42)। "जब सही समय आ गया, वह समय जो पिता ने तय किया था, तब उसने अपने पुत्र को भेजा" (गला. 4:4, लिविंग)। परमेश्वर ने हरेक बात के लिए एक सही समय ठहराया हुआ है (सभो. 3:1)। उस समय को सिर्फ परमेश्वर ही जानता है, इसलिए यीशु की तरह अगर हम भी हरेक बात में परमेश्वर की इच्छा चाहेंगे, तो हम कोई ग़लती नहीं करेंगे।
और पृथ्वी पर आने के बाद, ऐसा नहीं था कि वह वही करता रहा जो उसे अच्छा लगा। हालांकि उसका मन पूरी तरह शुद्ध था, फिर भी उसके मन में आने वाले हरेक अच्छे विचार के अनुसार उसने कभी कोई काम नहीं किया था। नहीं। उसने अपने मन को पवित्र आत्मा का दास बना दिया था।
हालांकि 12 साल की उम्र में वह पूरी तरह से पवित्र शास्त्र का ज्ञान प्राप्त कर चुका था, फिर भी अगले 18 साल तक एक बढ़ई का काम करते हुए वह अपनी माता के साथ रहा, और मेज़-कुर्सियाँ आदि बनाता रहा। उसके आसपास मनुष्य मर रहे थे और उन्हें बचाने वाले जिस संदेश की उन्हें ज़रूरत थी वह उसके पास था, फिर भी वह प्रचार करने की सेवकाई में बाहर नहीं निकला था। क्यों? क्योंकि तब तक पिता का समय नहीं हुआ था।
यीशु को इंतज़ार करने में कोई डर नहीं था।
"जो विश्वास करेगा वह उतावली न करेगा" (यशा. 28:16)।
और जब उसके पिता का समय हो गया, तब वह अपनी बढ़ई की दुकान से निकल कर प्रचार करने लगा था। उसके बाद, वह अक्सर किसी-न-किसी काम के बारे में कहता रहता था, "मेरा समय अभी नहीं आया है" (यूहन्ना 2:4; 7:6)। यीशु के जीवन में सब कुछ पिता के समय और इच्छा के अनुसार तय होता था।
अपने आप में, मनुष्यों की ज़रूरत कभी यीशु को सक्रिय होने के लिए मजबूर नहीं कर सकती थी, क्योंकि इसमें उसे अपनी ख़ुदी में से काम करना पड़ता - अपने जीव में से। मनुष्यों की ज़रूरतों को अपने ध्यान में रखना था, लेकिन वह परमेश्वर की इच्छा थी जिसे पूरा करना था। यूहन्ना 4:34,35 में यीशु ने इस बात को बिलकुल स्पष्ट कर दिया था।
ज़रूरत (पद 35): "अपने चारों तरफ देखो! मनुष्यों के जीवों के विशाल खेत खड़े हैं और पक गए हैं, और अब कटाई के लिए तैयार हैं।"
सक्रिय होने का सिद्धान्त (पद 34): "मेरा पोषण मुझे भेजने वाले मेरे पिता की इच्छा पूरी करने में से, और मेरे काम को पूरा करने में से आता है।"
यीशु ने अपने मित्रों द्वारा सुझाए गए बहुत से अच्छे काम नहीं किए थे, क्योंकि वह जानता था कि अगर वह मनुष्यों की सुनेगा और वह करेगा जो अच्छा नज़र आता है, तो जो सबसे अच्छा उसके पिता ने उसके लिए रखा था, वह उसे पाने से चूक जाएगा।
एक बार जब लोगों ने उसे एक जगह पर कुछ समय और रुक जाने के लिए कहा, तो उसने कहा कि वह नहीं रुक सकता क्योंकि उसने अपने पिता की आवाज़ को उसे कहीं और जाने के लिए कहते हुए सुन लिया था। मानवीय रीति से कहें तो उस जगह पर कुछ समय और रुक जाने के योग्य कारण थे क्योंकि उसके संदेश को लोग एक असामान्य रूप में ग्रहण कर रहे थे। लेकिन परमेश्वर के विचार मनुष्य के विचार नहीं होते और न ही परमेश्वर के मार्ग मनुष्यों के मार्ग होते हैं (यशा- 55:8)। इससे पहले कि यीशु ने पतरस और दूसरे लोगों के सुझाव सुने, उस दिन की भोर में यीशु ने अकेले जाकर प्रार्थना की थी, और उसने अपने पिता की आवाज़ को सुन लिया था (मरकुस 1:35-39)। यीशु मानवीय सोच-समझ पर भरोसा नहीं करता था। वह उस वचन का पालन करता था जो कहता है, "अपनी सोच-समझ का सहारा न लेना, और अपने सब कामों में परमेश्वर को याद रखना, तब वह तेरे लिए सीधा मार्ग निकालेगा" (नीति. 3:5,6)।
यशायाह 50:4 यीशु के बारे में नबूवत करते हुए कहता है, "प्रति भोर वह (पिता) मुझे जगाता है, और अपनी इच्छा के प्रति मेरी समझ को खोलता है।" यह यीशु की आदत थी। वह भोर के समय से लेकर सारा दिन पिता की आवाज़ को सुनता रहता था, और जो कुछ पिता उससे कहता था, वह हूबहू वही करता था। जो कुछ करना होता था, वह करने के लिए वह मनुष्यों से चर्चाएं नहीं करता था, लेकिन वह पिता के साथ प्रार्थना-संगति में रहता था। जैविक मसीही मनुष्यों के साथ चर्चाएं करने के बाद फैसले करते हैं। आत्मिक मनुष्य पिता से सुनना चाहते हैं।
यीशु अपने पिता के अनुसार जीता था (यूहन्ना 6:57)। यीशु के लिए, परमेश्वर का वचन खाने से भी ज़्यादा ज़रूरी था (मत्ती 4:4)। उसे दिन में कई बार, पिता से सीधे तौर पर वह पाने की ज़रूरत महसूस होती थी। और उसे पाने के बाद, वह उसका पालन करता था। आज्ञापालन भी उसके लिए प्रतिदिन के खाने से बढ़कर था (यूहन्ना 4:34)। यीशु अपने पिता पर निर्भर रहता था। पूरे दिन उसका मनोभाव यह रहता था, "बोल, पिता, मैं सुन रहा हूँ।"
उसके द्वारा मन्दिर में से लेन-देन करने वालों को बाहर निकालने के बारे में विचार करें। बहुत बार ऐसा अवश्य ही हुआ था जब यीशु ने मन्दिर में आते-जाते समय वहाँ लेन-देन करने वालों को नहीं निकाला था। उसने ऐसा तभी किया जब उसके पिता ने उसे वह करने के लिए कहा। जैविक मसीही लेन-देन करने वालों को या तो हमेशा ही निकालता रहेगा या फिर शायद कभी नहीं निकालेगा। लेकिन वह जो परमेश्वर की अगुवाई में चलता है, यह जानता है कि उसे कब, कहाँ और कैसे क्रियाशील होना है।
ऐसे बहुत से भले काम थे जो यीशु कर सकता था लेकिन उसने वे नहीं किए क्योंकि उसके लिए वे काम पिता की इच्छा की परिधि से बाहर थे। वह हमेशा सर्वश्रेष्ठ काम ही करता था। और वे काफी थे। वह पृथ्वी पर अच्छे काम करने के लिए नहीं बल्कि अपने पिता की इच्छा पूरी करने के लिए आया था।
उसने 12 साल की उम्र में मरियम और युसुफ से पूछा था, "क्या तुम नहीं जानते कि मैं अपने पिता का काम करता हुआ पाया जाऊँ" (मरकुस 2:49 - शाब्दिक अनुवाद)। वह सिर्फ इन्हीं बातों को पूरा करने में दिलचस्पी रखता था। पृथ्वी पर साढ़े 33 साल पूरे करने के बाद, वह पूरे संतोष के साथ यह कह सका, "हे पिता, जो कुछ तूने मुझे करने के लिए कहा, मैंने वह सब पूरा कर दिया है" (यूहन्ना 17:4)।
वह पूरे जगत में नहीं घूमा था, उसने कोई पुस्तक नहीं लिखी थी, उसके शिष्यों की संख्या भी कम थी, और पूरे जगत में ऐसी बहुत सी बातें थीं जिनका पूरा होना अभी बाक़ी था। लेकिन जो काम उसे पिता ने सौंपा था, उसने वह पूरा कर दिया था। अंत में, सिर्फ यही बात है जिसका पूरा होना ज़रूरी होता है।
यीशु यहोवा परमेश्वर का सेवक था। और एक सेवक की सबसे बड़ी बात यही होती है कि "वह सिर्फ वही करता है जो उसका स्वामी उसे करने के लिए कहता है" (1 कुरि. 4:2 - लिविंग)। यीशु ने थकान या झुंझलाहट भरी 'व्यस्तता' बिना, अपना पूरा जीवन पिता की सुनने में बिताया, और इस तरह अपने पिता की सम्पूर्ण इच्छा को पूरा किया। उसने अपनी मानवीय दिलचस्पियों को मृत्यु के हवाले कर दिया था। वह जैविक नहीं था। वह आत्मिक था।
यीशु ने अपने जीवन में प्रार्थना को एक उच्च प्राथमिकता दी थी। यीशु ने अपने जीवन में प्रार्थना को एक ऊँचा दर्जा दिया था। वह अक्सर सूनसान स्थानों में निकल जाता था और प्रार्थना करता था। एक बार अपने 12 शिष्यों के चुनाव के बारे में उसने पूरी रात प्रार्थना की थी (लूका 6:12,13)। एक जैविक मसीही प्रार्थना में परमेश्वर की बाट जोहने में बिताए गए समय को एक व्यर्थ समय मानता है, और वह सिर्फ अपने विवेक को शांत रखने के लिए प्रार्थना करता है। उसके जीवन में प्रार्थना एक आग्रही ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि उसे अपने ऊपर भरोसा होता है। लेकिन एक आत्मिक व्यक्ति सब बातों के लिए हमेशा परमेश्वर पर निर्भर रहता है, और अपनी इस ज़रूरत की वजह से ही उसे प्रार्थना करनी पड़ती है।
यीशु ने कहा कि सिर्फ एक बात ज़रूरी है, और वह है उसका वचन सुनना (लूका 10:42)। बैतनिय्याह की मरियम इसका एक उदाहरण थी। दूसरी तरफ, मार्था थी जो हालांकि निःस्वार्थ सेवा में व्यस्त थी, फिर भी वह बेचैनी से भरी और मरियम की आलोचना करने वाली थी। इन दोनों बहनों में हम जैविक और आत्मिक काम के बीच का फ़र्क देख सकते हैं। प्रभु और उसके शिष्यों की सेवा करने में मार्था कोई पाप नहीं कर रही थी। फिर भी वह बेचैन थी और मरियम की आलोचना कर रही थी। यह जैविक सेवा का एक स्पष्ट उदाहरण है। जैविक विश्वासी बेचैन और चिड़चिड़ा होता है। उसने "अपने काम" बंद नहीं किए हैं और उसने परमेश्वर के विश्राम में प्रवेश नहीं किया है (इब्रा. 4:10)। उसके उद्देश्य अच्छे हैं, लेकिन उसने यह नहीं समझा है कि उसके अपने काम, चाहे वे कितने भी अच्छे क्यों न हों, उसके मन-फिराव के बावजूद परमेश्वर की नज़र में सिर्फ "मैले चिथड़े" ही हैं (यशा. 64:6)।
अमालेकियों की अच्छी भेड़ें (शरीर) बुरी भेड़ों की तरह ही परमेश्वर को ग्रहणयोग्य नहीं होतीं (1 शमू. 15:3,9-19)। लेकिन मानवीय सोच-समझ इस बात को नहीं जान सकती। जबकि अच्छी भेड़ें परमेश्वर को अर्पित की जा सकती हैं, तो उन्हें फेंक देना मूर्खतापूर्ण लगता है। लेकिन परमेश्वर बलिदान नहीं आज्ञापालन चाहता है। "आज्ञापालन करना बलिदान करने से उत्तम है" (1 शमू. 15:22)। लेकिन अगर हम वह नहीं सुनेंगे जो परमेश्वर कहना चाहता है, तो हम आज्ञापालन कैसे कर सकते हैं। आज्ञापालन से पहले सुनना होता है। इसलिए यीशु ने कहा कि ज़रूरी बात यह है कि उसकी आवाज़ को सुना जाए। बाक़ी सब कुछ इस पर ही निर्भर करता है।
वे जो मार्था की तरह फ्सेवाय् करते हैं, चाहे कितनी भी निष्ठा से क्यों न करते हों, वे असल में सिर्फ अपनी ही सेवा कर रहे हैं। उन्हें प्रभु के सेवक नहीं कहा जा सकता, क्योंकि एक सेवक अपने स्वामी की सेवा करने से पहले यह इंतज़ार करता है कि उसका स्वामी उससे क्या करने के लिए कह रहा है। अगर हम अपने आपको अपनी आत्म-निर्भरता से ख़ाली कर लेंगे, तब हम सुलेमान की तरह प्रार्थना कर सकेंगे, "हे मेरे प्रभु परमेश्वर, अपने सेवक को एक सुनने वाला हृदय दे कि वह भले और बुरे की परख कर सके" (1 राजा 3:7, 9 कोष्ठक)। यीशु यह जानता था कि उसे यह परखने के लिए कि क्या अच्छा है (उसके सर्वोच्च रूप में) और क्या अच्छा नहीं है, अपने पिता की बात सुनने की ज़रूरत थी - यह परखने के लिए कि कौन सी बातें उसके पिता की इच्छा में थीं और कौन सी नहीं थीं।
यरूशलेम में मन्दिर के सुन्दर फाटक के बाहर, यीशु अक्सर एक लंगड़े व्यक्ति को भीख माँगते हुए देखता था। लेकिन उसने उसे चंगा नहीं किया था क्योंकि ऐसा करने के लिए उसने अपने पिता से कोई अगुवाई नहीं पाई थी। बाद में, जब वह स्वर्ग चला गया, तब पिता के ठहराए हुए सिद्ध समय में वह व्यक्ति पतरस और यूहन्ना द्वारा चंगा किया गया, और उसकी चंगाई द्वारा बहुत लोगों ने प्रभु की तरफ मन फिराया था (प्रेरितों. 3:1-4:4)। उसकी चंगाई के लिए पिता का ठहराया हुआ यही समय था। अगर यीशु ने उस व्यक्ति को पहले चंगा किया होता, तो वह पिता की इच्छा में रुकावट पैदा करने वाला बन जाता। वह जानता था कि पिता का समय सिद्ध होता है, इसलिए किसी काम को करने के लिए वह कभी बेचैन नहीं होता था।
यीशु का जीवन पूरे विश्राम का जीवन था। अपने पिता की इच्छा पूरी करने के लिए, प्रतिदिन 24 घण्टे का समय उसके लिए पर्याप्त रहता था। लेकिन अगर वह ऐसे काम करने का चुनाव करने लगता जो उसे अच्छे नज़र आते थे, तब 24 घण्टे का समय पर्याप्त न रहता, और फिर उसके ज़्यादातर दिन बेचैनी में ही गुज़रते। यीशु उसके मार्ग में आने वाले हरेक विलम्ब में आनन्दित रह सकता था, क्योंकि उसने यह सच्चाई मान ली थी कि स्वर्ग में एक सर्वशक्तिशाली पिता उसके प्रतिदिन का कार्यक्रम तय करता था। इसलिए किसी भी तरह का विलम्ब उसे परेशान नहीं करता था। यीशु का जीवन हमारे भीतरी मनुष्य में भी पूरा विश्राम देगा। इसका अर्थ यह नहीं है कि हम कुछ नहीं करेंगे, बल्कि यह कि हम सिर्फ वहीं करेंगे जो हमारे लिए पिता की योजना में होगा। तब ऐसा होगा कि हम अपने पूर्व-निर्धारित कार्यक्रम नहीं बल्कि पिता की इच्छा पूरी करने के लिए ज़्यादा उत्सुक होंगे।
जैविक विश्वासी "अपने काम" करने के लिए ऐसे संकल्पबद्ध रहते हैं कि वे अक्सर चिड़चिड़े और बेचैन रहते हैं। अंत में, उनमें से कुछ मानसिक व शारीरिक रूप में टूट कर बिखर जाते हैं।
यीशु का मानसिक रूप में टूट कर बिखर जाना असम्भव था, क्योंकि उसके भीतरी मनुष्य में वह पूरे विश्राम में रहता था। वह हमसे कहता है, "मेरा जुआ अपने ऊपर उठा लो और मुझसे सीखो, और तुम अपने मनों में विश्राम पाओगे" (मत्ती 11:29)। परमेश्वर का आत्मा पवित्र शास्त्र में से यीशु की इसी महिमा को हमें दिखाना चाहता है, हमें इसमें सहभागी बनाना चाहता है, और हमारे द्वारा इसे प्रकट करना चाहता है।
प्रभु हमारा चरवाहा है और वह अपनी भेड़ों को विश्राम देने वाले चारागाहों में ले जाता है। भेड़ें स्वयं अपने लिए कोई कार्यक्रम तय नहीं करतीं और न ही यह तय करती हैं कि उन्हें अगली बार कौन से चारागाह में जाना है। वे सिर्फ अपने चरवाहे के पीछे-पीछे चलती हैं। लेकिन इस तरह चलने के लिए एक व्यक्ति को अपनी आत्म-निर्भरता और आत्म-पूर्ति से ख़ाली होने की ज़रूरत है। यीशु सिर्फ अपने पिता के पीछे चलता था। लेकिन जैविक विश्वासी भेड़ नहीं बनना चाहते, और इस वजह से उनकी अपनी सोच-समझ में भटक जाते हैं। हमारी सोच-समझ परमेश्वर द्वारा दिया गया एक अद्भुत और उपयोगी वरदान है, लेकिन अगर हम उसे ऊँचा उठाते हुए अपने जीवन में प्रभु की जगह दे देंगे, तो वह सारे दान-वरदानों से ज़्यादा ख़तरनाक साबित हो सकती है।
प्रभु ने अपने शिष्यों को यह प्रार्थना सिखाई, "हे पिता, जैसे तेरी इच्छा स्वर्ग में पूरी होती है, वैसे ही पृथ्वी पर भी हो।" स्वर्ग में परमेश्वर की इच्छा कैसे पूरी होती है? वहाँ स्वर्गदूत "परमेश्वर के लिए कुछ करने" की कोशिश में यहाँ-वहाँ नहीं भागते। अगर वे ऐसा करेंगे, तो स्वर्ग में अस्त-व्यस्तता हो जाएगी। वे क्या करते हैं? वे परमेश्वर की उपस्थिति में यह सुनने के लिए खड़े रहते हैं कि उन्हें क्या करना है, और फिर वे वही करते हैं जो उन्हें व्यक्तिगत तौर पर करने के लिए कहा जाता है। उन शब्दों पर ध्यान दें जो स्वर्गदूत जिब्राईल ने ज़कर्याह से कहे थे, "मैं जिब्राईल हूँ जो परमेश्वर की उपस्थिति में खड़ा रहता हूँ; मैं तुझसे बात करने के लिए भेजा गया हूँ" (लूका 1:19)। प्रभु यीशु ने भी यही किया था - अपने पिता की उपस्थिति में खड़े रहते हुए उसकी आवाज़ को सुना था, और उसकी इच्छा को पूरा किया था।
जैविक विश्वासी कठोर परिश्रम करने वाले और बड़ा बलिदान करने वाले हो सकते हैं, लेकिन अनन्त की बिलकुल स्पष्ट ज्योति यह प्रकट कर देगी कि "उन्होंने सारी रात परिश्रम किया लेकिन कुछ नहीं पकड़ा था।" लेकिन जिन्होंने अपनी प्रतिदिन की सूली उठाई है (अपने जैविक-जीवन का इनकार करते हुए उसे मृत्यु के हवाले किया है) और प्रभु की आज्ञा का पालन किया है, उस दिन उनके जाल भरे हुए होंगे (यूहन्ना 21:1-6)।
"जो भी अपने आपको उस काम से दूर हटा लेता है जिसकी योजना मैंने बनाई है," यीशु ने कहा, "वह परमेश्वर के राज्य के योग्य नहीं है" (लूका 9:62 - लिविंग)। "जो सेवा तुम्हें प्रभु में सौंपी गई है, उसे सावधानी से पूरा करो" (कुलु. 4:17)।
"ऐसा हरेक पौधा जो मेरे स्वर्गीय पिता ने नहीं लगाया, वह उख़ाड़ दिया जाएगा" (मत्ती 15:13)। इसमें सवाल यह नहीं है कि पौधा अच्छा है या बुरा है, बल्कि यह कि उसे लगाने वाला कौन है। हरेक सही/वैध बात का एकमात्र मूल परमेश्वर ही है। बाइबल की शुरूआत इन शब्दों से होती है, "आदि में परमेश्वर..." हमारे सब कामों में भी ऐसा ही होना चाहिएः "अगर उन्हें अनन्त में बने रहना है, तो यह ज़रूरी है कि उनका मूल हमारे मनों में नहीं परमेश्वर में हो।"
"जो परमेश्वर की इच्छा पूरी करता है, वह सर्वदा बना रहता है" (1 यूहन्ना 2:17)। बाक़ी सब कुछ मिट जाएगा।
इसलिए, हम अपने आपसे यह सवाल पूछेंः
"क्या मैं परमेश्वर की इच्छा में जी रहा हूँ, और क्या मैं उसमें अपना काम कर रहा हूँ?"
"सब कुछ उसी के द्वारा है" (रोमियों. 11:36)।
परमेश्वर ने आदम के जीव में अद्भुत शक्तियों की रचना की थी। जितने भी पशु-पक्षी परमेश्वर ने बनाए थे, उसने उन सबके नाम रखे थे (उत्पत्ति 2:19)। उन हज़ारों नामों में से हमारे लिए कुछ नाम याद रखना भी मुश्किल होता है। यह तो आदम के जीव की शक्ति का सिर्फ एक सांकेतिक चिन्ह् है। परमेश्वर की दी हुई इन शक्तियों का उपयोग आदम को परमेश्वर पर निर्भर रहते हुए करना था। लेकिन आदम ने उन्हें परमेश्वर से अलग होकर विकसित करना चाहा, और अदन की वाटिका में किए गए उस घातक चुनाव के बाद, आदम उसके जीव के अनुसार जीने वाला बन गया था।
अगर हमें आत्मिक और जैविक कामों का फ़र्क जानना है, तो हमें पवित्र आत्मा की शक्ति और जैविक शक्ति के बीच के फ़र्क के बारे में ज़रूर कुछ मालूम होना चाहिए, और इस तरह शैतान द्वारा की जाने वाली नकल से धोखा खाने से बचे रहना चाहिए।
आज मसीही जगत के उस क्षेत्र के बारे में विचार करें जिसमें सबसे व्यापक तौर पर मानवीय जैविक-शक्ति का इस्तेमाल किया जा रहा है - चंगाई का क्षेत्र। 19वीं शताब्दी से, विज्ञान ने मानवीय मस्तिष्क की ज़बरदस्त शक्तियों की खोज शुरू कर दी थी। सम्मोहन के विज्ञान ने अनोखी प्रगति की है और मानसिक शक्तियों की सम्भावनाएं बहुत हैरानी में डाल देने वाली हैं। सम्मोहन के सिद्धान्त अब "पवित्र-आत्मा के वरदानों" के रूप में मसीही जगत में आयात किए जा रहे हैं।
यह पवित्र-आत्मा के असली वरदानों को तुच्छ जानना नहीं है, क्योंकि जहाँ वे होंगे, वहाँ हमेशा कलीसिया की उन्नति और परमेश्वर की महिमा होगी। यह उन नकली वरदानों की बात है जो बिलकुल असली जैसे लगते हैं लेकिन जो मनुष्यों के व्यक्तित्वों को ऊँचा उठाने में, उनके अपने राज और धन-दौलत के साम्राज्य स्थापित करने की दिशा में ले जाते हैं!
इन दिनों जिसे "विश्वास से चंगाई" (मसीही व ग़ैर-मसीही) कहा जा रहा है, वह सिर्फ मानवीय मस्तिष्क की शक्तियों का इस्तेमाल हो रहा है - रोग के लक्षण मौजूद रहते हुए भी, एक व्यक्ति अपनी चंगाई के प्रति स्वयं को आश्वस्त होता हुआ पाता है। आजकल के रोग क्योंकि ज़्यादातर मनोदैहिक होते हैं (अर्थात्, ऐसे शारीरिक रोग जिनका मूल मानसिक व भावनात्मक है), इसलिए यह सच है कि "सकारात्मक सोच" और स्वयं रोग के प्रति एक बदली हुई मनोदशा अक्सर देह को चंगा कर देते हैं। लेकिन यह सिर्फ देह और मन के प्राकृतिक सिद्धान्तों के काम का परिणाम है। यह हर्गिज़ अलौकिक चंगाई नहीं है।
यीशु आज भी लोगों को चमत्कारिक रूप से चंगा करता है, लेकिन वे चंगाइयाँ ऐसी मनोवैज्ञानिक छल-कपट द्वारा नहीं होतीं। जहाँ भी चंगाई का असली वरदान काम कर रहा है, वहाँ विश्वास करने के लिए कभी मानसिक संघर्ष करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि विश्वास परमेश्वर का दान है, और वह उसके वचन में रखी प्रतिज्ञाओं पर आधारित है; विश्वास किसी "सकारात्मक सोच" में से पैदा नहीं होता।
सम्मोहन के सिद्धान्तों का पालन करने द्वारा (चाहे अनजाने में ही), मनुष्य दूसरे मनुष्यों को अपनी (जैविक शक्ति के) ऐसे अधिकार में रख सकते हैं जैसा अधिकार परमेश्वर ने उन्हें कभी नहीं देना चाहा था। मसीही जगत में अक्सर इसे भी एक व्यक्ति को पवित्र-आत्मा द्वारा दिया गया अधिकार समझ लेने की ग़लती की जा सकती है।
परमेश्वर से अलग अपनी जैविक शक्ति को बढ़ाने में बहुत से ख़तरे हो सकते हैं। परमेश्वर ने वह शक्तियाँ हमें इसलिए दी हैं कि हम उन्हें उसके इस्तेमाल के लिए उसे सौंप दें।
यीशु ने इसी तरह से जीवन बिताया था। उसने निरन्तर अपने जैविक जीवन को मृत्यु के हवाले किया था, और अपने मानवीय जीव की शक्तियों द्वारा जीवन बिताने से इनकार किया था। इसकी बजाय वह पूरी तरह से अपने पिता पर निर्भर रहा था, और अपने जीवन और अपनी सेवकाई दोनों के ही लिए उसने लगातार पवित्र-आत्मा की सामर्थ्य को पाना चाहा था।
हमने पहले ही यह देखा था कि वह अक्सर प्रार्थना करने के लिए किसी सूनसान स्थान में चला जाता था (लूका 5:16)। अपने अंतिम दिनों में, सूली पर चढ़ने से पहले, वह दिन में मन्दिर में सिखाता था और रात के समय जैतून के पहाड़ पर चला जाता था - निस्संदेह वह बाधारहित प्रार्थना में लम्बा समय बिताना चाहता था (लूका 21:37,38)।
विश्वास से जीना पिता पर इसी तरह लगातार निर्भर होकर जीना होता है।
जो परमेश्वर की सामर्थ्य के द्वारा किया जाता है सिर्फ वही अनन्त होता है। बाक़ी सब कुछ मिट जाएगा। जो व्यक्ति परमेश्वर पर निर्भर होकर रहता है, बाइबल उसकी तुलना उस पेड़ से करती है जो अपना पोषण एक ज़मीन के नीचे बहने वाली नदी में से पाता है (यिर्म. 17:5-8)। यीशु इसी तरह जीता था - मनुष्य के रूप में, अपने संसाधन लगातार पवित्र आत्मा (परमेश्वर की नदी) में से पाते हुए।
यीशु का परीक्षा/प्रलोभन पर जयवंत होना, मानवीय संकल्प द्वारा नहीं था, बल्कि इसलिए क्योंकि पल-प्रतिपल पिता में से नया बल पाता रहता था। अपनी-ख़ुदी-से-इनकार का जो रास्ता यीशु द्वारा एक नमूने के तौर पर दिखाया और सिखाया गया, ऐसा रास्ता नहीं है जिसमें स्वयं अपने आप पर प्रबल होना चाहता है। नहीं। वह बुद्ध द्वारा दिखाया गया रास्ता है, और योग है, और जो पवित्र शास्त्र की शिक्षा से इतना ही दूर है जितना पृथ्वी से आकाश दूर है।
यीशु ने यह सिखाया कि परमेश्वर के लिए जीने और उसकी सेवा करने के लिए मनुष्यों के रूप में जैसी शक्ति हमारे पास होनी चाहिए, वैसी शक्ति हमारे पास नहीं है। उसने कहा था कि हम ऐसी असहाय डालियाँ हैं जो फलवंत होने के लिए उस पोषण पर निर्भर रहती हैं जिसकी आपूर्ति पेड़ में से होती है। "मुझसे अलग होकर," उसने कहा, "तुम कुछ नहीं कर सकते" (यूहन्ना 15:5)। और इसलिए, हम पवित्र आत्मा की मदद के बिना जो कुछ भी करते हैं, हम यह मान सकते हैं कि वह कुछ नहीं है।
यही वह बात है जिसमें "पवित्र-आत्मा से निरंतर भरते रहने" (इफि. 5:18) की बड़ी ज़रूरत रखी हुई है।
यीशु स्वयं पवित्र-आत्मा के अभिषेक से भरा हुआ था (लूका 4:1,18), और वह पवित्र आत्मा की सामर्थ्य में अपने पिता के लिए जीता और काम करता था। लेकिन यह सिर्फ इसलिए सम्भव हो सका क्योंकि मनुष्य के रूप में वह आत्मा में नम्र व दीन था।
यीशु ने जो मानवीय देह धारण की थी, वह उसकी निर्बलता को जानता था। इसलिए वह हमेशा ऐसे मौक़ों की तलाश में रहता था जिसमें वह एकान्त में जाकर प्रार्थना कर सके। किसी ने यह कहा है कि जैसे पर्यटक शहरों में रहने के लिए एक अच्छा होटल और देखने के लिए दर्शनीय जगहें ढूंढते हैं, वैसे ही यीशु प्रार्थना करने के लिए एकान्त स्थान ढूंढता था।
वह परीक्षा/प्रलोभन पर जय पाने और अपनी जैविक-शक्ति को मौत के हवाले करने के लिए सामर्थ्य पाना चाहता था। शरीर की निर्बलता के प्रति जैसा यीशु सचेत था ऐसा कोई मनुष्य नहीं हो सकता था, और इसलिए प्रार्थना में पिता के सम्मुख रहते हुए जैसे उसने मदद पाना चाहा था, वैसे किसी मनुष्य ने कभी नहीं चाहा था। देह में रहने के अपने दिनों में उसने "ऊँची आवाज़ से पुकारते और आँसू बहाते हुए" प्रार्थनाएं की थीं। इसका नतीजा यह हुआ कि उसने पिता से ऐसी भरपूर सामर्थ्य पाई जैसी किसी मनुष्य ने कभी नहीं पाई थी। इस तरह, यीशु ने एक बार भी पाप नहीं किया और वह कभी अपने जीव में से नहीं जीया (इब्रा. 4:15; 5:7-9)।
क्या यह एक महत्व की बात नहीं है कि सुसमाचारों में यीशु से जुड़ी बातों में "प्रार्थना करने" या "प्रार्थना" का उल्लेख 25 बार किया गया है।
इसमें ही उसके जीवन और काम का भेद छुपा था।
यीशु उसके जीवन की बड़ी घटनाओं से पहले ही प्रार्थना नहीं करता था, वह उसकी बड़ी उपलब्धियों के बाद भी प्रार्थना करता था। एक चमत्कारिक रूप में पाँच हज़ार लोगों को खिलाने के बाद, वह प्रार्थना करने के लिए पहाड़ पर चला गया था। इसमें कोई शक नहीं कि यह वह पिता की बाट जोहते हुए गर्व या आत्म-संतोष से बचने और अपनी शक्ति को फिर से नया करने के लिए करता था (यशा. 40:31)। हम अक्सर प्रभु के लिए कोई महत्वपूर्ण काम करने से पहले प्रार्थना करते हैं। लेकिन अगर हम यीशु की तरह हमारा काम ख़त्म करने के बाद पिता के सम्मुख बाट जोहने की आदत डाल लें, तो हम अपने आपको गर्व से बचा सकते हैं और इस तरह अपने आपको प्रभु के लिए ज़्यादा बड़े काम करने के लिए तैयार कर सकते हैं।
यीशु का जीवन जितना ज़्यादा व्यस्त होता गया था, वह उतनी ही ज़्यादा प्रार्थना करने लगा था। यह ऐसे समय थे जब उसके पास खाने और आराम करने का भी समय नहीं रहता था (मरकुस 3:20; 6:31,33,46), लेकिन वह फिर भी हमेशा प्रार्थना के लिए समय निकालता था। वह जानता था कि उसे कब सोना है और कब प्रार्थना करना है क्योंकि वह पवित्र आत्मा के प्रबोधनों का पालन करता था।
प्रभावशाली प्रार्थना करने के लिए पहले आत्मा की दीनता ज़रूरी है। प्रार्थना मानवीय असहायता की अभिव्यक्ति होती है, और अगर उसे सिर्फ एक धार्मिक विधि न होकर सार्थक होना है, तो हमें लगातार यह समझते रहना होगा कि मसीही जीवन जीने या परमेश्वर की सेवा करने के लिए मानवीय संसाधन कभी पर्याप्त नहीं हो सकते।
यीशु प्रार्थना में लगातार परमेश्वर की सामर्थ्य पाने की खोज में रहता था, और इसलिए उसे कभी निराश नहीं होना पड़ता था। इस तरह, उसने प्रार्थना द्वारा वह सब कुछ हासिल किया जो वह भी किसी और तरह से हासिल नहीं कर सकता था। जिस व्यक्ति का आत्म-विश्वास मज़बूत होता है, वह पाप पर जय पाने के लिए "शारीरिक बाहुबल" पर निर्भर रहना जारी रखता है। इससे पहले कि ऐसा व्यक्ति पाप पर जय पाने के लिए परमेश्वर की सामर्थ्य को जाने, उसका टूटना ज़रूरी होता है। इसलिए परमेश्वर ऐसा होने देता है कि वह लगातार हारता रहे, माह-दर-माह, जब तक कि वह उसके "शून्य बिन्दु" पर पहुँचकर अपनी कमज़ोरी को स्वीकार नहीं कर लेता। तब परमेश्वर उस पर कृपा की आत्मा उण्डेलता है और उसे एक जयवंत जीवन में ले चलता है, और तब परमेश्वर की महिमा उसके जीवन में से प्रकट होने लगती है।
हम जब निर्बल होते हैं, वास्तव में हम तभी बलवंत होते हैं (2 कुरि. 12:10)।
अब्राहम ने इश्माएल को अपनी प्राकृतिक शक्ति से पैदा किया था, लेकिन परमेश्वर ने इश्माएल को स्वीकार नहीं किया, और उसने अब्राहम से उसे दूर कर देने के लिए कहा (उत्पत्ति 17:18-21; 21:10-14)। मसीह के न्यायासन के सामने, जब हम उसके सामने अपने ऐसे भले उद्देश्य प्रस्तुत करेंगे जो हमने परमेश्वर पर निर्भर रहे बिना अपनी मानवीय योग्यताओं द्वारा पैदा किए थे, तो वह भी हमसे कह देगा कि वे उसे ग्रहणयोग्य नहीं हैं। फिर वे लकड़ी, घास-फूस और भूसा जलकर कर राख बन जाएगा।
सिर्फ वही जो "परमेश्वर द्वारा" किया गया था, बचा रहेगा। जब अब्राहम अपनी कमज़ोरी की जगह पर आ गया - जब बच्चे पैदा करने की उसकी प्राकृतिक शक्ति ख़त्म हो गई - तब इसहाक़ का अलौकिक शक्ति द्वारा जन्म हुआ, और यह पुत्र परमेश्वर को ग्रहण-योग्य था।
जिन बातों का परमेश्वर से सम्बंध है, उनमें एक इसहाक़ एक हज़ार इश्माएलों से बढ़कर होता है। एक ग्राम सोना एक किलोग्राम लकड़ी से ज़्यादा मूल्यवान ठहरेगा - जब आग ने दोनों को परख लिया होगा। पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से किया गया थोड़ा सा भी उससे ज़्यादा होगा जो हमने अपनी शक्ति के द्वारा किया होगा।
हमारे मन-फिराव से पहले और हमारे मन फिराव के बाद, हमारे भले काम और प्रभु की सेवा करने की हमारी अपनी कोशिशें हमेशा ही मैले चिथड़ों की तरह ही होंगे। लेकिन वह धार्मिकता जो विश्वास में से पैदा होती है और वे काम जो पवित्र आत्मा पर निर्भर रहते हुए किए गए हैं, मेमने के विवाह के दिन वे हमारा विवाह का वस्त्र होंगे (प्रका. 19:8)। यह कितना बड़ा फ़र्क है - या तो मैले चिथड़े या विवाह का वस्त्र! यह सब इस बात पर निर्भर रहेगा कि हमने अपने जीवन अपनी स्वयं की जैविक शक्ति द्वारा बिताएं हैं या परमेश्वर की सामर्थ्य द्वारा बिताएं हैं।
यीशु अपनी सेवकाई के लिए भी पवित्र आत्मा की सामर्थ्य पर निर्भर था। उसने पवित्र आत्मा का अभिषेक पाने से पहले कभी प्रचार करने का साहस नहीं किया था। वह पवित्र आत्मा के सामर्थ्य द्वारा पहले से ही ऐसी सिद्ध पवित्रता में रहा था कि पिता उसके बारे में यह साक्षी दे सका, "यह मेरा प्रिय पुत्र है जिससे में अति प्रसन्न हूँ" (मत्ती 3:17)। लेकिन सेवा के लिए उसे फिर भी पवित्र आत्मा के अभिषेक की ज़रूरत थी। इसलिए उसने अभिषेक पाने के लिए प्रार्थना की थी, और उसने अभिषेक पाया (लूका 3:21)। और क्योंकि उसने धार्मिकता से ऐसा प्रेम और पाप से ऐसी घृणा की थी जैसा उससे पहले कभी किसी मनुष्य ने नहीं किया था, इसलिए उसका अभिषेक भी ऐसी भरपूरी के साथ किया गया था जैसा उससे पहले कभी किसी मनुष्य का नहीं किया गया था (इब्रा. 1:9)। इसका नतीजा यह हुआ कि उसकी सेवकाई में लोगों ने शैतान की बंधुवाई में से छुटकारा पाया। अभिषेक का यही सबसे बड़ा उद्देश्य था, और वह सबसे पहले इसी रूप में प्रकट हुआ था (देखें लूका 4:18 व प्रेरितों. 10:38)।
परमेश्वर का काम मानवीय प्रतिभाओं और योग्यताओं द्वारा नहीं किया जाता। जो मनुष्य प्राकृतिक रूप में बहुत प्रतिभाशाली होते हैं, वे उनके मन-फिराव के बाद अक्सर यह सोचते हैं कि अब वे अपनी उन प्रतिभाओं को परमेश्वर के लिए दूसरे लोगों को प्रभावित करने में इस्तेमाल कर सकेंगे।
अनेक मसीही अपनी बोलने की कला, अपने तर्क और अपनी स्पष्ट बोली को पवित्र आत्मा की सामर्थ्य समझने की ग़लती भी कर बैठते हैं। लेकिन ये सिर्फ जीव की शक्तियाँ हैं, और अगर इन पर किसी भी तरह निर्भर रहा जाएगा, तो ये परमेश्वर के काम में रुकावट ही पैदा करेंगी। मानवीय जैविक शक्ति द्वारा किया जाने वाला कोई भी काम अनन्त नहीं हो सकता। वह अगर समय में नष्ट नहीं होगा, तो मसीह के न्यायासन के आगे नष्ट हो जाएगा।
लोगों को परमेश्वर की तरफ लाने के लिए यीशु अपनी बोली की या भावना की शक्ति पर निर्भर नहीं रहता था। वह जानता था कि ऐसी जैविक शक्ति से किया गया काम उसके सुनने वालों के सिर्फ जीव तक ही पहुँच पाएगा, और इससे उनकी आत्मा को कोई लाभ नहीं होगा। और इसी वजह से, लोगों को परमेश्वर के पास लाने के लिए उसने किसी तरह के मनोरंजक संगीत को भी इस्तेमाल नहीं किया था।
परमेश्वर के सामने समर्पण करने के लिए उसने लोगों की भावनाओं को उत्तेजना के एक ऊँचे स्तर पर पहुँचाने द्वारा उनकी भावनाओं के साथ खिलवाड़ नहीं किया था। असल में, उसने ऐसे कोई जैविक तरीक़े इस्तेमाल नहीं किए थे जो आजकल के ज़्यादातर सुसमाचार प्रचारक इस्तेमाल करते हैं। लोगों को प्रभावित करने के लिए उसने भावनात्मक आवेग और जैविक उत्तेजना का इस्तेमाल नहीं किया था। ये नेता और विक्रेता का तरीक़ा होता है, और वह इनमें से एक भी नहीं था।
यहोवा के सेवक के रूप में, अपने सारे काम के लिए वह पूरी तरह से पवित्र आत्मा पर निर्भर रहता था। इसका नतीजा यह हुआ कि उसके पीछे चलने वाले लोग स्वयं परमेश्वर में एक गहरे जीवन में पहुँच सके।
यीशु ने जैविक शक्ति का इस्तेमाल करते हुए दूसरे लोगों को अपनी स्वयं की विचारधारा में शामिल होने के लिए मजबूर नहीं किया था। उसने अपने आपको कभी दूसरों पर नहीं थोपा था। उसने दूसरों को हमेशा यह आज़ादी दी थी कि अगर वे चाहें तो उसे अस्वीकार कर सकते थे। जैविक मसीही अगुवे अपने प्रबल व्यक्तित्व द्वारा अपने झुण्ड और अपने सहकर्मियों को अपने वश में रखते हैं। लोगों में ऐसे अगुवों का एक आदरयुक्त भय छा जाता है और वे श्रद्धा के साथ उनके हरेक शब्द का पालन करते हैं।
यह हो सकता है कि ऐसे अगुवे के आसपास बहुत बड़ी भीड़ जमा हो जाए और उनमें एक आपसी एकता भी हो जाए, लेकिन वह सिर्फ उस अगुवे के प्रति भक्ति की एकता ही होगी। ऐसे अगुवे क्योंकि जीव और आत्मा के बीच का फ़र्क नहीं जानते, इसलिए वे अपने आपको धोखा देते हुए यह भी सोच सकते हैं कि जो शक्ति उनके पास है, वह पवित्र आत्मा की सामर्थ्य है। उनके अनुयायी भी ऐसे ही धोखे में पड़े रहते हैं। लेकिन न्यायासन की स्पष्ट ज्योति यह प्रकट कर देगी कि वह सब मानवीय जैविक शक्ति थी और यह कि उसने परमेश्वर के काम में रुकावट पैदा की थी।
ऐसे मानवीय करिश्मा वाले तो अनेक राजनेता और ग़ैर-मसीही नायक भी होते हैं जो अपने व्यक्तित्व और बोलने की शैली आदि की शक्ति द्वारा बड़ी भीड़ इकट्ठी कर लेते हैं।
यीशु ऐसा अगुवा नहीं था। और न ही किसी मसीही को ऐसा होना चाहिए। हमें अपनी जैविक शक्ति का इस्तेमाल करने से डरना चाहिए क्योंकि वह मनुष्य के लिए बनाए गए परमेश्वर के नियमों का उल्लंघन करती है और उसकी सेवा में रुकावट बनती है।
जैविक शक्ति दूसरों में कुछ सतही बदलाव कर सकती है और उनमें ईश्वरीय भक्ति का एक आडम्बर तैयार हो सकता है, लेकिन उसमें परमेश्वर के लिए न तो कोई गहरी भक्ति होगी और न ही उनके निजी जीवन में पाप पर जय पाई जा रही होगी।
एक आत्मिक काम कभी भी मानवीय जीव द्वारा बल्कि सिर्फ पवित्र आत्मा की सामर्थ्य द्वारा ही हो सकता है। यीशु यह जानता था इसलिए वह लगातार अपनी जैविक-शक्ति को मौत के हवाले करता रहता था। इस वजह से वह थोड़े ही समय में उसके पीछे चलने वालों के अन्दर एक गहरा और स्थाई काम कर सका था।
वह अपना व्यक्तित्व कभी किसी पर नहीं थोपता था, कभी किसी पर हुक्म नहीं चलाता था, और अपनी बोली या बौद्धिक शक्तियों द्वारा किसी को भयभीत नहीं करता था। वह मनुष्यों को अपने प्रभाव में नहीं लेना चाहता था बल्कि वह उनकी मदद करना चाहता था।
जैविक मसीही दूसरों की मदद करने की बजाय उनको प्रभावित करने में ज़्यादा दिलचस्पी रखते हैं। जैविक अगुवे कलीसिया का निर्माण नहीं कर सकते, क्योंकि वे लोगों को मसीह के साथ नहीं जोड़ते जो शीर्ष है, बल्कि स्वयं अपने साथ जोड़ लेते हैं।
जिनके अन्दर बलवंत जैविक शक्ति है, उन्हें भय और थरथराहट के साथ वचन की सेवा करनी चाहिए (जैसे पौलुस ने की थी - 1 कुरि. 2:1-5) कि ऐसा न हो कि उनके श्रोताओं का भरोसा परमेश्वर की सामर्थ्य में न होकर मानवीय बुद्धि पर हो जाए।
यीशु को हर समय अपनी मानवीय निर्बलता का अहसास रहता था। उसने कहा, "मनुष्य का पुत्र अपने आपमें कुछ नहीं कर सकता..." (यूहन्ना 5:19)। और इस वजह से उसका प्रार्थनामय-जीवन बहुत गहरा था। इसलिए पिता यीशु में अपने सारे काम कर सका (यूहन्ना 14:10)।
परमेश्वर पर ऐसी निर्भरता का मनोभाव ही हमें उन बातों से दूर रखेगा जिन्हें परमेश्वर ने वर्जित किया है, और जिनसे घृणा करने के लिए हमें यीशु ने कहा है - हमारे जैविक-जीवन और उसकी शक्तियों से। तब पवित्र आत्मा प्रभु की महिमा को हममें से प्रकट कर सकेगा।
अगर हम विश्वास से जीएंगे (प्रभु पर निर्भर रहेंगे), और अगर हमारा काम एक विश्वास का काम होगा, तब हम यक़ीनन सोने, चाँदी और मूल्यवान पत्थरों से निर्माण करेंगे।
और इसलिए, अब हमें अपने आपसे यह दूसरा सवाल पूछना चाहिएः क्या मैं परमेश्वर की शक्ति से जीता और काम करता हूँ?
"सब कुछ उसी के लिए है" (रोमियों. 11:36)।
परमेश्वर अल्फा और ओमेगा है - आदि और अंत है, पहला और अंतिम है। और क्योंकि अनन्त के लिए रची गईं सब बातों की शुरूआत उसमें से हुई है, इसलिए उनको उसी में पूरा भी होना है।
परमेश्वर ने सब कुछ इसलिए रचा कि उसके द्वारा उसकी महिमा हो। परमेश्वर अपने आप में पूरी तरह से परिपूर्ण है, और हम उसे ऐसा कुछ नहीं दे सकते जो उसकी पूर्णता में कुछ जोड़ सकता हो। जब वह हमें उसकी पवित्रता के खोजी होने के लिए बुलाता है, तो वह इसलिए ऐसा करता है क्योंकि उसमें हमारी स्वयं की सर्वश्रेष्ठ भलाई है। अगर वह ऐसा नहीं करेगा तो हम स्व-केन्द्रित और घृणित बन जाएंगे।
परमेश्वर में केन्द्रित रहना एक ऐसा नियम है जो परमेश्वर ने सृष्टि में अंतर्निहित किया है। उस नियम को मुक्त इच्छा शक्ति वाले नैतिक जीवधारी ही भंग कर सकते हैं। निर्जीव सृष्टि तो अपने सृष्टिकर्ता का आज्ञापालन और उसकी महिमा करती है। लेकिन आदम ने उस नियम को तोड़ा जिसके परिणाम हम मानवजाति को दुर्गति में देख सकते हैं।
प्रभु ने अपने शिष्यों को जो प्रार्थना करनी सिखाई, उसमें सबसे पहला निवेदन यही है, "तेरा नाम पवित्र माना जाए।" प्रभु यीशु के हृदय में यह सबसे प्रमुख अभिलाषा थी। उसने प्रार्थना की, "पिता, तेरे नाम की महिमा कर," और फिर उसने सूली का मार्ग चुन लिया क्योंकि वह पिता की महिमा के लिए था (यूहन्ना 12:27,28)। प्रभु यीशु के जीवन पर एक आवेग सर्वोच्च रूप में राज करता था - पिता की महिमा।
वह सब कुछ पिता की महिमा के लिए करता था। उसका जीवन पुण्य या सासांरिक बातों के अलग हिस्सों में बँटा हुआ नहीं था। उसके लिए सब कुछ पुण्य था। उसने परमेश्वर की महिमा के लिए स्टूल और बैंच भी उसी तरह बनाए थे जैसे उसने परमेश्वर की महिमा के लिए सुसमाचार का प्रचार और बीमारों को चंगा किया था। उसके लिए हरेक दिन समान रूप में पुण्य था और प्रतिदिन की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए ख़र्च किया गया धन भी उतना ही पुण्य था जितना पुण्य वह धन था जो परमेश्वर के काम में या ग़रीबों को देने में इस्तेमाल किया जाता था।
यीशु हर समय अपने हृदय में एक सिद्ध विश्राम की दशा में रहता था, क्योंकि वह सिर्फ पिता की महिमा चाहता था और सिर्फ अपने पिता की पसन्द में ही दिलचस्पी रखता था। वह अपने पिता के सम्मुख रहता था और उसे मनुष्यों के सम्मान या प्रशंसा की कोई परवाह नहीं थी। उसने कहा, "जो अपनी ओर से कहता है, वह अपनी ही बड़ाई चाहता है" (यूहन्ना 7:18)।
लेकिन चाहे ऐसा नज़र भी क्यों न आ रहा हो, या एक जैविक मसीही परमेश्वर का चाहे कितना भी खोजी होने का दिखावा भी क्यों न कर रहा हो, फिर भी असल में, वह उसकी गहराई में सिर्फ अपना आदर-सम्मान चाह रहा होता है। दूसरी तरफ, यीशु ने स्वयं अपने लिए कभी कोई आदर-सम्मान नहीं चाहा था।
वह जिसका मूल मनुष्य की चतुराई में होता है, और जो मानवीय कुशलता और योग्यता द्वारा किया जाता है, हमेशा मनुष्य को ही ऊँचा उठाता है। जो जीव में से शुरू होता है, वह सिर्फ सृष्टि की महिमा करता है।
लेकिन अनन्त के युगों में स्वर्ग में या पृथ्वी में ऐसा कुछ भी नहीं है जो किसी मनुष्य को आदर या महिमा दे सकता है। जो कुछ भी समय में से बच कर गुज़रते हुए अनन्त के द्वारों में प्रवेश करने पाएगा, वह सिर्फ परमेश्वर से, परमेश्वर के द्वारा, और परमेश्वर के लिए ही होगा।
जहाँ तक परमेश्वर की बात है, तो उसकी नज़र में एक काम से जुड़ा उद्देश्य वह बात है उस काम का मूल्य और गुण तय करता है। हम क्या काम करते हैं वह महत्वपूर्ण होता है, लेकिन हम वह क्यों करते हैं, वह और भी ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है।
हमने देखा है कि यीशु अपने काम की योजना पाने के लिए पिता की बाट जोहता था, और फिर उस योजना को पूरा करने की सामर्थ्य पाने के लिए भी पिता की बाट जोहता था, और इस तरह वह अपने पिता की सम्पूर्ण इच्छा को सिर्फ परमेश्वर की सामर्थ्य में ही पूरा करता था। लेकिन सिर्फ इतना ही नहीं था। जैसा कि हमने पिछले अध्याय में देखा था, कि अपनी बड़ी उपलब्धियों के बाद भी यीशु प्रार्थना करने के लिए चला जाता था - कि उसकी महिमा वह अपने पिता को दे सके। अपने परिश्रम के फल को वह एक बलिदानी भेंट के रूप में अपने पिता को अर्पित कर देता था। उसने अपने लिए कोई आदर-सम्मान नहीं चाहा था, और जब भी वह उसे दिया गया, उसने वह ग्रहण नहीं किया था (यूहन्ना 5:41; 8:50)। जब उसकी ख्याति दूर-दूर तक फैल गई, तब वह अपने पिता की महिमा करने के लिए पहाड़ों में चला गया था (लूका 5:15,16)। उसका यह दृढ़ संकल्प था कि वह स्वयं कभी उस महिमा को नहीं छूएगा।
लगातार यही मनोभाव बनाए रखने का नतीजा यह हुआ कि यीशु, पृथ्वी पर अपने जीवन के अंत में, पूरी ईमानदारी से यह कह सका था, "पिता, मैंने पृथ्वी पर तेरी महिमा की है" (यूहन्ना 17:4)।
वह पृथ्वी पर एक मनुष्य बनकर पिता की महिमा करने के लिए आया था। और उसने प्रतिदिन इसी बात को अपना लक्ष्य बनाकर अपना जीवन बिताया था। वह गंभीरता से यह प्रार्थना करता था कि उसे चाहे कुछ भी क़ीमत चुकानी पड़े, लेकिन महिमा सिर्फ पिता की ही हो। और अंततः वह इसी लक्ष्य को हासिल करने के लिए मरा कि पिता का जो सम्मान, सर्वोच्च स्थान, और महिमा जैसी स्वर्ग में है, वैसे ही पृथ्वी पर भी हो।
पौलुस कहता है कि आग से परखे जाने के दिन में (1 कुरि. 3:13), सभी यह जान लेंगे कि "हमने प्रभु का काम क्यों किया है?" (1 कुरि. 4:5, लिविंग)। उस दिन सबके उद्देश्य प्रकट हो जाएंगे और प्रभु द्वारा परखे जाएंगे।
जैविक सेवा अहम् (ख़ुदी) को ऊँचा और लोगों को परमेश्वर की बजाय हमारी तरफ खींचती है। लोग हमें सुनने के लिए आते हैं, प्रभावित हो जाते हैं और फिर दोबारा सुनने के लिए आते हैं, हमारा सम्मान करते हैं, और हमारे लिए भली बातें बोलते हैं। जब हम उस स्थान से हट जाते हैं, तब वे फिर से अपनी पुरानी आत्मिक दशा में लौट जाते हैं; जो प्रचार उन्होंने सुना था, उससे वे बदले जाकर बेहतर नहीं बने थे। एक मनुष्य के परिश्रम की असली परख उसके मर के चले जाने के बाद, उन लोगों की आत्मिक दशा द्वारा होती है जिनकी उसने सेवा की होती है। तब यह प्रकट हो जाता है कि उसकी सेवा जैविक थी या आत्मिक थी।
ऐसी सारी सेवकाई जो लोगों को हमारी तरफ खींचती है, वह अंतिम दिन लकड़ी, घास-फूस और भूसा साबित हो जाएगी क्योंकि उसने सिर्फ मनुष्य की महिमा की होगी।
यीशु की सेवकाई आत्मिक थी। इसका प्रमाण इस बात में है कि वह अपने पीछे जिनको छोड़ कर गया (हालांकि उनकी संख्या थोड़ी ही थी), वे भी जैविक नहीं आत्मिक बने थे। उसकी महिमा को प्रकट करने के लिए, इस बात में हमें भी उसके पद्चिन्हों पर चलना चाहिए।
जैविक सेवकाई और जैविक जीवन मसीह-विरोधी के आने और विश्व-स्तर पर उसे स्वीकार करने का रास्ता तैयार कर रहे हैं - जो पूरा जैविक मनुष्य होगा। वह अपने आपको दूसरों से ऊँचा उठाएगा, और बहुत से लोगों को अपनी तरफ खींच लाने के लिए चमत्कारिक शक्तियों का भी इस्तेमाल करेगा (2 थिस्स. 2:3-10)।
इसलिए, लोगों का ध्यान अपनी तरफ और अपने काम की तरफ खींचना मसीह-विरोधी की आत्मा का मूल तत्व है। मनुष्यों के विवेकों को इस तरह से अपने वश में कर लेना, कि फिर हम उन्हें यह बताएं कि उन्हें क्या करना है और कहाँ जाना है, एक जैविक काम होता है। लोगों को सलाह देना एक आत्मिक काम है, लेकिन उन्हें अपने वश में कर लेना, एक जैविक काम है।
यीशु ने अपने किसी भी शिष्य को कुछ करने के लिए कभी मजबूर नहीं किया था। परमेश्वर द्वारा मनुष्यों में निवेश किए गए चुनाव के अधिकार का उसने आदर किया।
इसलिए वह सभी मनुष्यों का सेवक था, और उन पर हुक्म चलाने की बजाय उसने उनकी सेवा की।
एक सेवक की आत्मा की जगह एक शासक और स्वामी की आत्मा में होकर प्रचार करना ज़्यादा आसान होता है (2 कुरि. 4:5)। हम अपने विचारों को दूसरों पर थोपने के लिए अपनी जैविक शक्ति का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसका नतीजा यह होगा कि लोग हमारे गुलाम बन जाएंगे।
एक व्यक्ति जो उत्साही है, और अपनी स्वयं की प्रबल जैविक-शक्ति से अनजान है, वह यह समझ ही नहीं पाएगा कि वह लोगों को मसीह के लिए नहीं बल्कि अपने लिए जीत रहा है। परमेश्वर का काम मानवीय बल या शक्ति से नहीं, बल्कि पवित्र-आत्मा की सामर्थ्य द्वारा किया जाता है। और पवित्र आत्मा के काम का एक चिन्ह् स्वतंत्रता है (2 कुरि. 3:17) - हरेक व्यक्ति को दी गई पूरी आज़ादी।
एक सेवक एक घर में किस तरह सेवा करता है, इस पर विचार करें। वह ख़ामोशी से काम करता रहता है, और जो करने की ज़रूरत है वह करने के बाद, वह चुपचाप रसोई में लौट जाता है। वह तुरही बजाता और दिखावा करता हुआ नहीं आता, और न ही वह मेज़ पर बैठे लोगों को यह बताता है कि उन्हें क्या करना चाहिए। ऐसे कितने लोग हैं जो इस तरह प्रभु की सेवा करने के लिए तैयार हैं?
जैसा कि किसी ने कहा है, "एक सेवक को सिर्फ एक ही बात में राज करने का अधिकार है, और वह है स्वयं उसका शरीर। जिस अनुपात में वह अपने शरीर पर राज करता है, उसी अनुपात में वह दूसरों को उनके आत्मिक जीवन में बढ़ा सकता है। एक आत्मिक सेवक सिर्फ उस सामर्थ्य से सेवा करता है जो उसे परमेश्वर द्वारा दी जाती है, और यह सामर्थ्य उसे सिर्फ दूसरों की ज़रूरत पूरी करने के लिए ही दी जाती है। लेकिन अगर हम उस सामर्थ्य को एक व्यक्ति पर राज करने या उसे किसी भी तरह से मजबूर करने के लिए इस्तेमाल करेंगे, तो वह निराश होकर अंततः अपना रास्ता चुन सकता है। एक सेवक को इस तरह काम करना चाहिए कि जीवात्माएं स्वयं उसके संपर्क में नहीं बल्कि परमेश्वर के साथ एक जीवित संपर्क में लाई जाएं जो सब कुछ करता है (1 कुरि- 12:6)।"
यीशु ने इस तरह परमेश्वर की महिमा करनी चाही थी कि वह स्वयं उसके प्रेरितों के लिए ऐसा रास्ता तैयार करने के लिए तैयार था कि उसके जाने के बाद, वे उससे भी बड़े काम कर सकें (यूहन्ना 14:12)। यह बड़ा काम, निस्संदेह कलीसिया का निर्माण करना था जिसमें उसके अंगों को आपस में इस तरह से एक होना था जैसे पिता और पुत्र एक थे (यूहन्ना 17:21-23)। यीशु के पृथ्वी पर रहने के दिनों में, उसके दो शिष्य भी आपस में इस तरह एक नहीं हुए थे जैसे पिता और पुत्र एक हैं। लेकिन पैन्तेकुस्त के दिन के बाद, उसके अनेक शिष्य बिलकुल उसी तरह से एक हुए हैं जैसा उसने चाहा था। यही वह बड़ा काम था।
यीशु ने दूसरों के लिए ऐसा रास्ता तैयार किया कि वे एक बड़ा काम कर सकें। उसने मर कर उस काम की बुनियाद रखी और फिर उसके शिष्यों ने उस पर निमार्ण किया।
यीशु में कोई खुदगर्ज़ी नहीं थी। अगर उसके द्वारा किए गए किसी काम का श्रेय किसी दूसरे को मिल जाता था, लेकिन अगर उसमें पिता की महिमा होती थी, तो उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता था।
अगर आज हमें कलीसिया की, मसीह की देह की, जीवन से सेवा करनी है, और अगर हमें उसे मसीह के पूरे डीलडौल तक बढ़ाना है, तो हममें यही आत्मा होनी चाहिए।
यीशु पूरी तरह से पिता के इस तरह सम्मुख रहा कि मर के जी उठने के बाद, उसने उसे सूली पर चढ़ाने वालों के सामने भी अपने आपको निर्दोष साबित करने की कोशिश नहीं की थी।
संसार और यहूदी अगुवों की नज़र में यीशु की सेवकाई पूरी तरह से निष्फल थी। अगर यीशु जैविक होता, तो अपने जी उठने के बाद उसमें यह बड़ी लालसा होती कि वह उन अगुवों के सामने जाकर उन्हें विस्मित कर देता और अपने आपको सच्चा साबित कर देता। लेकिन उसने ऐसा नहीं किया था। अपने जी-उठने के बाद, उसने अपने आपको सिर्फ उन पर प्रकट किया जिन्होंने उस पर विश्वास किया था।
उस समय यीशु को सच्चा साबित करने का पिता का ठहराया हुआ समय नहीं हुआ था, और यीशु इंतज़ार करने के लिए तैयार था। वह समय अभी तक नहीं आया है।
संसार में आज भी यीशु के बारे में ग़लतफहमी है, और ज़्यादातर लोग उसके जीवन को एक नाकामी मानते हैं। उसका जीवन (मनुष्य के रूप में) एक गौशाला की चरनी के अपमान से शुरू हुआ था, और दो घिनौने अपराधियों के बीच में सूली पर पूरा हुआ था। इस संसार ने आिख़री बार उसे वही देखा था।
अगर उसमें पिता की महिमा हो रही थी, तो यीशु को मनुष्यों के सामने नाकाम नज़र आने में कोई आपत्ति नहीं थी। उसका जीवन और काम मनुष्यों द्वारा सराहा जाने के लिए नहीं किया गया था, और इसलिए एक दिन पिता उसे सबके सामने अपार महिमा और आदर के साथ सच्चा ठहराएगा, और उस दिन हरेक घुटना उसके आगे टिक जाएगा और हर ज़बान यह अंगीकार करेगी कि यीशु ही प्रभु है - लेकिन वह भी परमेश्वर पिता की महिमा के लिए ही होगा।
और इसलिए, हमें अपने आपसे यह तीसरा सवाल पूछना चाहिएः
क्या मैं सिर्फ परमेश्वर की महिमा के लिए जीता और काम करता हूँ?
पवित्र शास्त्र के अंतिम पृष्ठों में, हम पवित्र आत्मा के काम का नतीजा देख सकते हैं - मसीह की दुल्हन। हम वहाँ शैतान के नकली कामों का नतीजा भी देख सकते हैं - वेश्या कलीसिया।
यूहन्ना कहता है, "मैंने पवित्र नगरी, नए यरूशलेम को परमेश्वर की तरफ एक दुल्हन की तरह सजी हुई उतरते देखा। वह परमेश्वर की महिमा से भरी थी, और उसकी चमक अत्यंत बहुमूल्य पत्थर अर्थात् यशब के समान थी जो स्फटिक की तरह उज्जवल था" (प्रका. 21:2,10,11, लिविंग)।
मसीह की दुल्हन का दर्शन देखने से पहले, युहन्ना ने वेश्या का दर्शन देखा था - वह आत्मिक वेश्या जो परमेश्वर से प्रेम करने का दावा तो करती है, लेकिन असल में वह इस संसार से प्रेम करती है (याकूब 4:4)। यह नकली मसीहियत है जिसमें ईश्वरीय भक्ति (सही धर्म-सिद्धान्तों) का वेश तो है, लेकिन उसकी शक्ति (ईश्वरीय जीवन) नहीं है (2 तीमु. 3:5)।
यूहन्ना कहता है, "मैंने एक स्त्री को देखा - महान् बेबीलोन, वेश्याओं की माता, और एक आवाज़ को यह कहते सुना, 'गिर पड़ी, महानगरी बेबीलोन गिर पड़ी। उसके जलने का धुआँ देखो। उसका धुआँ युगानुयुग उठता रहेगा" (प्रका. 17:3,5; 18:2,9; 19:3)।
यह तुलना बहुत आश्चर्यजनक है। दुल्हन न्याय की आग में से गुज़र जाती है, 'एक बहुमूल्य जवाहरात की तरह चमकती है,' लेकिन वेश्या पूरी तरह जल कर भस्म हो जाती है, और उसका धुआँ आकाश में ऊँचा उठता रहता है क्योंकि वह नाश हो जाने वाली वस्तुओं से बनी थी।
दुल्हन यरूशलेम, और वेश्या बेबीलोन दो व्यवस्थाएं हैं - एक परमेश्वर की तरफ से है, और दूसरी 'पार्थिव, जैविक और शैतानी' है (याकूब 3:15 कोष्ठक)।
हम पहले बेबीलोन को देखें।
बेबीलोन की शुरूआत बाबुल की मीनार से हुई थी, जो मनुष्य की योजना के अनुसार, मनुष्य की शक्ति से, और मनुष्य की महिमा के लिए बनाई गई थी।
"उन्होंने एक-दूसरे से कहा" (मनुष्य से),
"आओ, हम अपने लिए एक नगर बनाएं" (मनुष्य द्वारा),
"और अपने लिए नाम कमाएं" (मनुष्य के लिए) (उत्पत्ति 11:3-4)।
सालों बाद, नबूकदनेस्सर राजा ने, महान् बेबीलोन नगरी का निर्माण करने के बाद जो उसके विशाल वैश्विक साम्राज्य की राजधानी थी, एक दिन नगर को देखा और उसी मनोभाव में यह कहाः
"क्या यह महान् नगरी बेबीलोन नहीं है,
जिसे मैंने स्वयं (मनुष्य से)...
अपनी सामर्थ्य से (मनुष्य द्वारा)...
अपने प्रताप की महिमा के लिए बनाया है (मनुष्य के लिए)" (दानि. 4:30)।
बेबीलोन की मीनार का अंत उसके न्याय में हुआ था। नबूकदनेस्सर के अहंकार द्वारा भी तुरन्त परमेश्वर का न्याय उस पर आ पड़ा था (दानि. 4:31-33)। जो कुछ भी मनुष्य की सोच-समझ से और मनुष्य की शक्ति द्वारा मनुष्य की महिमा के लिए किया गया है, उस सब का भी परमेश्वर द्वारा न्याय किया जाएगा। जो कुछ भी मानवीय जैविक-शक्ति द्वारा किया गया है, चाहे वह "मसीही काम" भी क्यों न कहलाता हो, वह नाश हो जाएगा।
"बेबीलोन की चौड़ी शहरपनाह नींव से ढा दी जाएगी, और उसके ऊँचे फाटकों में आग लगा दी जाएगी। उसके बनाने वाले देश-देश के लोगों (मसीही सेवकों---?) का परिश्रम व्यर्थ ठहरेगा - उनका काम आग में भस्म हो जाएगा" (यिर्म. 51:58 - लिविंग)।
दूसरी तरफ, यरूशलेम, परमेश्वर का नगर है (इब्रा. 12:22)। पुरानी वाचा में, परमेश्वर का मन्दिर यहीं था। यरूशलेम, परमेश्वर का निवास-स्थान, जिसका मूल मूसा द्वारा बनाए गए मिलाप वाले तम्बू में था (निर्ग. 25:8)।
मिलाप वाला तम्बू हूबहू परमेश्वर द्वारा दिए गए नमूने के अनुसार ही बनाया गया थाः
"...जो-जो आज्ञा परमेश्वर ने मूसा को दी थी, उन सब के अनुसार उसने किया" (निर्ग. 40:16) (परमेश्वर से)।
उसका निर्माण ऐसे लोगों द्वारा किया गया था जिन्होंने परमेश्वर की सामर्थ्य में होकर काम किया थाः
"बसलेल... मैंने उसे परमेश्वर के आत्मा से भर दिया है..." (निर्ग. 31:1-5) (परमेश्वर द्वारा)।
वह परमेश्वर की महिमा के लिए बनाया गया थाः
"तब मिलाप वाला तम्बू परमेश्वर की महिमा से भर गया" (निर्ग. 40:34) (परमेश्वर के लिए)।
वह जो परमेश्वर में से शुरू होता है, और उसकी ईश्वरीय सामर्थ्य द्वारा आगे बढ़ता है, सिर्फ वही परमेश्वर की महिमा के लिए हमेशा बना रहेगा। वह एक क़ीमती जवाहरात की तरह जगमगाता हुआ आग में से गुज़र जाएगा, क्योंकि वह सोने, चाँदी और मूल्यवान पत्थरों से बना है।
जब हम पवित्र शास्त्र के शुरूआती पन्नों को उसके आख़िरी पन्नों से मिलाते हैं, तो हम यह पाते हैं कि उनमें मौजूद दोनों पेड़ों ने - (जीवन के वृक्ष और भले और बुरे के ज्ञान के वृक्ष ने), समय पूरा होने तक, दो व्यवस्थाओं को उत्पन्न किया है - यरूशलेम और बेबीलोन।
वह जो वास्तव में पवित्र से उत्पन्न हुआ है - परमेश्वर से, परमेश्वर द्वारा, और परमेश्वर के लिए - हमेशा बना रहता है। और वह जो शरीर में से पैदा हुआ है - मनुष्य से , मनुष्य द्वारा और मनुष्य के लिए - नाश हो जाता है।
आज हम उत्पत्ति और प्रकाशितवाक्य के पन्नों के बीच में रह रहे हैं। और चाहे यह बात हमें समझ में आए या न आए, हम इन दोनों में से किसी एक व्यवस्था के घेरे में आ चुके हैं - एक जो परमेश्वर को ऊँचा उठाने और उसकी महिमा करने के लिए संकल्पबद्ध है, और दूसरी मनुष्य को ऊँचा उठाने और उसकी महिमा करने के लिए संकल्पबद्ध है; एक मसीह के पीछे जा रही है, और दूसरी आदम के पीछे जा रही है; एक आत्मा में जीवन जी रही है, और दूसरी देह और जीव में जीवन जी रही है।
यीशु और आदम दोनों ने परमेश्वर की आवाज़ को सुना था - दोनों के बीच में बस यही फ़र्क है कि एक ने सुनने के बाद आज्ञा का पालन किया, और दूसरे ने सुनने के बाद आज्ञा का उल्लंघन किया। और यीशु ने कहा कि उसकी आवाज़ को सुनने वालों के साथ भी यही होगा - एक आज्ञा का पालन करेंगे और अपना घर चट्टान पर बनाएंगे, और दूसरे सुनने के बाद आज्ञापालन नहीं करेंगे और इस तरह अपना घर रेत पर बनाएंगे, जो अंत में नाश हो जाएगा (मत्ती 7:24-27)।
यीशु ने जिन दो घरों की बात की थी, वे यरूशलेम और बेबीलोन हैं।
ऐसे लोग हैं जो वास्तव में विश्वास द्वारा धर्मी ठहराए जाते हैं और नई वाचा में प्रवेश करते हैं, यीशु के लहू मुहरबंद किए जाते हैं, परमेश्वर की इच्छा का पालन करने वाले जीवन में यीशु के पीछे चलते हैं (ख़ास तौर पर जैसा मत्ती अध्याय 5-7 में बताया गया है), जो चट्टान पर अपना घर बनाते हैं, और जिनका भाग यरूशलेम में है। यह जानने के लिए कि हमारा भाग यरूशलेम-वासियों के साथ है या नहीं, हमें सिर्फ मत्ती के अध्याय 5-7 पढ़ने की ज़रूरत है।
एक समानान्तर में, दूसरे ऐसे लोग हैं (और ये एक बड़े बहुमत में हैं), जो मत्ती अध्याय 5-7 में यीशु की आवाज़ सुनते हैं, लेकिन धार्मिकता, विश्वास, और कृपा की ग़लत समझ होने के कारण, एक धोखे से भरी सुरक्षा में रहते हुए यीशु के शब्दों का पालन करने पर ध्यान नहीं देते, और इस तरह, वे रेत में - बेबीलोन में - अपना निर्माण करते हैं, और हमेशा के लिए नाश हो जाते हैं।
ये अपनी नज़र में "मसीही" हैं, क्योंकि यीशु ने कहा कि रेत पर बनाने वाले मनुष्य ने उसकी आवाज़ को सुना था, इसलिए, वह कोई विधर्मी मूर्तिपूजक नहीं था, लेकिन ऐसा था जेा बाइबल पढ़ता था और "कलीसिया" में जाता था। उसकी समस्या सिर्फ यही थी कि वह आज्ञापालन नहीं करता था, इसलिए वह उस अनन्त उद्धार में सहभागी नहीं हो सकता था जिसकी प्रतिज्ञा उन लोगों से की गई है जो यीशु की आज्ञा का पालन करते हैं (इब्रा. 5-9)। उसका विश्वास असली नहीं था, क्योंकि उसने उसे सिद्ध करने के लिए आज्ञापालन के काम नहीं किए थे (याकूब 2:22, 26)।
जिन लोगों का सिर (नायक) आदम है, वे परमेश्वर की प्रकाशित इच्छा के प्रति आज्ञा उल्लंघन करने में अपने सिर की बात मानते हैं, लेकिन शैतान उन्हें यह कहते हुए तसल्ली दे देता है कि "तुम नहीं मरोगे" (उत्पत्ति 3:4), क्योंकि वे यह दावा करते हैं कि उन्होंने "मसीह को स्वीकार कर लिया है।" इस तरह, वे बेबीलोन में एक झूठी सुरक्षा में रहते हैं।
वैसे ही, जिनका सिर मसीह है, उनकी पहचान यह है कि वे परमेश्वर की इच्छा का पालन करते हुए "वैसे ही चलते हैं जैसे यीशु चलता था" (1 यूहन्ना 2:6)। ये मसीह के भाई व बहनें हैं (मत्ती 12:50), और यरूशलेम का भाग हैं।
मत्ती अध्याय 5-7 के अंत में यीशु ने जो दृष्टान्त सुनाया, उसमें एक दिलचस्प बात यह है कि बुद्धिमान और मूर्ख दोनों ही मनुष्यों के घर कुछ समय तक, जब तक की बरसात और बाढ़ नहीं आई थीं, साथ-साथ खड़े रहे थे, वैसे ही जैसे आज बेबीलोन और यरूशलेम साथ-साथ खड़े हैं। जबकि मूर्ख मनुष्य की दिलचस्पी सिर्फ बाहरी दिखावे में थी (उस साक्षी में, जो उसकी मनुष्यों के सामने थी), लेकिन बुद्धिमान मनुष्य का ध्यान प्रमुख रूप में उसकी बुनियाद पर था (परमेश्वर के सामने, उस जीवन में जो हृदय में छुपा हुआ था)।
लेकिन जब बरसात और बाढ़ आईं (परमेश्वर का न्याय), तब पहले बुनियाद को परखा गया।
"क्योंकि समय आ गया है कि परमेश्वर के घराने से ही न्याय आरम्भ हो; और अगर उसकी शुरूआत हमसे होनी है, तो उनकी क्या नियति होगी जिन्होंने परमेश्वर की तरफ से आए सुसमाचार की आज्ञा का उल्लंघन किया है? और अगर धर्मीजन ही मुश्किल से उद्धार पाएगा, तो अधर्मी और पापी के लिए तो कोई मौक़ा ही नहीं बचेगा?" (1 पत. 4:17,18 - बार्कले)।
"हरेक जो मुझसे 'हे प्रभु, हे प्रभु' कहता है, स्वर्ग के राज्य में प्रवेश न करेगा, लेकिन जो मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा पर चलता है, वही प्रवेश करेगा। उस दिन बहुत लोग मुझसे कहेंगे, 'हे प्रभु, हे प्रभु, क्या हमने तेरे नाम से नबूवत नहीं की, और तेरे नाम से दुष्टात्माओं को नहीं निकाला, और तेरे नाम से बहुत से चमत्कार नहीं किए थे?' तब मैं उनसे स्पष्ट कह दूँगा, 'मैंने तुमको कभी नहीं जाना (क्योंकि "जो पाप करता है, वह उसे नहीं जानता" - 1 यूहन्ना 3:6), कुकर्मियों (परमेश्वर की आज्ञा न मानने वालों), मुझसे दूर हटो'" (मत्ती 7:21-23)।
यहाँ ध्यान दें कि ऐसे बहुत होंगे जो उनके मनों में मसीही होंगे (यीशु को 'प्रभु' कह रहे होंगे) और उनकी भावनाओं में मसीही होंगे (यीशु को 'हे प्रभु, हे प्रभु' कह रहे होंगे), लेकिन फिर भी वे ऐसे लोग होंगे जिन्होंने उनके जीवनों में अपनी इच्छा को परमेश्वर की इच्छा पूरी करने के लिए अर्पित नहीं किया होगा। प्रभु ऐसे लोगों को अस्वीकार करते हुए यह कह देगा कि वे उसके लिए अनजाने लोग हैं।
यरूशलेम की विशिष्ट लाक्षणिकता पवित्रता है। उसे "पवित्र नगरी" कहा गया है (प्रका. 21:2)। लेकिन बेबीलोन की विशिष्टता उसकी महानता है। उसे "महान नगरी" कहा गया है (प्रका. 18:10)। प्रकाशितवाक्य में उसे 11 बार "महान" कहा गया है।
वे जो सच्ची पवित्रता में वास करते हैं, परमेश्वर के आज्ञाकारी रहते हैं, और विश्वास द्वारा कृपा से मसीह के स्वभाव में सहभागी होते हैं, वे एक सामूहिक रूप में यरूशलेम में निर्मित किए जाते हैं, जबकि वे जो इस पृथ्वी पर महान् बनने की खोज में रहते हैं (मनुष्यों की साक्षी और सम्मान चाहते हैं), वे बेबीलोन में निर्मित किए जाते हैं।
1900 सालों तक, परमेश्वर के लोगों के पास यह बुलाहट आती रही है, "हे मेरे लोगों उसमें से (बेबीलोन में से) निकल आओ; उसके पापों में सहभागी न बनो, वर्ना तुम भी उसके साथ दण्ड पाओगे" (प्रका. 18:4 - लिविंग)।
अब, जबकि हम युग के अंत में पहुँच गए हैं, तो यह बुलाहट आज और भी ज़्यादा आग्रहपूर्ण हो गई है। यह वास्तव में एक दुःखद बात है कि परमेश्वर के लोग भी परमेश्वर की ऐसी पुकार को न सुनने की वजह से जो बिलकुल स्पष्ट है, बेबीलोन में उलझ जाएंगे, और इस तरह उसके दण्ड में सहभागी हों जाएंगे। अगर लोगों ने ऐसा जीवन नहीं बिताया है जो सच्चे मसीही-सिद्धान्तों के साथ मेल खाता है, या आज्ञापालन के ऐसे काम नहीं किए हैं जो असली विश्वास की पहचान के चिन्ह् होते हैं, तो उस दिन मसीही धर्म-सिद्धान्तों को थामे रहने से, या "मसीह के लिए फैसला" कर लेने से किसी को कोई फायदा नहीं होगा।
जब परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप व समानता में रचा था, तब उसकी कितनी तीव्र इच्छा थी कि मनुष्य उसके ईश्वरीय स्वभाव में सहभागी हो और उसकी महिमा को प्रदर्शित करे!
और जब मनुष्य पाप में गिरा, तो परमेश्वर उसकी कितनी भारी क़ीमत चुकाने के लिए तैयार हुआ, कि "उसने अपने ही पुत्र को पापमय शरीर की समानता में, तथा पाप के लिए बलिदान होने के लिए भेजकर, शरीर में पाप को दोषी ठहराया," (रोमि. 8:3), कि एक ऐसा मार्ग तैयार हो सके जिसके द्वारा मनुष्य पुनःस्थापित किया जाए, और वापिस उसी जगह पर लाया जाए जहाँ वह एक बार फिर से ईश्वरीय उद्देश्य को पूरा कर सके।
पिता, पुत्र और पवित्र-आत्मा, मनुष्य को छुड़ाने और उसे बदलने का काम एक साथ मिलकर कर रहे हैं। हालांकि बहुत से ऐसे पुरुष व स्त्रियाँ हैं जो उनकी मूर्खता में परमेश्वर की बुलाहट का जवाब नहीं देंगे, फिर भी परमेश्वर का उद्देश्य ऐसे बचे हुओं में (उन थोड़े से लोगों में जिन्होंने जीवन का संकरा मार्ग पा लिया है), पूरा हो जाएगा। ये वे लोग हैं जिन्होंने यीशु की तरह अपने आपको परमेश्वर के अधीन किया है, जिनके द्वारा परमेश्वर की महिमा न सिर्फ यहाँ समय के दायरे में, बल्कि अनन्त में युगानुयुग तब भी प्रकट होती रहेगी जब परमेश्वर उनके द्वारा अपनी कृपा की उस असीम भरपूरी को प्रकट करेगा जिसमें वे मसीह यीशु के द्वारा सहभागी हुए हैं।
आज, कल और युगानुयुग, उसकी महिमा होती रहे। जिसके सुनने के कान हों, वह सुने।